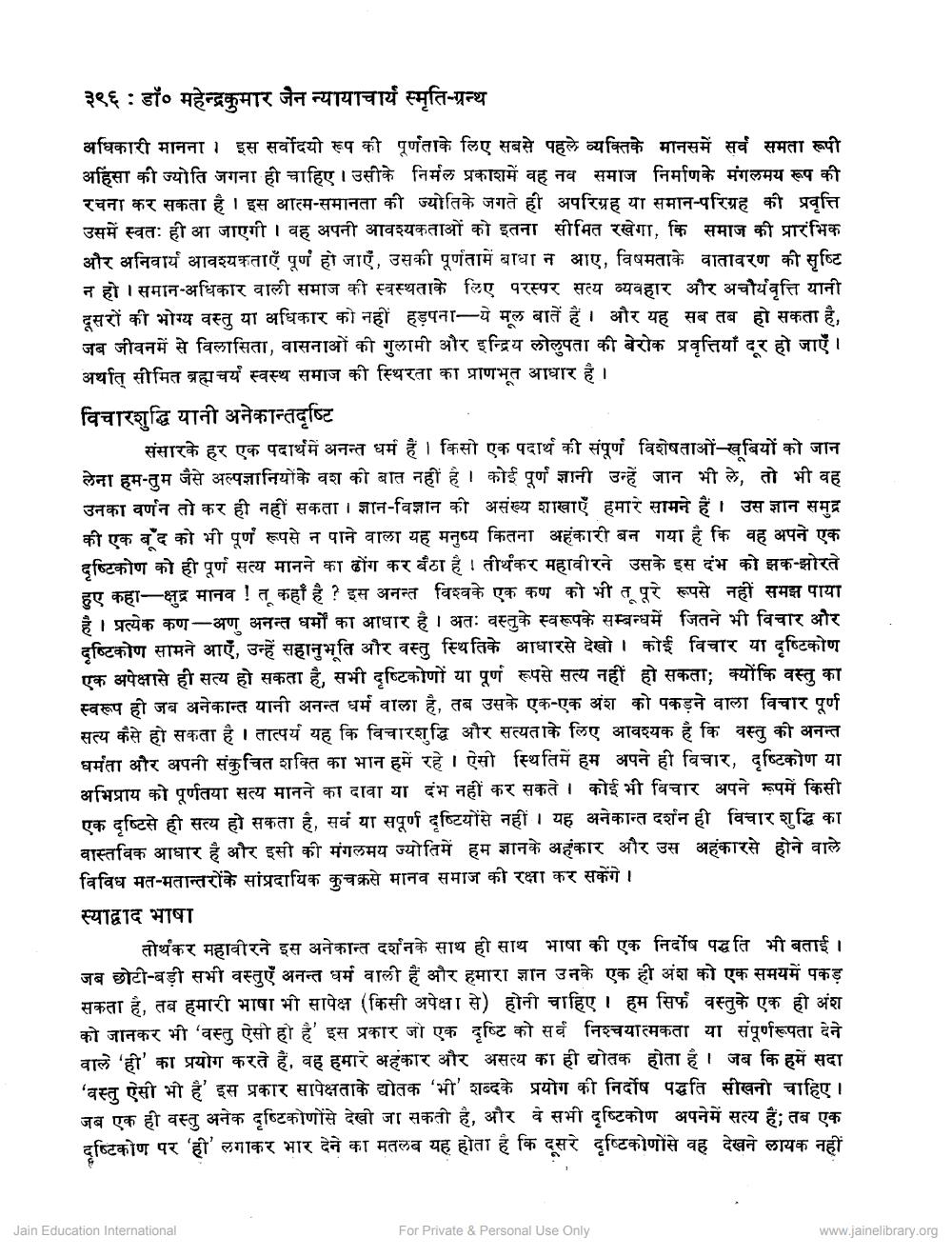________________
३९६ : डॉ० महेन्द्रकुमार जैन न्यायाचार्य स्मृति-ग्रन्थ
अधिकारी मानना । इस सर्वोदयो रूप की पूर्णता के लिए सबसे पहले व्यक्तिके मानस में सर्वं समता रूपी अहिंसा की ज्योति जगना ही चाहिए। उसीके निर्मल प्रकाशमें वह नव समाज निर्माणके मंगलमय रूप की रचना कर सकता है । इस आत्म-समानता की ज्योतिके जगते ही अपरिग्रह या समान - परिग्रह की प्रवृत्ति उसमें स्वतः ही आ जाएगी। वह अपनी आवश्यकताओं को इतना सीमित रखेगा, कि समाज की प्रारंभिक और अनिवार्य आवश्यकताएँ पूर्ण हो जाएँ, उसकी पूर्णता में बाधा न आए, विषमताके वातावरण की सृष्टि न हो । समान अधिकार वाली समाज की स्वस्थताके लिए परस्पर सत्य व्यवहार और अचौर्य वृत्ति यानी दूसरों की भोग्य वस्तु या अधिकार को नहीं हड़पना -ये मूल बातें हैं । और यह सब तब हो सकता है, जब जीवनमें से विलासिता, वासनाओं की गुलामी और इन्द्रिय लोलुपता की बेरोक प्रवृत्तियाँ दूर हो जाएँ । अर्थात् सीमित ब्रह्मचर्यं स्वस्थ समाज की स्थिरता का प्राणभूत आधार है ।
विचारशुद्धि यानी अनेकान्तदृष्टि
संसार के हर एक पदार्थ में अनन्त धर्म हैं । किसो एक पदार्थ की संपूर्ण विशेषताओं-खूबियों को जान लेना हम-तुम जैसे अल्पज्ञानियोंके वश की बात नहीं है । कोई पूर्ण ज्ञानी उन्हें जान भी ले, तो भी वह उनका वर्णन तो कर ही नहीं सकता । ज्ञान-विज्ञान की असंख्य शाखाएँ हमारे सामने हैं । उस ज्ञान समुद्र की एक बूँद को भी पूर्ण रूपसे न पाने वाला यह मनुष्य कितना अहंकारी बन गया है कि वह अपने एक दृष्टिकोण को ही पूर्ण सत्य मानने का ढोंग कर बैठा है। तीर्थंकर महावीरने उसके इस दंभ को झकझोरते हुए कहा - क्षुद्र मानव ! तू कहाँ है ? इस अनन्त विश्वके एक कण को भी तू पूरे रूपसे नहीं समझ पाया है । प्रत्येक कण - अणु अनन्त धर्मों का आधार है । अतः वस्तुके स्वरूपके सम्बन्ध में जितने भी विचार और दृष्टिकोण सामने आएँ, उन्हें सहानुभूति और वस्तु स्थितिके आधारसे देखो। कोई विचार या दृष्टिकोण एक अपेक्ष सत्य हो सकता है, सभी दृष्टिकोणों या पूर्ण रूपसे सत्य नहीं हो सकता; क्योंकि वस्तु का स्वरूप ही जब अनेकान्त यानी अनन्त धर्म वाला है, तब उसके एक-एक अंश को पकड़ने वाला विचार पूर्ण सत्य कैसे हो सकता है । तात्पर्य यह कि विचारशुद्धि और सत्यता के लिए आवश्यक है कि वस्तु की अनन्त धर्मता और अपनी संकुचित शक्ति का भान हमें रहे । ऐसी स्थिति में हम अपने ही विचार, दृष्टिकोण या
अभिप्राय को पूर्णतया सत्य मानने का दावा या दंभ नहीं कर सकते । कोई भी विचार अपने रूपमें किसी एक दृष्टिसे ही सत्य हो सकता है, सर्व या सपूर्ण दृष्टियोंसे नहीं । यह अनेकान्त दर्शन ही विचार शुद्धि का वास्तविक आधार है और इसी की मंगलमय ज्योतिमें हम ज्ञानके अहंकार और उस अहंकार से होने वाले विविध मत-मतान्तरोंके सांप्रदायिक कुचक्रसे मानव समाज की रक्षा कर सकेंगे ।
स्याद्वाद भाषा
तीर्थंकर महावीरने इस अनेकान्त दर्शनके साथ ही साथ भाषा की एक निर्दोष पद्धति भी बताई । जब छोटी-बड़ी सभी वस्तुएँ अनन्त धर्म वाली हैं और हमारा ज्ञान उनके एक ही अंश को एक समयमें पकड़ सकता है, तब हमारी भाषा भी सापेक्ष ( किसी अपेक्षा से) होनी चाहिए। हम सिर्फ वस्तुके एक ही अंश को जानकर भी 'वस्तु ऐसी हो है' इस प्रकार जो एक दृष्टि को सर्वं निश्चयात्मकता या संपूर्णरूपता देने वाले 'ही' का प्रयोग करते हैं, वह हमारे अहंकार और असत्य का ही द्योतक होता है । जब कि हमें सदा 'वस्तु ऐसी भी है' इस प्रकार सापेक्षताके द्योतक 'भी' शब्द के प्रयोग की निर्दोष पद्धति सीखनी चाहिए । जब एक ही वस्तु अनेक दृष्टिकोणोंसे देखी जा सकती है, और वे सभी दृष्टिकोण अपने में सत्य हैं; तब एक दृष्टिकोण पर 'ही' लगाकर भार देने का मतलब यह होता है कि दूसरे दृष्टिकोणोंसे वह देखने लायक नहीं
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org