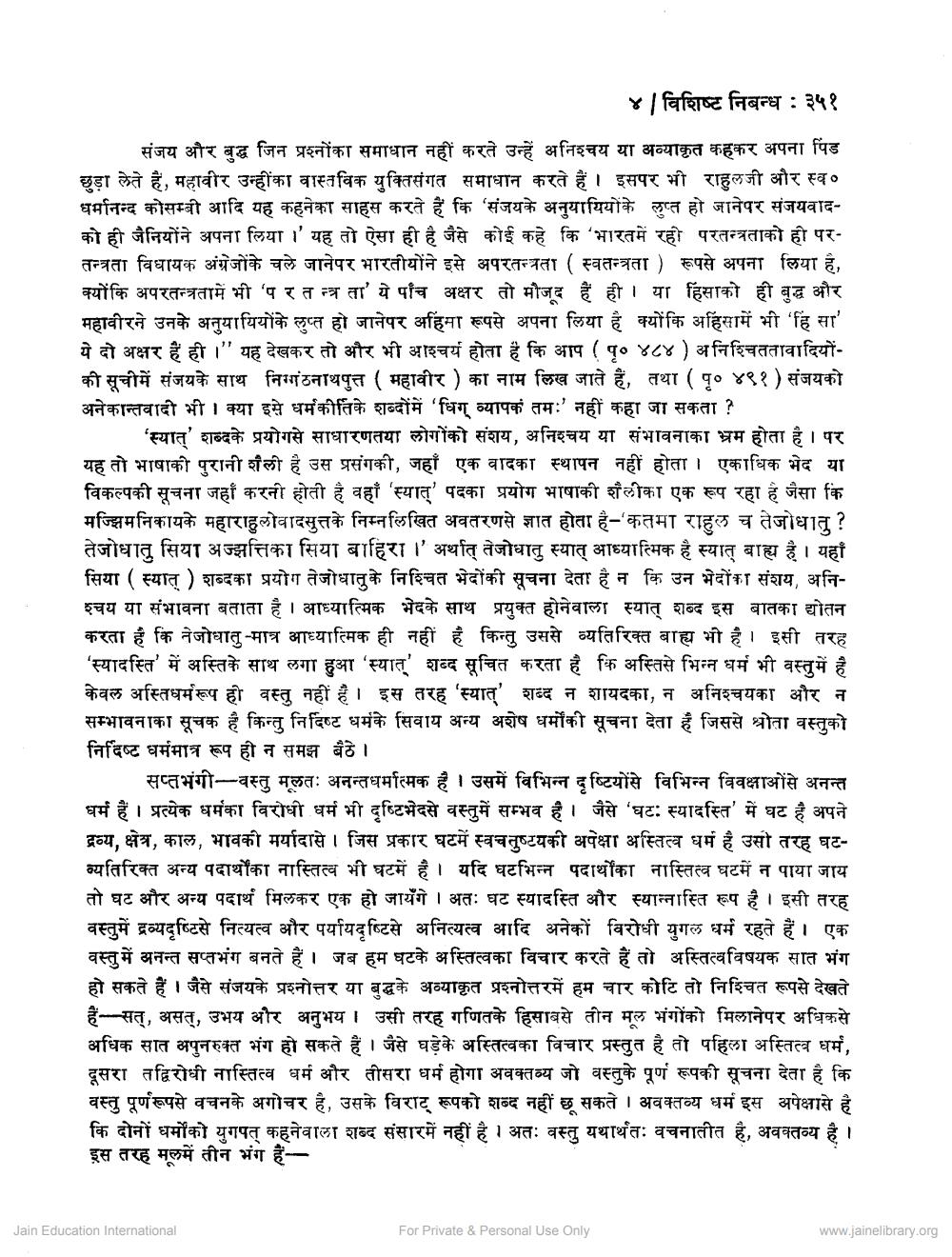________________
४/ विशिष्ट निबन्ध : ३५१
संजय और बुद्ध जिन प्रश्नोंका समाधान नहीं करते उन्हें अनिश्चय या अव्याकृत कहकर अपना पिंड छुड़ा लेते है, महावीर उन्हींका वास्तविक युक्तिसंगत समाधान करते हैं। इसपर भी राहुलजी और स्व० धर्मानन्द कोसम्बी आदि यह कहनेका साहस करते हैं कि 'संजयके अनुयायियोंके लुप्त हो जानेपर संजयवादको ही जैनियोंने अपना लिया।' यह तो ऐसा ही है जैसे कोई कहे कि 'भारतमें रही परतन्त्रताको ही परतन्त्रता विधायक अंग्रेजोंके चले जानेपर भारतीयोंने इसे अपरतन्त्रता ( स्वतन्त्रता ) रूपसे अपना लिया है, क्योंकि अपरतन्त्रतामें भी 'प र त न्त्र ता' ये पांच अक्षर तो मौजूद हैं ही। या हिंसाको ही बुद्ध और महावीरने उनके अनुयायियोंके लुप्त हो जानेपर अहिंमा रूपसे अपना लिया है क्योंकि अहिंसामें भी 'हिं सा' ये दो अक्षर हैं ही।" यह देखकर तो और भी आश्चर्य होता है कि आप ( पृ० ४८४ ) अनिश्चिततावादियोंकी सूचीमें संजयके साथ निग्गंठनाथपुत्त ( महावीर ) का नाम लिख जाते हैं, तथा ( पृ० ४९१) संजयको अनेकान्तवादी भी। क्या इसे धर्मकीर्तिके शब्दों में 'धिग् व्यापकं तमः' नहीं कहा जा सकता?
'स्यात' शब्दके प्रयोगसे साधारणतया लोगोंको संशय, अनिश्चय या संभावनाका भ्रम होता है । पर यह तो भाषाकी पुरानी शैली है उस प्रसंगकी, जहाँ एक वादका स्थापन नहीं होता। एकाधिक भेद या विकल्पकी सूचना जहाँ करनी होती है वहाँ 'स्यात्' पदका प्रयोग भाषाकी शैलीका एक रूप रहा है जैसा कि मज्झिमनिकायके महाराहुलोवादसुत्तके निम्नलिखित अवतरणसे ज्ञात होता है-'कतमा राहल च तेजोधात? तेजोधातु सिया अज्झत्तिका सिया बाहिरा ।' अर्थात् तेजोधातु स्यात् आध्यात्मिक है स्यात् बाह्य है। यहाँ सिया (स्यात् ) शब्दका प्रयोग तेजोधातुके निश्चित भेदोंकी सूचना देता है न कि उन भेदोंका संशय, अनिश्चय या संभावना बताता है । आध्यात्मिक भेदके साथ प्रयुक्त होनेवाला स्यात् शब्द इस बातका द्योतन करता है कि तेजोधातु-मात्र आध्यात्मिक ही नहीं है किन्तु उससे व्यतिरिक्त बाह्य भी है। इसी तरह 'स्यादस्ति' में अस्तिके साथ लगा हुआ स्यात्' शब्द सूचित करता है कि अस्तिसे भिन्न धर्म भी वस्तु में है
धर्मरूप ही वस्तु नहीं है। इस तरह स्यात्' शब्द न शायदका, न अनिश्चयका और न सम्भावनाका सूचक है किन्तु निर्दिष्ट धर्मके सिवाय अन्य अशेष धर्मोकी सूचना देता है जिससे श्रोता वस्तुको निर्दिष्ट धर्ममात्र रूप ही न समझ बैठे।
सप्तभंगी-वस्तु मलतः अनन्तधर्मात्मक है। उसमें विभिन्न दृष्टियोंसे विभिन्न विवक्षाओंसे अनन्त धर्म हैं। प्रत्येक धर्मका विरोधी धर्म भी दृष्टिभेदसे वस्तुमें सम्भव है। जैसे 'घटः स्यादस्ति' में घट है अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावकी मर्यादासे । जिस प्रकार घटमें स्वचतुष्टयकी अपेक्षा अस्तित्व धर्म है उसी तरह घटव्यतिरिक्त अन्य पदार्थोंका नास्तित्व भी घटमें है। यदि घटभिन्न पदार्थोंका नास्तित्व घटमें न पाया जाय तो घट और अन्य पदार्थ मिलकर एक हो जायेंगे । अतः घट स्यादस्ति और स्यान्नास्ति रूप है। इसी तरह वस्तुमें द्रव्यदृष्टिसे नित्यत्व और पर्यायदृष्टिसे अनित्यत्व आदि अनेकों विरोधी युगल धर्म रहते हैं। एक वस्तु में अनन्त सप्तभंग बनते हैं। जब हम घटके अस्तित्वका विचार करते हैं तो अस्तित्वविषयक सात भंग हो सकते हैं । जैसे संजयके प्रश्नोत्तर या बुद्धके अव्याकृत प्रश्नोत्तरमें हम चार कोटि तो निश्चित रूपसे देखते हैं-सत्, असत्, उभय और अनुभय । उसी तरह गणितके हिसाबसे तीन मूल भंगोंको मिलानेपर अधिकसे अधिक सात अपुनरुक्त भंग हो सकते हैं । जैसे घड़े के अस्तित्वका विचार प्रस्तुत है तो पहिला अस्तित्व धर्म, दूसरा तद्विरोधी नास्तित्व धर्म और तीसरा धर्म होगा अवक्तव्य जो वस्तुके पूर्ण रूपकी सूचना देता है कि वस्तु पूर्णरूपसे वचनके अगोचर है, उसके विराट रूपको शब्द नहीं छ सकते । अवक्तव्य धर्म इस अपेक्षासे है कि दोनों धर्मोको युगपत् कहनेवाला शब्द संसारमें नहीं है । अतः वस्तु यथार्थतः वचनातीत है, अवक्तव्य है। इस तरह मलमें तीन भंग है
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org