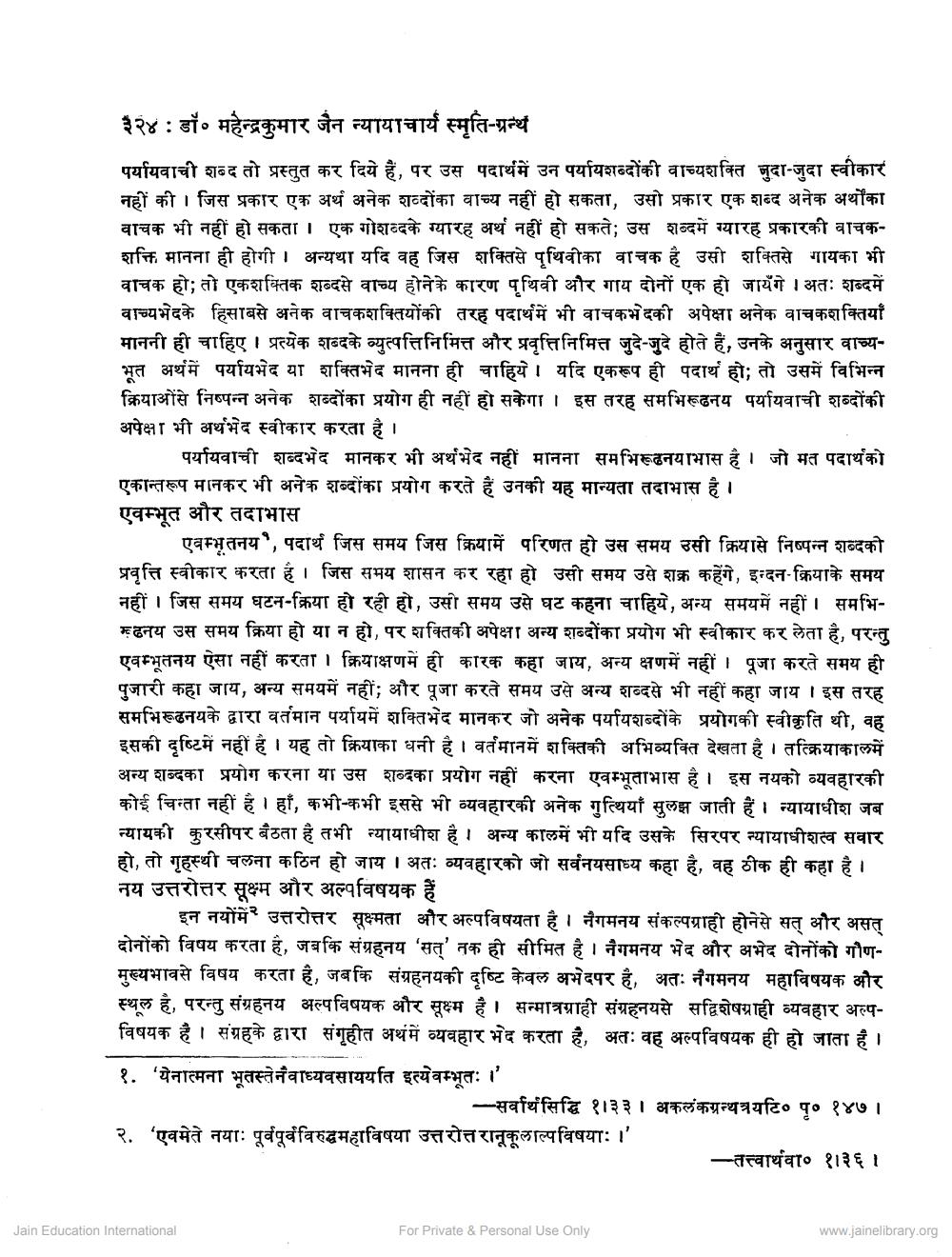________________
३२४ : डॉ० महेन्द्रकुमार जैन न्यायाचार्य स्मृति-ग्रन्थ
पर्यायवाची शब्द तो प्रस्तुत कर दिये हैं, पर उस पदार्थ में उन पर्यायशब्दोंकी वाच्यशक्ति जुदा-जुदा स्वीकार नहीं की । जिस प्रकार एक अर्थ अनेक शब्दोंका वाच्य नहीं हो सकता, उसी प्रकार एक शब्द अनेक अर्थोंका वाचक भी नहीं हो सकता । एक गोशब्दके ग्यारह अर्थ नहीं हो सकते; उस शब्द में ग्यारह प्रकारकी वाचकशक्ति मानना ही होगी । अन्यथा यदि वह जिस शक्तिसे पृथिवीका वाचक है उसी शक्तिसे गायका भी वाचक हो; तो एकशक्तिक शब्दसे वाच्य होने के कारण पृथिवी और गाय दोनों एक हो जायँगे । अतः शब्दमें वाच्यभेदके हिसाब से अनेक वाचकशक्तियोंकी तरह पदार्थ में भी वाचकभेदकी अपेक्षा अनेक वाचकशक्तियाँ माननी ही चाहिए । प्रत्येक शब्दके व्युत्पत्तिनिमित्त और प्रवृत्तिनिमित्त जुदे - जुदे होते हैं, उनके अनुसार वाच्य - भूत अर्थ में पर्यायभेद या शक्तिभेद मानना ही चाहिये । यदि एकरूप ही पदार्थ हो; तो उसमें विभिन्न क्रियाओंसे निष्पन्न अनेक शब्दों का प्रयोग ही नहीं हो सकेगा । इस तरह समभिरूढनय पर्यायवाची शब्दोंकी अपेक्षा भी अर्थभेद स्वीकार करता है ।
पर्यायवाची शब्दभेद मानकर भी अर्थभेद नहीं मानना समभिरूढनयाभास है । जो मत पदार्थको एकान्तरूप मानकर भी अनेक शब्दों का प्रयोग करते हैं उनकी यह मान्यता तदाभास है ।
एवम्भूत और तदाभास
एवम्भूतनय', पदार्थ जिस समय जिस क्रियामें परिणत हो उस समय उसी क्रियासे निष्पन्न शब्दको प्रवृत्ति स्वीकार करता है । जिस समय शासन कर रहा हो उसी समय उसे शक्र कहेंगे, इन्दन- क्रिया के समय नहीं । जिस समय घटन-क्रिया हो रही हो, उसी समय उसे घट कहना चाहिये, अन्य समय में नहीं । समभि
ढनय उस समय क्रिया हो या न हो, पर शक्तिकी अपेक्षा अन्य शब्दों का प्रयोग भी स्वीकार कर लेता है, परन्तु एवम्भूतनय ऐसा नहीं करता । क्रियाक्षण में ही कारक कहा जाय, अन्य क्षणमें नहीं । पूजा करते समय पुजारी कहा जाय, अन्य समयमें नहीं; और पूजा करते समय उसे अन्य शब्दसे भी नहीं कहा जाय । इस तरह समभिरूढनयके द्वारा वर्तमान पर्याय में शक्तिभेद मानकर जो अनेक पर्यायशब्दोंके प्रयोगकी स्वीकृति थी, वह इसकी दृष्टि में नहीं है । यह तो क्रियाका धनी है । वर्तमान में शक्तिकी अभिव्यक्ति देखता है । तत्क्रियाकालमें अन्य शब्दका प्रयोग करना या उस शब्दका प्रयोग नहीं करना एवम्भूताभास है । इस नयको व्यवहारकी कोई चिन्ता नहीं है । हाँ, कभी-कभी इससे भी व्यवहारकी अनेक गुत्थियाँ सुलझ जाती हैं । न्यायाधीश जब न्यायकी कुरसीपर बैठता है तभी न्यायाधीश है । अन्य कालमें भी यदि उसके सिरपर न्यायाधीशत्व सवार हो, तो गृहस्थी चलना कठिन हो जाय । अतः व्यवहारको जो सर्वनयसाध्य कहा है, वह ठीक ही कहा है । नय उत्तरोत्तर सूक्ष्म और अल्पविषयक हैं।
इन नयोंमें? उत्तरोत्तर सूक्ष्मता और अल्पविषयता है । नैगमनय संकल्पग्राही होनेसे सत् और असत् दोनोंको विषय करता है, जबकि संग्रहनय 'सत्' तक ही सीमित है । नैगमनय भेद और अभेद दोनोंको गौणमुख्यभावसे विषय करता है, जबकि संग्रहनयकी दृष्टि केवल अभेदपर है, अतः नैगमनय महाविषयक और स्थूल है, परन्तु संग्रहनय अल्पविषयक और सूक्ष्म है | सन्मात्रग्राही संग्रहनयसे सद्विशेषग्राही व्यवहार अल्पविषयक है । संग्रहके द्वारा संगृहीत अर्थ में व्यवहार भेद करता है, अतः वह अल्पविषयक ही हो जाता है । १. 'येनात्मना भूतस्तेनैवाध्यवसाययति इत्येवम्भूतः ।'
- सर्वार्थसिद्धि १।३३ | अकलंकग्रन्थत्रयटि० पृ० १४७ । २. ' एवमेते नयाः पूर्वपूर्वविरुद्ध महाविषया उत्तरोत्तरानूकूलाल्पविषयाः । '
- तत्त्वार्थवा० १३६ ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org