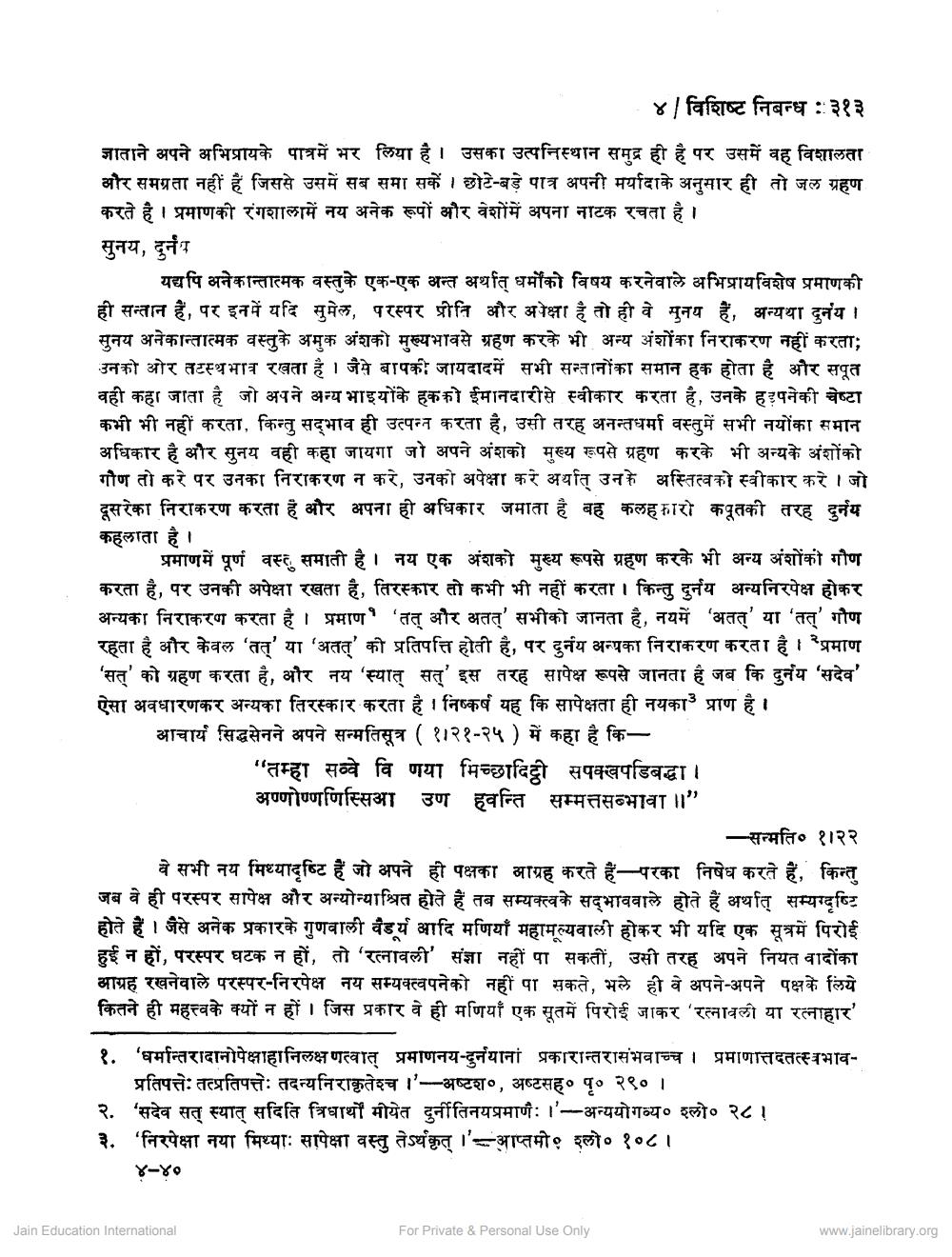________________
४/ विशिष्ट निबन्ध : ३१३
ज्ञाताने अपने अभिप्रायके पात्रमें भर लिया है। उसका उत्पनिस्थान समुद्र ही है पर उसमें वह विशालता
और समग्रता नहीं हैं जिससे उसमें सब समा सकें। छोटे-बड़े पात्र अपनी मर्यादाके अनुसार ही तो जल ग्रहण करते है । प्रमाणको रंगशालामें नय अनेक रूपों और वेशों में अपना नाटक रचता है। सुनय, दुर्नय
यद्यपि अनेकान्तात्मक वस्तके एक-एक अन्त अर्थात् धर्मोको विषय करनेवाले अभिप्रायविशेष प्रमाणकी ही सन्तान हैं, पर इनमें यदि सुमेल, परस्पर प्रीति और अपेक्षा है तो ही वे सुनय हैं, अन्यथा दुर्नय । सुनय अनेकान्तात्मक वस्तुके अमुक अंशको मुख्यभावसे ग्रहण करके भी अन्य अंशोंका निराकरण नहीं करता; उनको ओर तटस्थभाव रखता है । जैसे बापकी जायदादमें सभी सन्तानोंका समान हक होता है और सपूत वही कहा जाता है जो अपने अन्य भाइयोंके हकको ईमानदारीसे स्वीकार करता है, उनके हड़पनेकी चेष्टा कभी भी नहीं करता, किन्तु सद्भाव ही उत्पन्न करता है, उसी तरह अनन्तधर्मा वस्तुमें सभी नयोंका समान अधिकार है और सुनय वही कहा जायगा जो अपने अंशको मुख्य रूपसे ग्रहण करके भी अन्यके अंशोंको गौण तो करे पर उनका निराकरण न करे, उनको अपेक्षा करे अर्थात् उनके अस्तित्वको स्वीकार करे । जो दूसरेका निराकरण करता है और अपना ही अधिकार जमाता है बह कलहकारो कपूतकी तरह दुर्नय कहलाता है।
प्रमाणमें पूर्ण वस्तु समाती है। नय एक अंशको मुख्य रूपसे ग्रहण करके भी अन्य अंशोंको गौण करता है, पर उनकी अपेक्षा रखता है, तिरस्कार तो कभी भी नहीं करता। किन्तु दुर्नय अन्यनिरपेक्ष होकर अन्यका निराकरण करता है। प्रमाण' 'तत् और अतत्' सभीको जानता है, नयमें 'अतत्' या 'तत्' गौण रहता है और केवल 'तत्' या 'अतत्' को प्रतिपत्ति होती है, पर दुर्नय अन्यका निराकरण करता है । प्रमाण 'सत्' को ग्रहण करता है, और नय 'स्यात् सत्' इस तरह सापेक्ष रूपसे जानता है जब कि दुर्नय 'सदेव' ऐसा अवधारणकर अन्यका तिरस्कार करता है । निष्कर्ष यह कि सापेक्षता ही नयका प्राण है। __आचार्य सिद्धसेनने अपने सन्मतिसूत्र ( १।२१-२५ ) में कहा है कि
"तम्हा सव्वे वि णया मिच्छादिट्ठी सपक्खपडिबद्धा। अण्णोण्णणिस्सिआ उण हवन्ति सम्मत्तसब्भावा॥"
-सन्मति० १०२२ वे सभी नय मिथ्यावृष्टि हैं जो अपने ही पक्षका आग्रह करते हैं-परका निषेध करते हैं, किन्तु जब वे ही परस्पर सापेक्ष और अन्योन्याश्रित होते हैं तब सम्यक्त्वके सद्भाववाले होते हैं अर्थात् सम्यग्दृष्टि होते है । जैसे अनेक प्रकारके गुणवाली वैडर्य आदि मणियाँ महामल्यवाली होकर भी यदि एक सूत्र में पिरोई हुई न हों, परस्पर घटक न हों, तो 'रत्नावली' संज्ञा नहीं पा सकतों, उसी तरह अपने नियत वादोंका आग्रह रखनेवाले परस्पर-निरपेक्ष नय सम्यक्त्वपनेको नहीं पा सकते, भले ही वे अपने-अपने पक्ष के लिये कितने ही महत्त्वके क्यों न हों। जिस प्रकार वे ही मणियाँ एक सूतमें पिरोई जाकर 'रत्नावली या रत्नाहार'
१. 'धर्मान्तरादानोपेक्षाहानिलक्षणत्वात प्रमाणनय-दुर्नयानां प्रकारान्तरासंभवाच्च । प्रमाणात्तदतत्स्वभाव
प्रतिपत्तेः तत्प्रतिपत्तेः तदन्यनिराकृतेश्च ।'-अष्टश०, अष्टसह० पृ० २९० । २. 'सदेव सत् स्यात् सदिति विधार्थों मीयेत दुर्नीतिनयप्रमाणः ।'-अन्ययोगव्य० श्लो० २८ । ३. 'निरपेक्षा नया मिथ्याः सापेक्षा वस्तु तेऽर्थकृत् ।'-आप्तमोश्लो० १०८ ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org