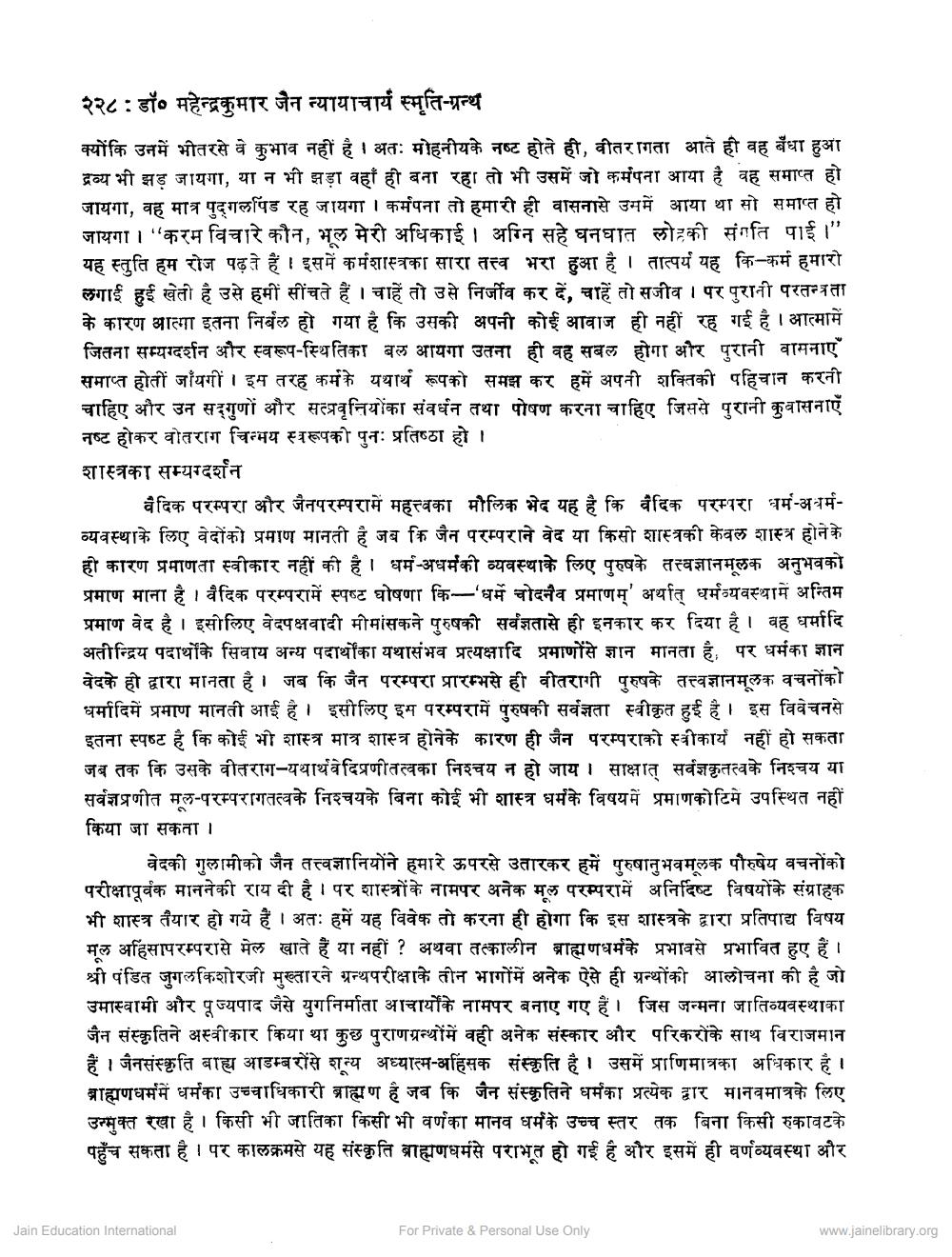________________
२२८ : डॉ० महेन्द्रकुमार जैन न्यायाचार्य स्मृति-ग्रन्थ
बँधा हुआ
क्योंकि उनमें भीतरसे वे कुभाव नहीं है । अतः मोहनीयके नष्ट होते ही, वीतरागता आते ही वह द्रव्य भी झड़ जायगा, या न भी झड़ा वहाँ ही बना रहा तो भी उसमें जो कर्मपना आया है वह समाप्त हो जायगा, वह मात्र पुद्गलपिंड रह जायगा । कर्मपना तो हमारी ही वासनासे उनमें आया था सो समाप्त हो जायगा । " करम विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई । अग्नि सहे घनघात लोहकी संगति पाई । " यह स्तुति हम रोज पढ़ते हैं । इसमें कर्मशास्त्रका सारा तत्त्व भरा हुआ है । तात्पर्य यह कि कर्म हमारी लगाई हुई खेती है उसे हमीं सींचते हैं । चाहें तो उसे निर्जीव कर दें, चाहें तो सजीव । पर पुरानी परतन्त्रता के कारण आत्मा इतना निर्बल हो गया है कि उसकी अपनी कोई आवाज ही नहीं रह गई है । आत्मामें जितना सम्यग्दर्शन और स्वरूप स्थितिका बल आयगा उतना ही वह सबल होगा और पुरानी वामनाएँ समाप्त होती जायगी । इस तरह कर्मके यथार्थ रूपको समझ कर हमें अपनी शक्तिकी पहिचान करनी चाहिए और उन सद्गुणों और सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन तथा पोषण करना चाहिए जिससे पुरानी कुवासनाएँ नष्ट होकर वीतराग चिन्मय स्वरूपकी पुनः प्रतिष्ठा हो ।
शास्त्रका सम्यग्दर्शन
वैदिक परम्परा और जैनपरम्परा में महत्त्वका मौलिक भेद यह है कि वैदिक परम्परा धर्म-अधर्मव्यवस्थाके लिए वेदोंको प्रमाण मानती है जब कि जैन परम्पराने वेद या किसी शास्त्रकी केवल शास्त्र होने के ही कारण प्रमाणता स्वीकार नहीं की है । धर्म-अधर्मकी व्यवस्था के लिए पुरुष के तत्त्वज्ञानमूलक अनुभवको प्रमाण माना है । वैदिक परम्परामें स्पष्ट घोषणा कि - 'धर्मे चोदनैव प्रमाणम्' अर्थात् धर्मव्यवस्था में अन्तिम प्रमाण वेद है । इसीलिए वेदपक्षवादी मीमांसकने पुरुषकी सर्वज्ञतासे ही इनकार कर दिया है । वह धर्मादि अतीन्द्रिय पदार्थोंके सिवाय अन्य पदार्थोंका यथासंभव प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे ज्ञान मानता है, पर धर्मका ज्ञान वेदके ही द्वारा मानता है। जब कि जैन परम्परा प्रारम्भसे ही वीतरागी पुरुषके तत्त्वज्ञानमूलक वचनोंको धर्मादिमें प्रमाण मानती आई है । इसीलिए इस परम्परामें पुरुषकी सर्वज्ञता स्वीकृत हुई है । इस विवेचन से इतना स्पष्ट है कि कोई भी शास्त्र मात्र शास्त्र होनेके कारण ही जैन परम्पराको स्वीकार्य नहीं हो सकता जब तक कि उसके वीतराग - यथार्थवेदिप्रणीतत्वका निश्चय न हो जाय । साक्षात् सर्वज्ञकृतत्व के निश्चय या सर्वज्ञप्रणीत मूल परम्परागतत्वके निश्चयके बिना कोई भी शास्त्र धर्मके विषय में प्रमाणकोटिमे उपस्थित नहीं किया जा सकता ।
वेदको गुलामीको जैन तत्त्वज्ञानियोंने हमारे ऊपरसे उतारकर हमें पुरुषानुभवमूलक पौरुषेय वचनों को परीक्षापूर्वक माननेकी राय दी है । पर शास्त्रों के नामपर अनेक मूल परम्परामें अनिर्दिष्ट विषयोंके संग्राहक भी शास्त्र तैयार हो गये हैं । अतः हमें यह विवेक तो करना ही होगा कि इस शास्त्र के द्वारा प्रतिपाद्य विषय मूल अहिंसापरम्परासे मेल खाते हैं या नहीं ? अथवा तत्कालीन ब्राह्मणधर्मके प्रभावसे प्रभावित हुए हैं। श्री पंडित जुगलकिशोरजी मुख्तारने ग्रन्थपरीक्षाके तीन भागों में अनेक ऐसे ग्रन्थोंकी आलोचना की है जो जिस जन्मना जातिव्यवस्थाका
स्वामी और पूज्यपाद जैसे युगनिर्माता आचार्योंके नामपर बनाए गए हैं। जैन संस्कृतिने अस्वीकार किया था कुछ पुराणग्रन्थोंमें वही अनेक संस्कार और परिकरोंके साथ विराजमान हैं । जैनसंस्कृति बाह्य आडम्बरोंसे शून्य अध्यात्म-अहिंसक संस्कृति है । उसमें प्राणिमात्रका अधिकार है । ब्राह्मणधर्म में धर्मका उच्चाधिकारी ब्राह्मण है जब कि जैन संस्कृतिने धर्मका प्रत्येक द्वार मानवमात्र के लिए उन्मुक्त रखा है। किसी भी जातिका किसी भी वर्णका मानव धर्मके उच्च स्तर तक बिना किसी रुकावट के पहुँच सकता है । पर कालक्रमसे यह संस्कृति ब्राह्मणधर्मसे पराभूत हो गई है और इसमें ही वर्णव्यवस्था और
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org