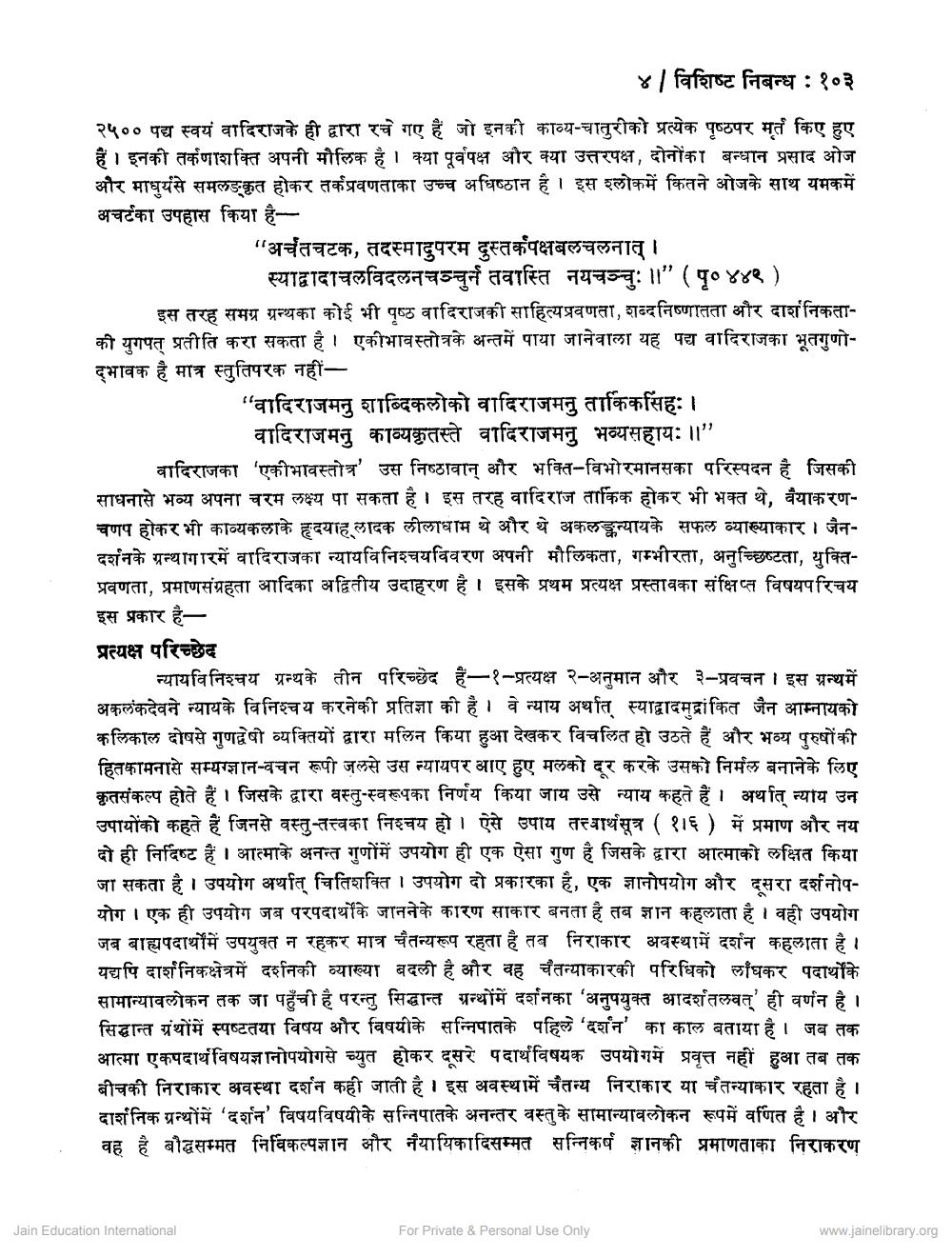________________
४ / विशिष्ट निबन्ध : १०३ २५०० पद्य स्वयं वादिराजके ही द्वारा रचे गए हैं जो इनकी काव्य-चातुरीको प्रत्येक पृष्ठपर मृर्त किए हुए हैं । इनकी तर्कणाशक्ति अपनी मौलिक है । क्या पूर्वपक्ष और क्या उत्तरपक्ष, दोनोंका बन्धान प्रसाद ओज और माधुर्य से समलङ्कृत होकर तर्कप्रवणताका उच्च अधिष्ठान है । इस श्लोकमें कितने ओजके साथ यमकमें अचका उपहास किया है
"अर्चतचटक, तदस्मादुपरम दुस्तर्कपक्षबलचलनात् ।
स्याद्वादाचलविदलनचञ्चुर्न तवास्ति नयचञ्चुः ॥” ( पृ० ४४९ )
इस तरह समग्र ग्रन्थका कोई भी पृष्ठ वादिराजकी साहित्यप्रवणता, शब्दनिष्णातता और दार्शनिकता - की युगपत् प्रतीति करा सकता है । एकीभावस्तोत्रके अन्त में पाया जानेवाला यह पद्य वादिराजका भूतगुणोद्भावक है मात्र स्तुतिपरक नहीं
" वादिराजमनु शाब्दिकलोको वादिराजमनु तार्किक सिंहः । वादिराजमनु काव्यकृतस्ते वादिराजमनु भव्य सहायः ॥ "
वादिराजका 'एकीभावस्तोत्र' उस निष्ठावान् और भक्ति-विभोरमानसका परिस्पदन है जिसकी साधनासे भव्य अपना चरम लक्ष्य पा सकता है। इस तरह वादिराज तार्किक होकर भी भक्त थे, वैयाकरणचप होकर भी काव्यकलाके हृदयाह लादक लीलाधाम थे और थे अकलङ्कन्याय के सफल व्याख्याकार । जैनदर्शनके ग्रन्थागारमें वादिराजका न्यायविनिश्चयविवरण अपनी मौलिकता, गम्भीरता, अनुच्छिष्टता, युक्तिप्रवणता प्रमाणसंग्रहता आदिका अद्वितीय उदाहरण है। इसके प्रथम प्रत्यक्ष प्रस्तावका संक्षिप्त विषयपरिचय इस प्रकार है
प्रत्यक्ष परिच्छेद
न्यायविनिश्चय ग्रन्थ के तीन परिच्छेद हैं- १ - प्रत्यक्ष २ - अनुमान और ३ - प्रवचन । इस ग्रन्थ में अकलंकदेवने न्यायके विनिश्चय करनेकी प्रतिज्ञा की है । वे न्याय अर्थात् स्याद्वादमुद्रांकित जैन आम्नायको कलिकाल दोषसे गुणद्वेषी व्यक्तियों द्वारा मलिन किया हुआ देखकर विचलित हो उठते हैं और भव्य पुरुषों की हितकामनासे सम्यग्ज्ञान-वचन रूपी जलसे उस न्यायपर आए हुए मलको दूर करके उसको निर्मल बनानेके लिए कृतसंकल्प होते हैं । जिसके द्वारा वस्तु-स्वरूपका निर्णय किया जाय उसे न्याय कहते हैं । अर्थात् न्याय उन उपायोंको कहते हैं जिनसे वस्तु तत्त्वका निश्चय हो । ऐसे उपाय तत्त्वार्थसूत्र ( १६ ) में प्रमाण और नय दो ही निर्दिष्ट हैं | आत्माके अनन्त गुणोंमें उपयोग ही एक ऐसा गुण है जिसके द्वारा आत्माको लक्षित किया जा सकता है । उपयोग अर्थात् चितिशक्ति | उपयोग दो प्रकारका है, एक ज्ञानोपयोग और दूसरा दर्शनोपयोग । एक ही उपयोग जब परपदार्थोंके जाननेके कारण साकार बनता है तब ज्ञान कहलाता है । वही उपयोग जब बाह्यपदार्थोंमें उपयुक्त न रहकर मात्र चैतन्यरूप रहता है तब निराकार अवस्थामें दर्शन कहलाता है । यद्यपि दार्शनिक क्षेत्र में दर्शनकी व्याख्या बदली है और वह चैतन्याकारकी परिधिको लाँघकर पदार्थोंके सामान्यावलोकन तक जा पहुँची है परन्तु सिद्धान्त ग्रन्थोंमें दर्शनका 'अनुपयुक्त आदर्शतलवत्' ही वर्णन है । सिद्धान्त ग्रंथों में स्पष्टतया विषय और विषयीके सन्निपातके पहिले 'दर्शन' का काल बताया है। जब तक आत्मा एकपदार्थविषयज्ञानोपयोगसे च्युत होकर दूसरे पदार्थविषयक उपयोग में प्रवृत्त नहीं हुआ तब तक बीचकी निराकार अवस्था दर्शन कही जाती है । इस अवस्थामें चैतन्य निराकार या चैतन्याकार रहता है । दार्शनिक ग्रन्थों में 'दर्शन' विषयविषयीके सन्निपातके अनन्तर वस्तु के सामान्यावलोकन रूपमें वर्णित है । और वह है बौद्धसम्मत निर्विकल्पज्ञान और नैयायिकादिसम्मत सन्निकर्ष ज्ञानकी प्रमाणताका निराकरण
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org