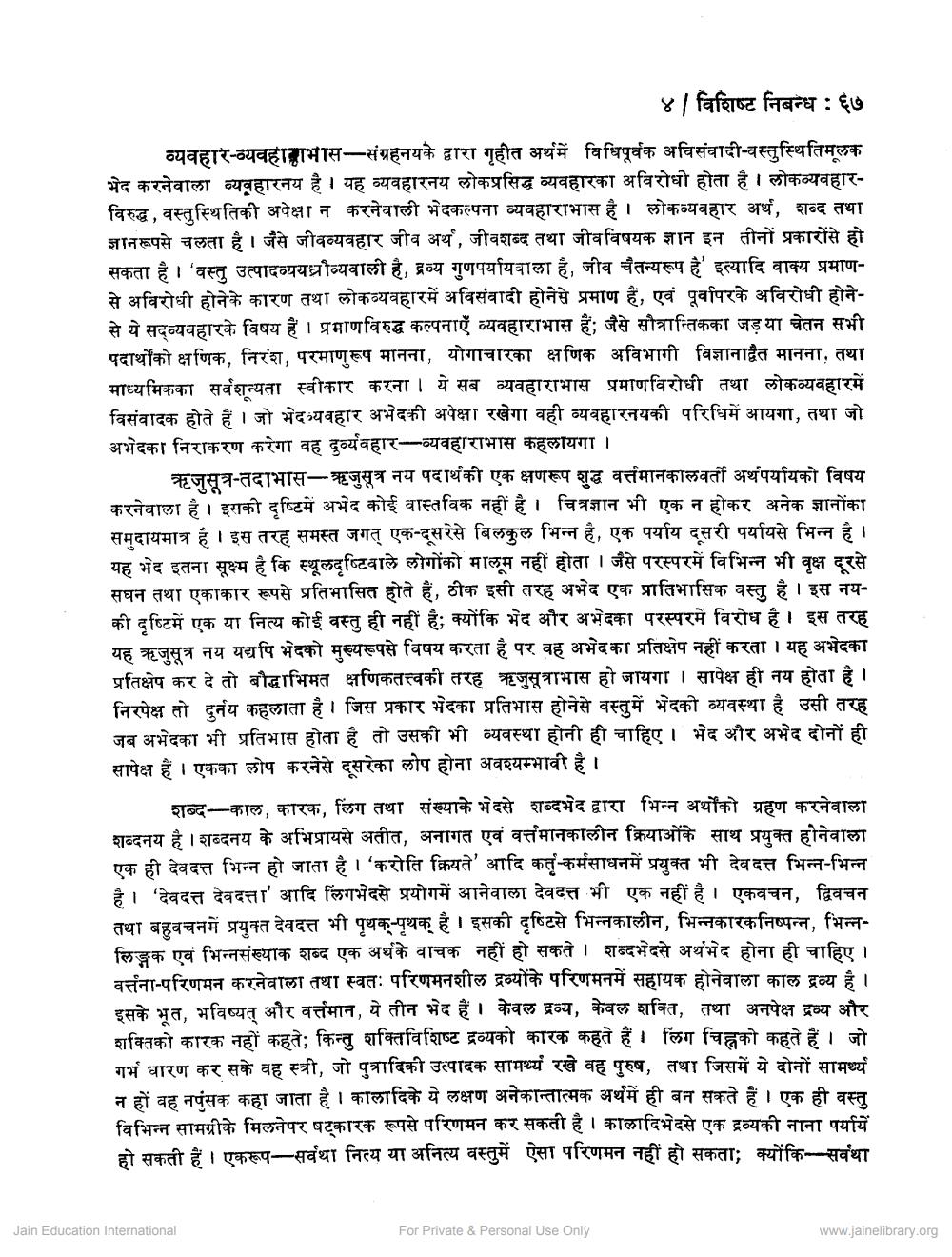________________
४ / विशिष्ट निबन्ध : ६७
व्यवहार-व्यवहााभास - संग्रहनय के द्वारा गृहीत अर्थ में विधिपूर्वक अविसंवादी वस्तुस्थितिमूलक भेद करनेवाला व्यवहारनय है । यह व्यवहारनय लोकप्रसिद्ध व्यवहारका अविरोधी होता है । लोकव्यवहारविरुद्ध, वस्तुस्थितिकी अपेक्षा न करनेवाली भेदकल्पना व्यवहाराभास है । लोकव्यवहार अर्थ, शब्द तथा ज्ञानरूपसे चलता है । जैसे जीवव्यवहार जीव अर्थ, जीवशब्द तथा जीवविषयक ज्ञान इन तीनों प्रकारोंसे हो सकता है । 'वस्तु उत्पादव्ययश्रीन्यवाली है, द्रव्य गुणपर्यायवाला है, जीव चैतन्यरूप है' इत्यादि वाक्य प्रमाणसे अविरोधी होने के कारण तथा लोकव्यवहारमें अविसंवादी होनेसे प्रमाण हैं, एवं पूर्वापर के अविरोधी होनेसे ये सद्व्यवहारके विषय | प्रमाणविरुद्ध कल्पनाएँ व्यवहाराभास हैं; जैसे सौत्रान्तिकका जड़ या चेतन सभी पदार्थोंको क्षणिक, निरंश, परमाणुरूप मानना, योगाचारका क्षणिक अविभागी विज्ञानाद्वैत मानना, तथा माध्यमिकका सर्वशून्यता स्वीकार करना । ये सब व्यवहाराभास प्रमाणविरोधी तथा लोकव्यवहारमें विसंवादक होते हैं । जो भेदव्यवहार अभेदकी अपेक्षा रखेगा वही व्यवहारनयकी परिधि में आयगा, तथा जो अभेदका निराकरण करेगा वह दुर्व्यवहार - व्यवहाराभास कहलायेगा ।
ऋजुसूत्र - तदाभास—ऋजुसूत्र नय पदार्थकी एक क्षणरूप शुद्ध वर्त्तमानकालवर्ती अर्थपर्यायको विषय करनेवाला है । इसकी दृष्टिमें अभेद कोई वास्तविक नहीं है । चित्रज्ञान भी एक न होकर अनेक ज्ञानोंका समुदायमात्र है । इस तरह समस्त जगत् एक-दूसरेसे बिलकुल भिन्न है, एक पर्याय दूसरी पर्यायसे भिन्न है । यह भेद इतना सूक्ष्म है कि स्थूलदृष्टिवाले लोगोंको मालूम नहीं होता । जैसे परस्परमें विभिन्न भी वृक्ष दूरसे सघन तथा एकाकार रूपसे प्रतिभासित होते हैं, ठीक इसी तरह अभेद एक प्रातिभासिक वस्तु है । इस नयकी दृष्टिमें एक या नित्य कोई वस्तु ही नहीं है; क्योंकि भेद और अभेदका परस्पर में विरोध है । इस तरह यह ऋजुसूत्र नय यद्यपि भेदको मुख्यरूपसे विषय करता है पर वह अभेदका प्रतिक्षेप नहीं करता । यह अभेदका प्रतिक्षेप कर दे तो बौद्धाभिमत क्षणिकतत्त्वकी तरह ऋजुसूत्राभास हो जायगा । सापेक्ष ही नय होता है । निरपेक्ष तो दुर्नय कहलाता है। जिस प्रकार भेदका प्रतिभास होनेसे वस्तुमें भेदको व्यवस्था है उसी तरह जब अभेदका भी प्रतिभास होता है तो उसकी भी व्यवस्था होनी ही चाहिए । भेद और अभेद दोनों ही सापेक्ष हैं । एकका लोप करनेसे दूसरेका लोप होना अवश्यम्भावी है ।
शब्द -काल, कारक, लिंग तथा संख्याके भेदसे शब्दभेद द्वारा भिन्न अर्थोंको ग्रहण करनेवाला शब्दtय है । शब्दय के अभिप्रायसे अतीत, अनागत एवं वर्त्तमानकालीन क्रियाओंके साथ प्रयुक्त होनेवाला एक ही देवदत्त भिन्न हो जाता है । 'करोति क्रियते' आदि कर्तृ कर्मसाधनमें प्रयुक्त भी देवदत्त भिन्न-भिन्न है । 'देवदत्त देवदत्ता' आदि लिंगभेदसे प्रयोगमें आनेवाला देवदत्त भी एक नहीं है । एकवचन, द्विवचन तथा बहुवचन में प्रयुक्त देवदत्त भी पृथक्-पृथक् है । इसकी दृष्टिसे भिन्नकालीन, भिन्नकारक निष्पन्न, भिन्नलिङ्गक एवं भिन्नसंख्याक शब्द एक अर्थके वाचक नहीं हो सकते । शब्दभेदसे अर्थभेद होना ही चाहिए । वर्त्तना परिणमन करनेवाला तथा स्वतः परिणमनशील द्रव्योंके परिणमनमें सहायक होनेवाला काल द्रव्य है । इसके भूत, भविष्यत् और वर्तमान, ये तीन भेद हैं। केवल द्रव्य, केवल शक्ति, तथा अनपेक्ष द्रव्य और शक्तिको कारक नहीं कहते; किन्तु शक्तिविशिष्ट द्रव्यको कारक कहते | लिंग चिह्नको कहते हैं । जो गर्भ धारण कर सके वह स्त्री, जो पुत्रादिकी उत्पादक सामथ्यं रखे वह पुरुष तथा जिसमें ये दोनों सामर्थ्य न हों वह नपुंसक कहा जाता है । कालादिके ये लक्षण अनेकान्तात्मक अर्थ में ही बन सकते हैं। एक ही वस्तु विभिन्न सामग्री मिलनेपर षट्कारक रूपसे परिणमन कर सकती है । कालादिभेदसे एक द्रव्यकी नाना पर्यायें हो सकती हैं । एकरूप - सर्वथा नित्य या अनित्य वस्तुमें ऐसा परिणमन नहीं हो सकता; क्योंकि सर्वथा
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org