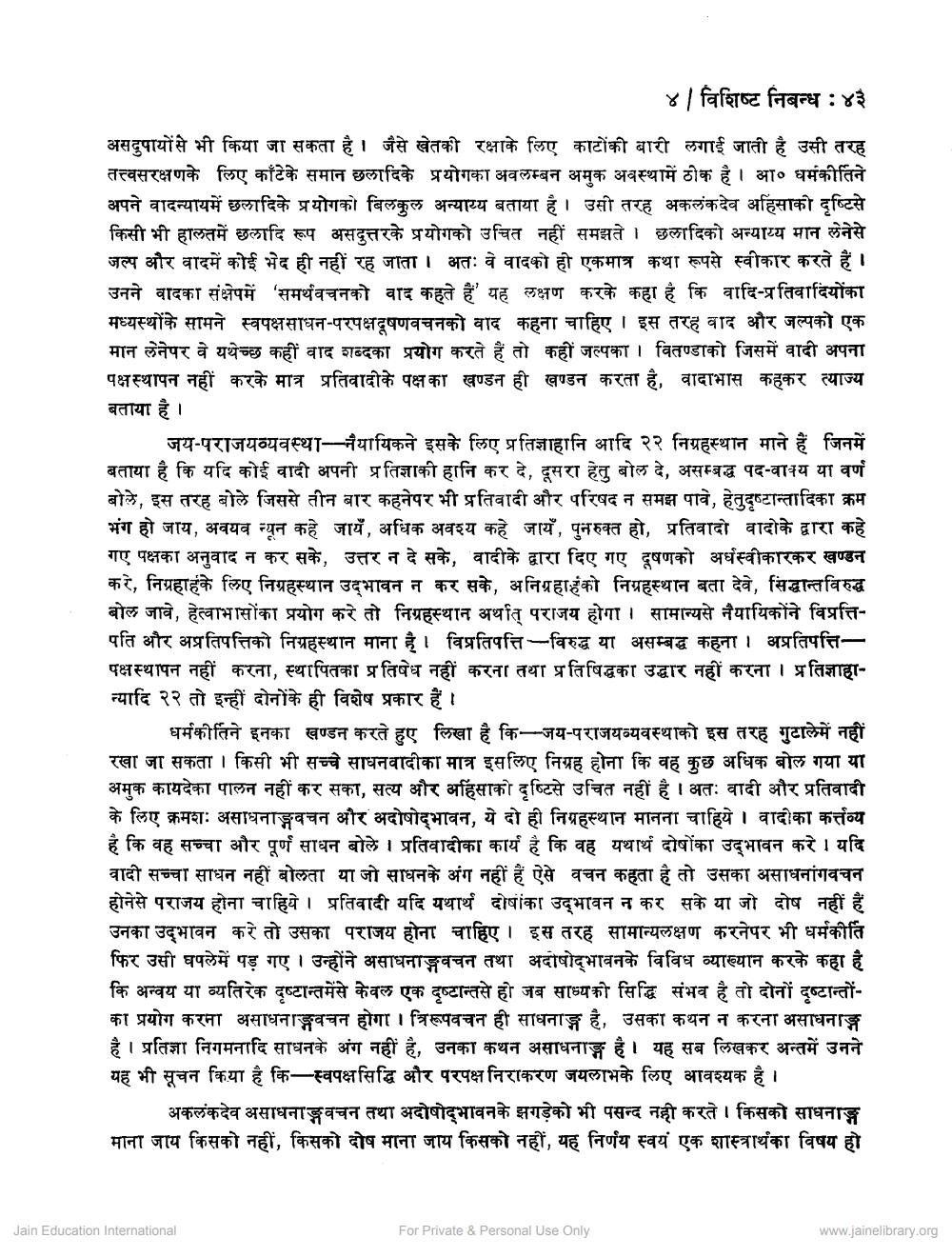________________
४ / विशिष्ट निबन्ध : ४३
असदुपायों से भी किया जा सकता है। जैसे खेतकी रक्षाके लिए काटोंकी बारी लगाई जाती है उसी तरह तत्त्वसरक्षणके लिए काँटेके समान छलादिके प्रयोगका अवलम्बन अमक अवस्थामें ठीक है। आ० धर्मकीर्तिने अपने वादन्यायमें छलादिके प्रयोगको बिलकूल अन्याय्य बताया है। उसी तरह अकलंकदेव अहिंसाको दृष्टिसे किसी भी हालतमें छलादि रूप असदुत्तरके प्रयोगको उचित नहीं समझते। छलादिको अन्याय्य मान लेनेसे जल्प और वादमें कोई भेद ही नहीं रह जाता। अतः वे वादको ही एकमात्र कथा रूपसे स्वीकार करते हैं। उनने वादका संक्षेपमें 'समर्थवचनको वाद कहते हैं' यह लक्षण करके कहा है कि वादि-प्रतिवादियोंका मध्यस्थोंके सामने स्वपक्षसाधन-परपक्षदूषणवचनको वाद कहना चाहिए । इस तरह वाद और जल्पको एक मान लेनेपर वे यथेच्छ कहीं वाद शब्दका प्रयोग करते हैं तो कहीं जल्पका। वितण्डाको जिसमें वादी अपना पक्षस्थापन नहीं करके मात्र प्रतिवादीके पक्षका खण्डन ही खण्डन करता है, वादाभास कहकर त्याज्य बताया है।
जय-पराजयव्यवस्था-नैयायिकने इसके लिए प्रतिज्ञाहानि आदि २२ निग्रहस्थान माने हैं जिनमें बताया है कि यदि कोई वादी अपनी प्रतिज्ञाकी हानि कर दे, दूसरा हेतु बोल दे, असम्बद्ध पद-वाक्य या वर्ण बोले, इस तरह बोले जिससे तीन बार कहनेपर भी प्रतिवादी और परिषद न समझ पावे, हेतुदृष्टान्तादिका क्रम भंग हो जाय, अवयव न्यून कहे जायँ, अधिक अवश्य कहे जायँ, पुनरुक्त हो, प्रतिवादो वादोके द्वारा कहे गए पक्षका अनुवाद न कर सके, उत्तर न दे सके, वादीके द्वारा दिए गए दूषणको अर्धस्वीकारकर खण्डन करे, निग्रहाईके लिए निग्रहस्थान उदभावन न कर सके, अनिग्रहाईको निग्रहस्थान बता देवे, सिद्धान्ता बोल जावे, हेत्वाभासोंका प्रयोग करे तो निग्रहस्थान अर्थात पराजय होगा। सामान्यसे नैयायिकोंने वित्तिपति और अप्रतिपत्तिको निग्रहस्थान माना है। विप्रतिपत्ति-विरुद्ध या असम्बद्ध कहना। अप्रतिपत्तिपक्षस्थापन नहीं करना, स्थापितका प्रतिषेध नहीं करना तथा प्रतिषिद्धका उद्धार नहीं करना । प्रतिज्ञाहान्यादि २२ तो इन्हीं दोनोंके ही विशेष प्रकार हैं।
धर्मकीर्तिने इनका खण्डन करते हुए लिखा है कि-जय-पराजयव्यवस्थाको इस तरह गुटालेमें नहीं रखा जा सकता। किसी भी सच्चे साधनवादीका मात्र इसलिए निग्रह होना कि वह कुछ अधिक बोल गया या अमुक कायदेका पालन नहीं कर सका, सत्य और अहिंसाको दृष्टिसे उचित नहीं है । अतः वादी और प्रतिवादी के लिए क्रमशः असाधनाङ्गवचन और अदोषोद्भावन, ये दो ही निग्रहस्थान मानना चाहिये । वादीका कर्तव्य है कि वह सच्चा और पूर्ण साधन बोले । प्रतिवादीका कार्य है कि वह यथार्थ दोषोंका उद्भावन करे । यदि वादी सच्चा साधन नहीं बोलता या जो साधनके अंग नहीं हैं ऐसे वचन कहता है तो उसका असाधनांगवचन होनेसे पराजय होना चाहिये । प्रतिवादी यदि यथार्थ दोषांका उद्भावन न कर सके या जो दोष नहीं हैं उनका उद्भावन करे तो उसका पराजय होना चाहिए। इस तरह सामान्यलक्षण करनेपर भी धर्मकीर्ति फिर उसी घपलेमें पड़ गए। उन्होंने असाधनाङ्गवचन तथा अदोषोद्भावनके विविध व्याख्यान करके कहा है कि अन्वय या व्यतिरेक दृष्टान्तमेंसे केवल एक दृष्टान्तसे हो जब साध्यको सिद्धि संभव है तो दोनों दृष्टान्तोंका प्रयोग करना असाधनाङ्गवचन होगा। त्रिरूपवचन ही साधनाङ्ग है, उसका कथन न करना असाधनाङ्ग है । प्रतिज्ञा निगमनादि साधनके अंग नहीं है, उनका कथन असाधनाङ्ग है। यह सब लिखकर अन्तमें उनने यह भी सूचन किया है कि स्वपक्षसिद्धि और परपक्ष निराकरण जयलाभके लिए आवश्यक है।
अकलंकदेव असाधनाङ्गवचन तथा अदोषोभावनके झगड़ेको भी पसन्द नही करते । किसको साधनाङ्ग माना जाय किसको नहीं, किसको दोष माना जाय किसको नहीं, यह निर्णय स्वयं एक शास्त्रार्थका विषय हो
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org