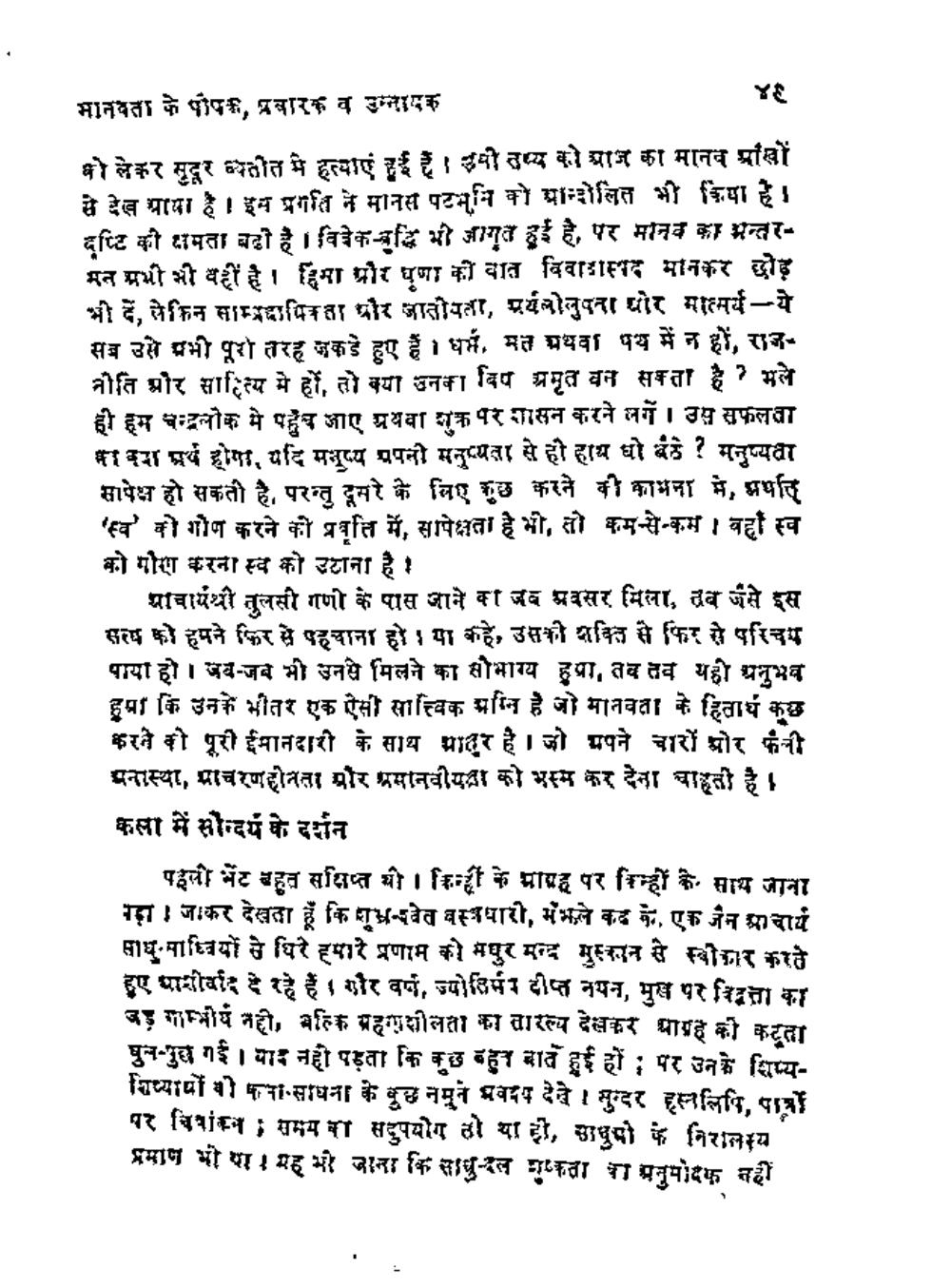________________
भानवता के पोपक, प्रबारक व उन्नायक
को लेकर सुदूर बतीत में हत्याएं हुई है। इसी तथ्य को प्राज का मानव प्रांखों से देख पाया है। इस प्रति ने मानस पटभूमि को प्रान्दोलित भी किया है। दृष्टि की क्षमता बढ़ी है । विवेक-द्धि भी जागत हुई है, पर मानव का अन्तरमन प्रभी भी वहीं है। हिमा और पणा की वात विवादास्पद मानकर छोड़ भी दें, लेकिन साम्प्रदायिकता और जातीरता, प्रर्यलोलुपना घोर मात्मर्य-ये सब उसे अभी पूरी तरह जकडे हुए हैं। धर्म, मत अथवा पथ में न हो, राजनौति और साहित्य मे हों, तो क्या उनका दिप अमृत बन सकता है ? मले ही हम चन्द्रलोक मे पहुँच आए अथवा शुक्र पर शासन करने लगे। उस सफलता माश अर्थ होगा, यदि मभूप्य प्रपनी मनुप्यता से ही हाथ धो बैठे ? मनुष्यता सापेक्ष हो सकती है, परन्तु दूसरे के लिए कुछ करने की कामना में, अपति 'स्व' को गौण करने को प्रति में, सापेक्षता है भी, तो कम-से-कम । वहाँ स्व को गोरा करना स्व को उठाना है।
प्राचार्यश्री तुलसी गणो के पास जाने का जब अवसर मिला, तव जैसे इस सत्य को हमने फिर से पहचाना हो या कहे, उसकी शक्ति से फिर से परिचय पाया हो। जब-जब भी उनसे मिलने का सौभाग्य हुप्रा, तव तव यही अनुभव हुप्रा कि उनके भीतर एक ऐसी सात्त्विक अग्नि है जो मानवता के हितार्थ कुछ करने को पूरी ईमानदारी के साथ माहर है । जो अपने चारों ओर फैली अनास्था, माचरण होनता और प्रमानवीयता को भस्म कर देना चाहती है। कला में सौन्दर्य के दर्शन
पहली भेंट बहुत सक्षिप्त यो । किन्हीं के मारह पर किन्हीं के साथ जाना पड़ा। जाकर देखता हूँ कि शुभ-पवेत वस्त्रधारी, मझले कद में, एक जैन प्राचार्य साधु माध्वियों से घिरे हमारे प्रणाम को मधुर मन्द मुस्कान से स्वीकार करते हुए भाशीर्वाद दे रहे हैं । गौर वर्ण, ज्योतिर्मर दीप्त नयन, मुख पर विद्वत्ता का उड़ गाम्भीर्य नही, बल्कि ग्रहणशीलता का तारल्य देखकर भागह की कटता पुन-पुछ गई। याद नहीं पड़ता कि कुछ बहुत बात हुई हों; पर उनके शिष्यशिध्यायों को कना-साधना के कुछ नमूने अवश्य देते । सुन्दर हस्तलिपि, पात्रों पर नि ; समय का सदुपयोग हो था ही, साधुमो के निरालस्य प्रमाण भी था । मह भी जाना कि साघु-दल सकता का अनुमोदफ नहीं