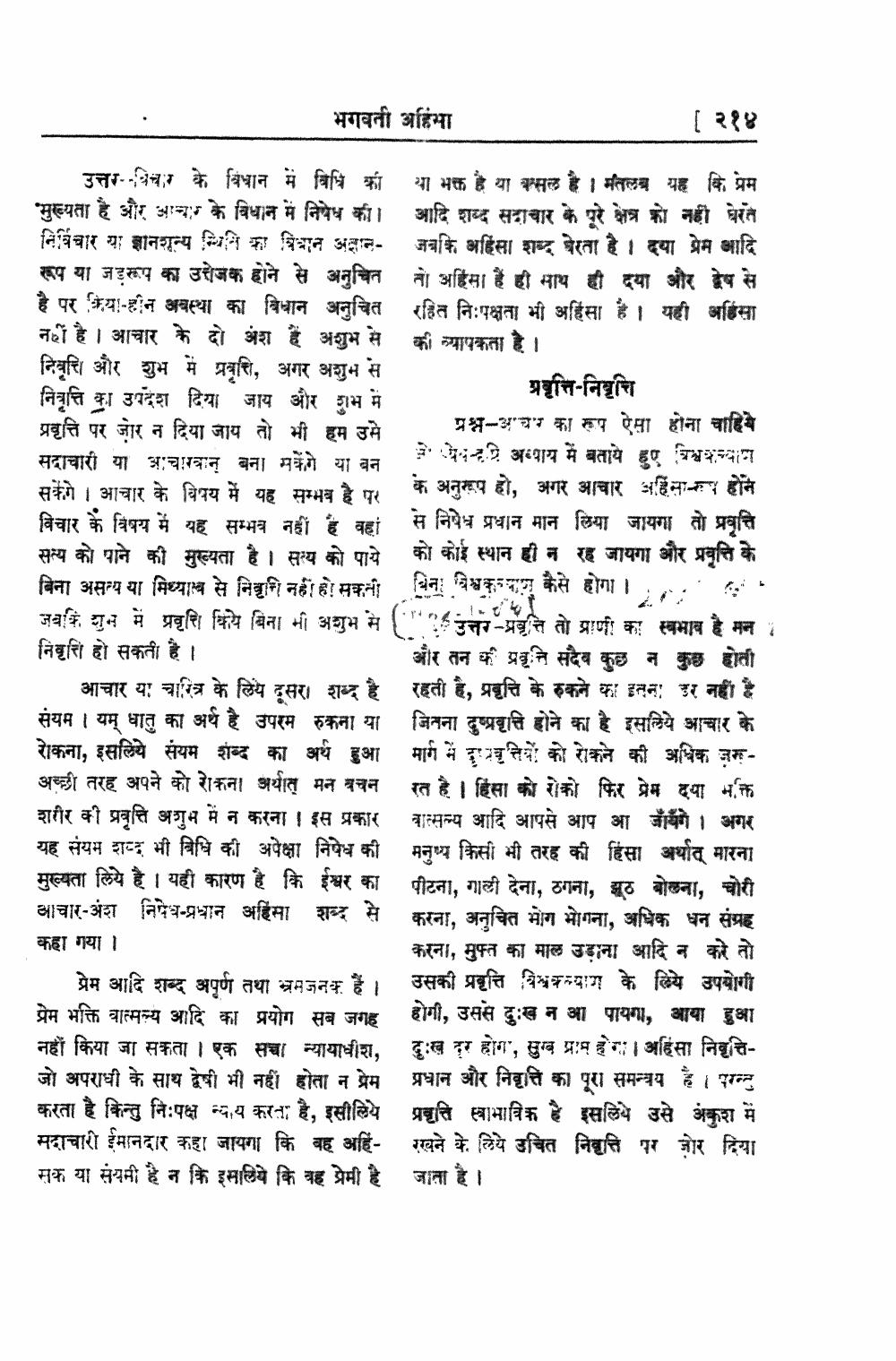________________
भगवती अहिंसा
उत्तर--विचार के विधान में विधि की मुख्यता है और अचार के विधान में निषेध की। निर्विचार या ज्ञानशून्य स्थिति का विधान अज्ञानरूप या जड़रूप का उत्तेजक होने से अनुचित है परक्रिया हीन अवस्था का विधान अनुचित नहीं है । आचार के दो अंश हैं अशुभ निवृत्ति और शुभ में प्रवृति, अगर अशुभ स निवृत्ति का उपदेश दिया जाय और शुभ में प्रवृत्ति पर जोर न दिया जाय तो भी हम उसे सदाचारी या आचारवान् बना सकेंगे या बन सकेंगे। आचार के विषय में यह सम्भव है पर विचार के विषय में यह सम्भव नहीं है वहां सत्य को पाने की मुख्यता है । सत्य को पाये बिना असत्य या मिध्यात्व से निवृति नहीं हो सकती जबकि शुभ में प्रवृति किये बिना भी अशुभ से निवृत्ति हो सकती है ।
(
आचार या चारित्र के लिये दूसरा शब्द है संयम । यम् धातु का अर्थ है उपरम रुकना या रोकना, इसलिये संयम शब्द का अर्थ हुआ अच्छी तरह अपने को रोकना अर्थात् मन वचन शरीर की प्रवृत्ति अशुभ में न करना । इस प्रकार यह संयम शब्द भी विधि की अपेक्षा निषेध की मुख्यता लिये है । यही कारण है कि ईश्वर का आचार- अंश निषेध-प्रधान अहिंसा शब्द से कहा गया ।
।
[ २१४
या भक्त है या है । तलब यह कि प्रेम आदि शब्द सदाचार के पूरे क्षेत्र को नहीं घेरते जबकि अहिंसा शब्द घेरता है । दया प्रेम आदि तो अहिंसा हैं ही साथ ही दया और द्वेष से रहित निःपक्षता भी अहिंसा है। यही अहिंसा की व्यापकता है ।
प्रेम आदि शब्द अपूर्ण तथा भ्रमजनक हैं । प्रेम भक्ति वात्सल्य आदि का प्रयोग सब जगह नहीं किया जा सकता । एक सच्चा न्यायाधीश, जो अपराधी के साथ द्वेषी भी नहीं होता न प्रेम करता है किन्तु निःपक्ष न्याय करता है, इसीलिये सदाचारी ईमानदार कहा जायगा कि वह अहिंसक या संयमी है न कि इसलिये कि वह प्रेमी है
प्रवृत्ति - निवृति
प्रश्न- अचर का रूप ऐसा होना चाहिये वन्द अध्याय में बताये हुए विश्ववाण के अनुरूप हो, अगर आचार अहिंसक होने से निषेव प्रधान मान लिया जायगा तो प्रवृत्ति को कोई स्थान ही न रह जायगा और प्रवृत्ति के बिना विश्वका कैसे होगा ।
उत्तर-प्रवृत्ति
मन
और तन की प्रवृत्ति सदैव कुछ न कुछ होती रहती है, प्रवृत्ति के रुकने का इतना डर नहीं है जितना दुष्प्रवृत्ति होने का है इसलिये आचार के मार्ग में दुष्प्रवृत्तियों को रोकने की अधिक ज़रूरत है। हिंसा को रोको फिर प्रेम दया भक्ति वात्सल्य आदि आपसे आप आ जायेंगे। अगर
मनुष्य किसी भी तरह की हिंसा अर्थात् मारना पीटना, गाली देना, ठगना, झूठ बोलना, चोरी करना, अनुचित भोग भोगना, अधिक धन संग्रह करना, मुफ्त का माल उड़ाना आदि न करे तो उसकी प्रवृत्ति विश्वकल्याण के लिये उपयोगी होगी, उससे दुःख न आ पायगा, आया हुआ दुःख दूर होगा, सुख प्राम होगा । अहिंसा निवृत्तिप्रधान और निवृत्ति का पूरा समन्वय है । परन्तु प्रवृत्ति स्वाभाविक है इसलिये उसे अंकुश में रखने के लिये उचित निवृत्ति पर जोर दिया जाता है।