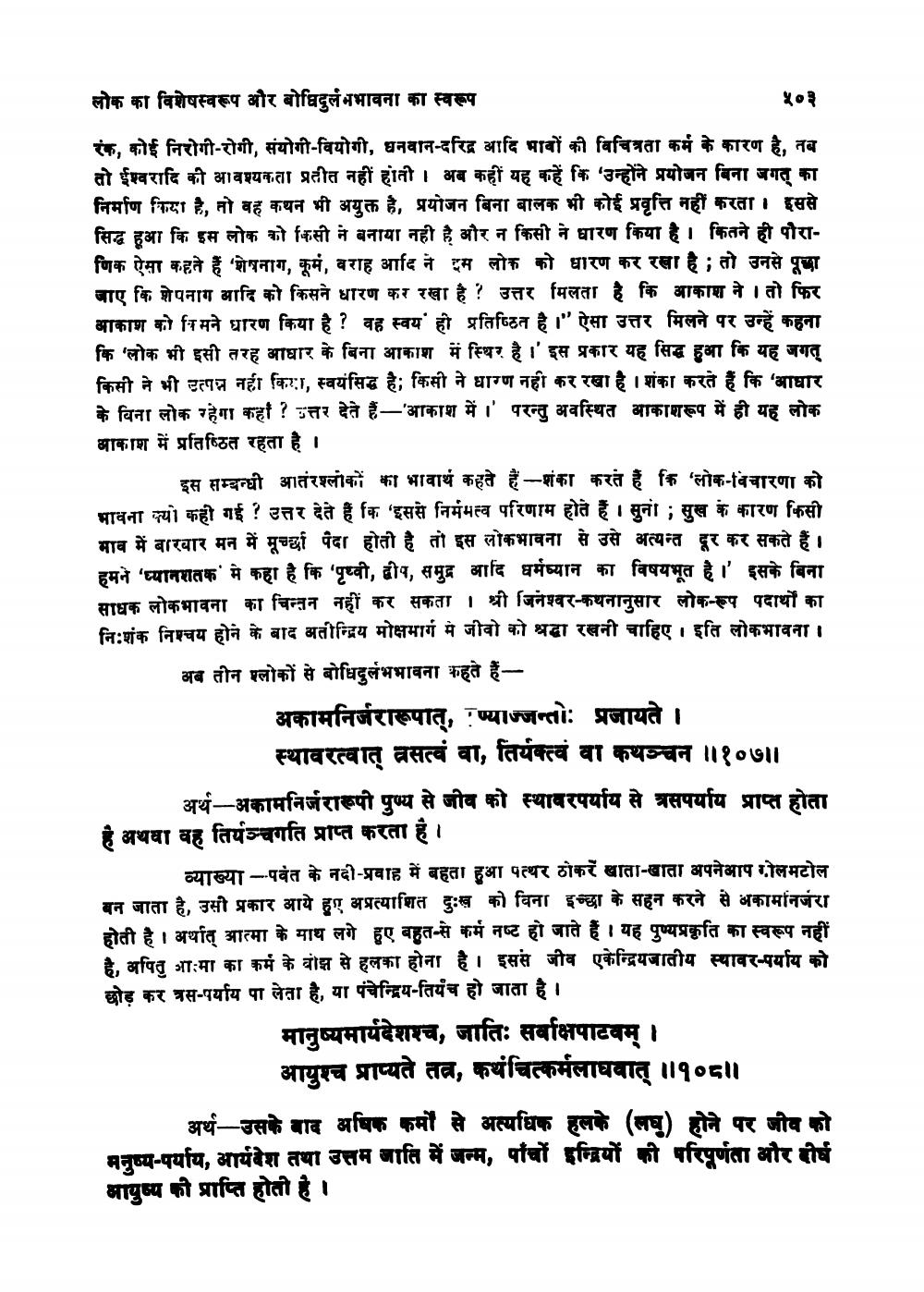________________
लोक का विशेषस्वरूप और बोधिदुर्लभभावना का स्वरूप
५०३ रंक, कोई निरोगी-रोगी, संयोगी-वियोगी, धनवान-दरिद्र आदि भावों की विचित्रता कर्म के कारण है, तब तो ईश्वरादि की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। अब कहीं यह कहें कि 'उन्होंने प्रयोजन बिना जगत् का निर्माण किया है, तो वह कथन भी अयुक्त है, प्रयोजन बिना बालक भी कोई प्रवृत्ति नहीं करता। इससे सिद्ध हुआ कि इस लोक को किसी ने बनाया नही है और न किसी ने धारण किया है। कितने ही पौराणिक ऐसा कहते हैं 'शेषनाग, कूर्म, बराह आदि ने दम लोक को धारण कर रखा है; तो उनसे पूछा जाए कि शेषनाग आदि को किसने धारण कर रखा है ? उत्तर मिलता है कि आकाश ने । तो फिर आकाश को किमने धारण किया है ? वह स्वयं ही प्रतिष्ठित है।" ऐसा उत्तर मिलने पर उन्हें कहना कि 'लोक भी इसी तरह आधार के बिना आकाश में स्थिर है।' इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि यह जगत् किसी ने भी उत्पन्न नहीं किया, स्वयंसिद्ध है। किसी ने धारण नहीं कर रखा है । शंका करते हैं कि 'आधार के बिना लोक रहेगा कहाँ ? उत्तर देते हैं-'आकाश में ।' परन्तु अवस्थित आकाशरूप में ही यह लोक आकाश में प्रतिष्ठित रहता है ।
इस सम्बन्धी आतंरश्लोकों का भावार्थ कहते हैं -शंका करते हैं कि 'लोक-विचारणा को भावना क्यों कही गई ? उत्तर देते हैं कि 'इससे निर्ममत्व परिणाम होते हैं । सुनो ; सुख के कारण किसी भाव में बारवार मन में मूछी पैदा होती है तो इस लोकभावना से उसे अत्यन्त दूर कर सकते हैं। हमने 'ध्यानशतक में कहा है कि 'पृथ्वी, द्वीप, समुद्र आदि धर्मध्यान का विषयभूत है।' इसके बिना साधक लोकभावना का चिन्तन नहीं कर सकता । श्री जिनेश्वर-कथनानुसार लोक-रूप पदार्थों का नि:शंक निश्चय होने के बाद अतीन्द्रिय मोक्षमार्ग में जीवो को श्रद्धा रखनी चाहिए। इति लोकभावना। अब तीन श्लोकों से बोधिदुर्लभभावना कहते हैं
अकामनिर्जरारूपात्, ‘ण्याज्जन्तोः प्रजायते ।
स्थावरत्वात् वसत्वं वा, तिर्यक्त्वं वा कथञ्चन ॥१०७॥ अर्थ-अकामनिर्जरारूपो पुण्य से जीव को स्थावरपर्याय से त्रसपर्याय प्राप्त होता है अथवा वह तिर्यञ्चगति प्राप्त करता है।
व्याख्या-पर्वत के नदी-प्रवाह में बहता हुआ पत्थर ठोकरें खाता-खाता अपनेआप गोलमटोल बन जाता है, उसी प्रकार आये हुए अप्रत्याशित दुःख को विना इच्छा के सहन करने से अकामांनजरा होती है । अर्थात् आत्मा के साथ लगे हुए बहुत-से कर्म नष्ट हो जाते हैं । यह पुण्यप्रकृति का स्वरूप नहीं है, अपितृ आःमा का कर्म के बोझ से हलका होना है। इससे जीव एकेन्द्रियजातीय स्थावर-पर्याय को छोड़ कर वस-पर्याय पा लेता है, या पंचेन्द्रिय-तियंच हो जाता है।
मानुष्यमार्यदेशश्च, जातिः सर्वाक्षपाटवम् ।
आयुश्च प्राप्यते तत्र, कथंचित्कर्मलाघवात् ॥१०॥ अर्थ-उसके बाद अधिक कर्मो से अत्यधिक हलके (लघु) होने पर जीव को मनुष्य-पर्याय, आर्यवेश तथा उत्तम जाति में जन्म, पाँचों इन्द्रियों की परिपूर्णता और वीर्ष मायुष्य को प्राप्ति होती है।