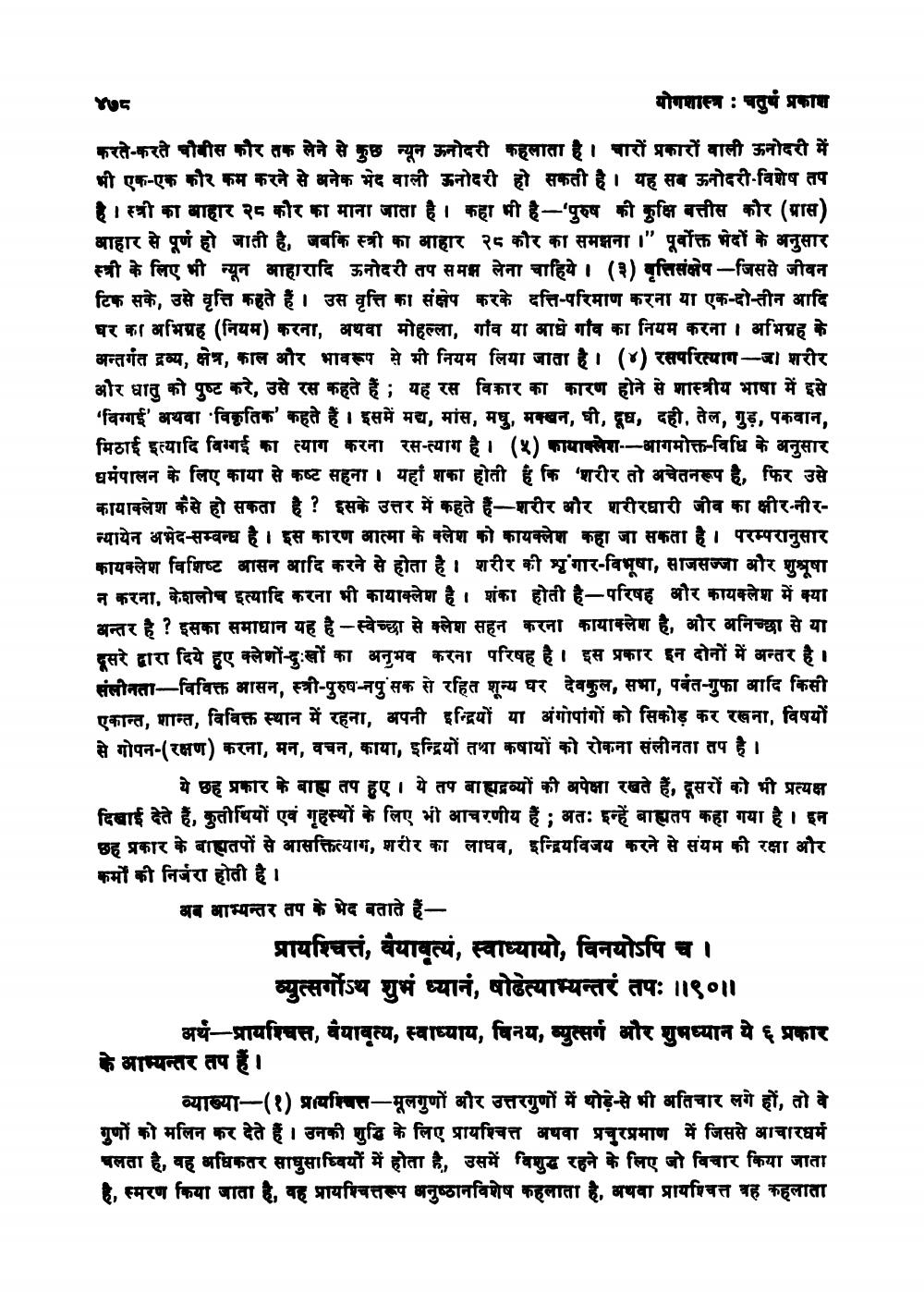________________
४७८
योगशास्त्र : चतुषं प्रकाश करते-करते चौबीस कौर तक लेने से कुछ न्यून ऊनोदरी कहलाता है। चारों प्रकारों वाली ऊनोदरी में भी एक-एक कोर कम करने से अनेक भेद वाली ऊनोदरी हो सकती है। यह सब ऊनोदरी-विशेष तप है। स्त्री का बाहार २८ कौर का माना जाता है। कहा भी है-'पुरुष की कुक्षि बत्तीस कोर (पास) बाहार से पूर्ण हो जाती है, जबकि स्त्री का आहार २८ कौर का समझना ।" पूर्वोक्त भेदों के अनुसार स्त्री के लिए भी न्यून आहारादि ऊनोदरी तप समझ लेना चाहिये । (३) वृत्तिसंक्षेप-जिससे जीवन टिक सके, उसे वृत्ति कहते हैं। उस वृत्ति का संक्षेप करके दत्ति-परिमाण करना या एक-दो-तीन आदि घर का अभिग्रह (नियम) करना, अथवा मोहल्ला, गांव या बाधे गांव का नियम करना । अभिग्रह के अन्तर्गत द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावरूप से भी नियम लिया जाता है। (४) रसपरित्याग-जा शरीर और धातु को पुष्ट करे, उसे रस कहते हैं; यह रस विकार का कारण होने से शास्त्रीय भाषा में इसे 'विग्गई' अथवा 'विकृतिक' कहते हैं । इसमें मद्य, मांस, मधु, मक्खन, घी, दूध, दही, तेल, गुड़, पकवान, मिठाई इत्यादि विग्गई का त्याग करना रस-त्याग है। (५) कायाक्लेश--आगमोक्त-विधि के अनुसार धर्मपालन के लिए काया से कष्ट सहना। यहां शका होती है कि 'शरीर तो अचेतनरूप है, फिर उसे कायाक्लेश कैसे हो सकता है ? इसके उत्तर में कहते हैं-शरीर और शरीरधारी जीव का क्षीर-नीरन्यायेन अभेद-सम्बन्ध है। इस कारण आत्मा के क्लेश को कायक्लेश कहा जा सकता है। परम्परानुसार कायक्लेश विशिष्ट आसन आदि करने से होता है। शरीर की शृंगार-विभूषा, साजसज्जा और शुश्रूषा न करना, केशलोच इत्यादि करना भी कायाक्लेश है। शंका होती है-परिषद और कायक्लेश में क्या अन्तर है ? इसका समाधान यह है -स्वेच्छा से क्लेश सहन करना कायाक्लेश है, और अनिच्छा से या दूसरे द्वारा दिये हुए क्लेशों-दुःखों का अनुभव करना परिषह है। इस प्रकार इन दोनों में अन्तर है। संलीनता-विविक्त मासन, स्त्री-पुरुष नपुंसक से रहित शून्य घर देवकुल, सभा, पर्वत-गुफा आदि किसी एकान्त, शान्त, विविक्त स्थान में रहना, अपनी इन्द्रियों या अंगोपांगों को सिकोड़ कर रखना, विषयों से गोपन-(रक्षण) करना, मन, वचन, काया, इन्द्रियों तथा कषायों को रोकना संलीनता तप है।
ये छह प्रकार के बाह्य तप हुए। ये तप बाह्यद्रव्यों की अपेक्षा रखते हैं, दूसरों को भी प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, कुतीथियों एवं गृहस्थों के लिए भी आचरणीय हैं ; अतः इन्हें बाह्यतप कहा गया है। इन छह प्रकार के बाहतपों से आसक्तित्याग, शरीर का लाघव, इन्द्रियविजय करने से संयम की रक्षा और कर्मों की निर्जरा होती है। अब बाभ्यन्तर तप के भेद बताते हैं
प्रायश्चित्तं, वैयावत्यं, स्वाध्यायो, विनयोऽपि च ।
व्युत्सर्गोऽथ शुभं ध्यानं, षोढत्याभ्यन्तरं तपः ॥१०॥ अर्थ-प्रायश्चित्त, वैयावृत्य, स्वाध्याय, विनय, व्युत्सर्ग और शुभध्यान ये ६ प्रकार के आभ्यन्तर तप हैं।
व्याख्या-(१) प्रायश्चित्त-मूलगुणों और उत्तरगुणों में थोड़े-से भी अतिचार लगे हों, तो वे गुणों को मलिन कर देते हैं । उनकी शुद्धि के लिए प्रायश्चित्त अथवा प्रचुरप्रमाण में जिससे आचारधर्म चलता है, वह अधिकतर साधुसाध्वियों में होता है, उसमें विशुद्ध रहने के लिए जो विचार किया जाता है, स्मरण किया जाता है, वह प्रायश्चित्तरूप अनुष्ठानविशेष कहलाता है, अथवा प्रायश्चित्त वह कहलाता