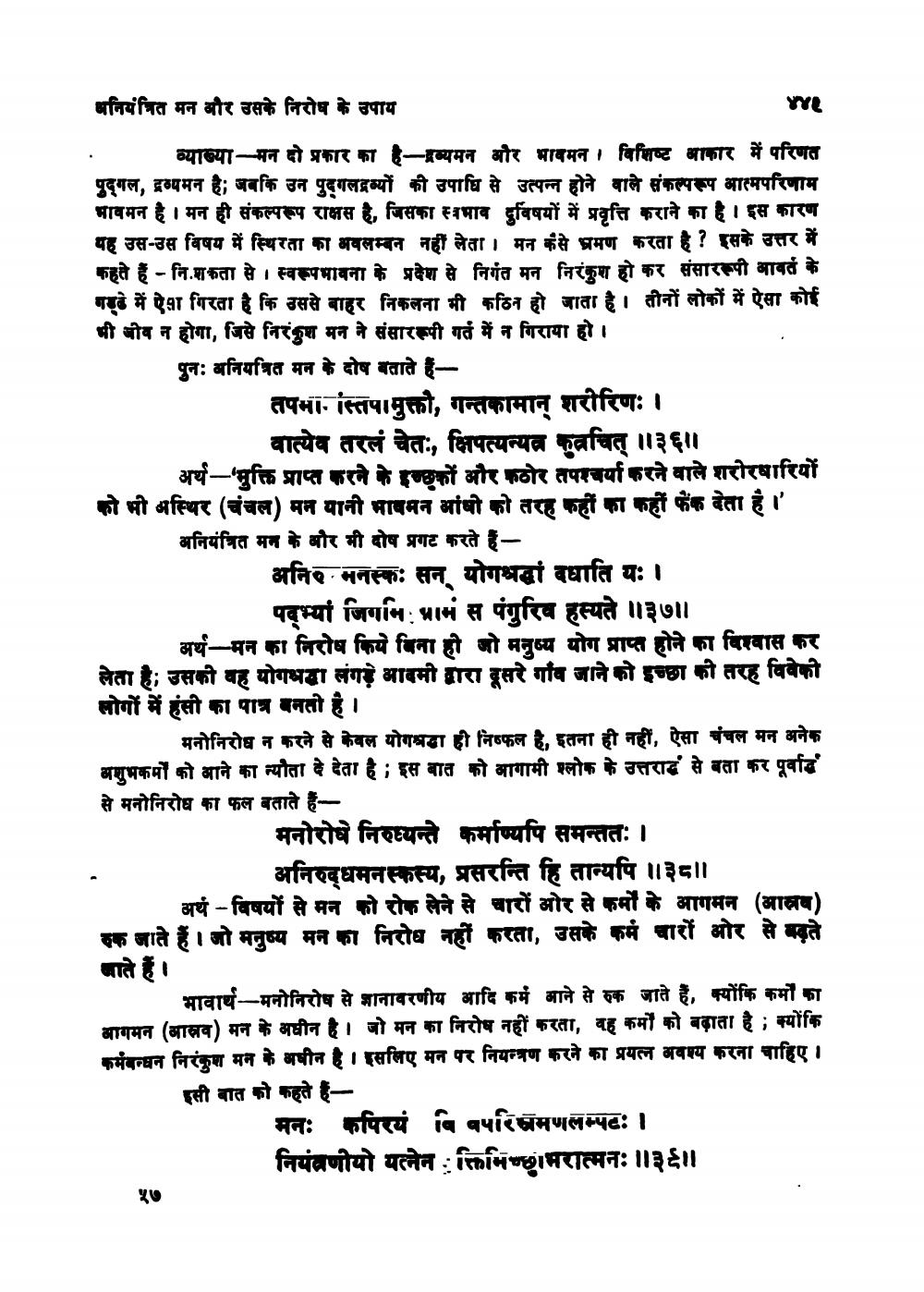________________
बनियंत्रित मन और उसके निरोष के उपाय
me
व्याख्या-मन दो प्रकार का है-द्रव्यमन और भावमन । विशिष्ट आकार में परिणत पुद्गल, द्रव्यमन है। जबकि उन पुद्गलद्रव्यों की उपाधि से उत्पन्न होने वाले संकल्परूप आत्मपरिणाम भावमन है । मन ही संकल्परूप राक्षस है, जिसका स्वभाव दुविषयों में प्रवृत्ति कराने का है । इस कारण यह उस-उस विषय में स्थिरता का अवलम्बन नहीं लेता। मन कैसे भ्रमण करता है ? इसके उत्तर में कहते हैं - नि.शकता से । स्वरूपभावना के प्रदेश से निर्गत मन निरंकुश हो कर संसाररूपी आवर्त के गळे में ऐसा गिरता है कि उससे बाहर निकलना भी कठिन हो जाता है। तीनों लोकों में ऐसा कोई भी जीव न होगा, जिसे निरंकुश मन ने संसाररूपी गर्त में न गिराया हो। पुनः बनियत्रित मन के दोष बताते हैं
तपमा स्तिपामुक्ती, गन्तकामान् शरीरिणः ।
वात्येव तरलं चेतः, क्षिपत्यन्यन कुवचित् ॥३६॥ अर्थ-मुक्ति प्राप्त करने के इच्छकों और कठोर तपश्चर्या करने वाले शरीरबारियों को भी अस्थिर (चंचल) मन यानी भाषमन आंघो को तरह कहीं का कहीं फेंक देता है।' अनियंत्रित मन के बौर भी दोष प्रगट करते हैं
अनि मनस्कः सन योगश्रद्धा वधाति यः।
पद्भ्यां जिगनि: आम स पंगुरिव हस्यते ॥३७॥ अर्थ-मन का निरोष किये बिना ही जो मनुष्य योग प्राप्त होने का विश्वास कर लेता है। उसकी वह योगमाया लंगड़े मादमी द्वारा दूसरे गांव जाने को इच्छा की तरह विवेकी लोगों में हंसी का पात्र बनती है।
____ मनोनिरोध न करने से केवल योगश्रद्धा ही निष्फल है, इतना ही नहीं, ऐसा चंचल मन अनेक अशुभकर्मों को आने का न्योता दे देता है। इस बात को आगामी श्लोक के उत्तराद से बता कर पूर्वाद्ध से मनोनिरोध का फल बताते हैं
मनोरोघे निरुध्यन्ते कर्माण्यपि समन्ततः ।
अनिरुद्धमनस्कस्य, प्रसरन्ति हि तान्यपि ॥३८॥ अर्थ-विषयों से मन को रोक लेने से चारों ओर से कर्मों के आगमन (मानव) रुक जाते हैं । जो मनुष्य मन का निरोध नहीं करता, उसके कर्म चारों ओर से बढ़ते जाते हैं।
भावार्थ-मनोनिरोध से ज्ञानावरणीय आदि कर्म आने से रुक जाते हैं, क्योंकि कर्मों का आगमन (मानव) मन के अधीन है। जो मन का निरोष नहीं करता, वह कर्मों को बढ़ाता है ; क्योंकि कर्मबन्धन निरंकुश मन के अधीन है । इसलिए मन पर नियन्त्रण करने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए । इसी बात को कहते हैं
मनः कपिरयं विपरित्रमणलम्पटः। नियंवणीयो यत्लेन ::क्तिमिछाभरात्मनः॥३६॥