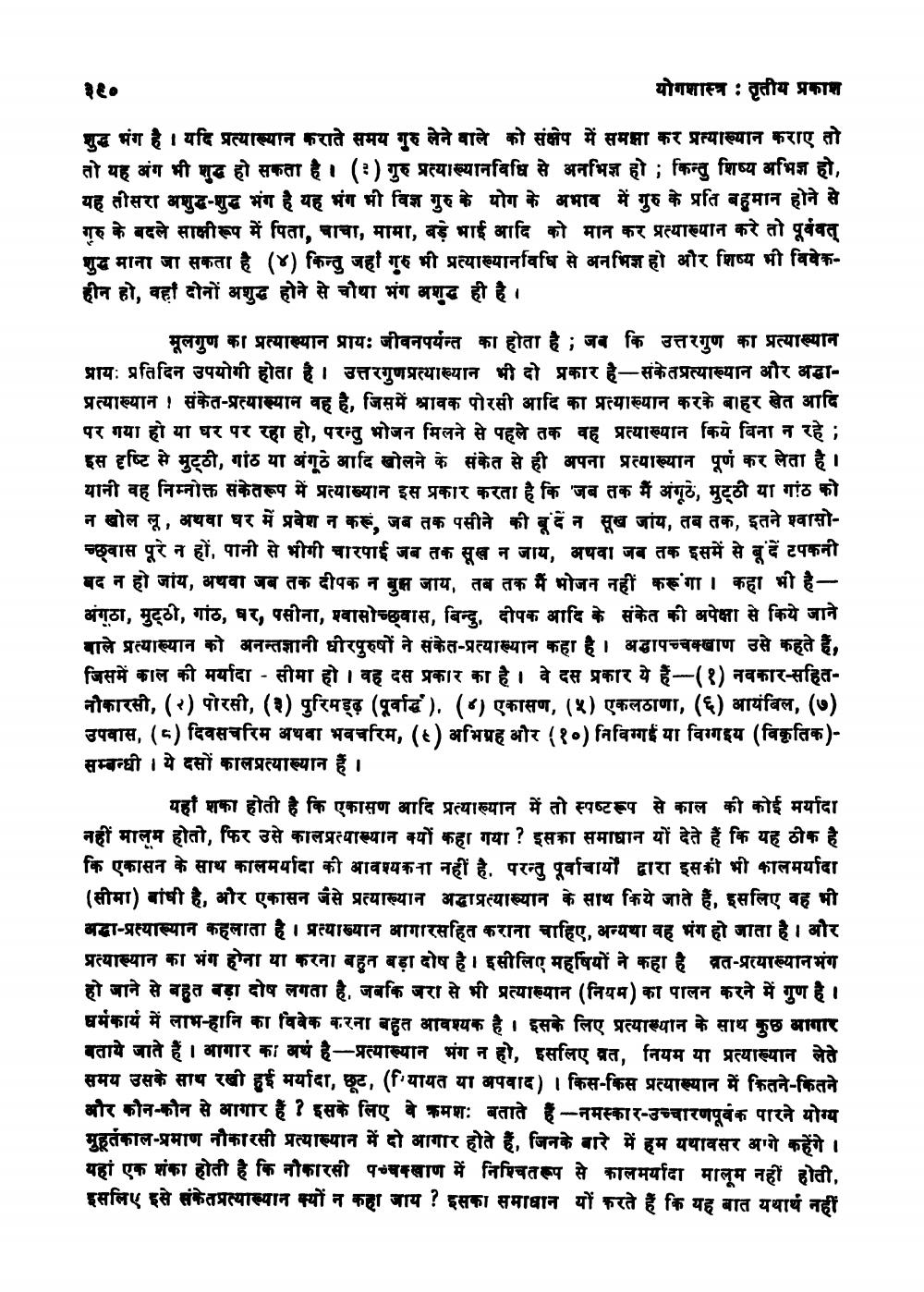________________
३६.
योगशास्त्र : तृतीय प्रकाश शुद्ध भंग है । यदि प्रत्याख्यान कराते समय गुरु लेने वाले को संक्षेप में समझा कर प्रत्याख्यान कराए तो तो यह अंग भी शुद्ध हो सकता है। (३) गुरु प्रत्याख्यानविधि से अनभिज्ञ हो; किन्तु शिष्य अभिज्ञ हो, यह तीसरा अशुद्ध-शुद्ध भंग है यह भंग भी विज्ञ गुरु के योग के अभाव में गुरु के प्रति बहुमान होने से गुरु के बदले साक्षीरूप में पिता, चाचा, मामा, बड़े भाई आदि को मान कर प्रत्याख्यान करे तो पूर्ववत् शुद्ध माना जा सकता है (४) किन्तु जहाँ गुरु भी प्रत्याख्यानविधि से अनभिज्ञ हो और शिष्य भी विवेकहीन हो, वहाँ दोनों अशुद्ध होने से चौथा भंग अशुद्ध ही है।
मूलगुण का प्रत्याख्यान प्रायः जीवनपर्यन्त का होता है ; जब कि उत्तरगुण का प्रत्याख्यान प्रायः प्रतिदिन उपयोगी होता है। उत्तरगुणप्रत्याख्यान भी दो प्रकार है-संकेतप्रत्याख्यान और अद्धाप्रत्याख्यान । संकेत-प्रत्याख्यान वह है, जिसमें श्रावक पोरसी आदि का प्रत्याख्यान करके बाहर खेत आदि पर गया हो या घर पर रहा हो, परन्तु भोजन मिलने से पहले तक वह प्रत्याख्यान किये बिना न रहे ; इस दृष्टि से मुट्ठी, गांठ या अंगूठे आदि खोलने के संकेत से ही अपना प्रत्याख्यान पूर्ण कर लेता है। यानी वह निम्नोक्त संकेतरूप में प्रत्याख्यान इस प्रकार करता है कि 'जब तक मैं अंगूठे, मुट्ठी या गांठ को न खोल लू , अथवा घर में प्रवेश न करूं, जब तक पसीने की बूंदें न सूख जांय, तब तक, इतने श्वासोच्छ्वास पूरे न हों, पानी से भीगी चारपाई जब तक सूख न जाय, अथवा जब तक इसमें से बूंदें टपकनी बद न हो जाय, अथवा जब तक दीपक न बुझ जाय, तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। कहा भी हैअंगठा, मुट्ठी, गांठ, घर, पसीना, श्वासोच्छ्वास, बिन्दु, दीपक आदि के संकेत की अपेक्षा से किये जाने बाले प्रत्याख्यान को अनन्तज्ञानी धीरपुरुषों ने संकेत-प्रत्याख्यान कहा है। अद्धापच्चक्खाण उसे कहते हैं, जिसमें काल की मर्यादा - सीमा हो । वह दस प्रकार का है। वे दस प्रकार ये हैं--(१) नवकार-सहितनौकारसी, (२) पोरसी, (३) पुरिमड्ढ़ (पूर्वार्द्ध), (४) एकासण, (५) एकलठाणा, (६) आयंबिल, (७) उपवास, (6) दिवसचरिम अथवा भवचरिम, (6) अभिग्रह और (१०) निविग्गई या विग्गइय (विकृतिक)सम्बन्धी । ये दसों कालप्रत्याख्यान हैं ।
यहाँ शका होती है कि एकासण आदि प्रत्याख्यान में तो स्पष्ट रूप से काल की कोई मर्यादा नहीं मालूम होतो, फिर उसे कालप्रत्याख्यान क्यों कहा गया? इसका समाधान यों देते हैं कि यह ठीक है कि एकासन के साथ कालमर्यादा की आवश्यकता नहीं है, परन्तु पूर्वाचार्यों द्वारा इसकी भी कालमर्यादा (सीमा) बांधी है, और एकासन जैसे प्रत्याख्यान अद्धाप्रत्याख्यान के साथ किये जाते हैं, इसलिए वह भी बदा-प्रत्याख्यान कहलाता है । प्रत्याख्यान आगारसहित कराना चाहिए, अन्यथा वह भंग हो जाता है। और प्रत्याख्यान का भंग होना या करना बहुत बड़ा दोष है। इसीलिए महर्षियों ने कहा है व्रत-प्रत्याख्यानभंग हो जाने से बहुत बड़ा दोष लगता है, जबकि जरा से भी प्रत्याख्यान (नियम) का पालन करने में गुण है। धर्मकार्य में लाभ-हानि का विवेक करना बहुत आवश्यक है । इसके लिए प्रत्याख्यान के साथ कुछ भागार बताये जाते हैं। बागार का अर्थ है-प्रत्याख्यान भंग न हो, इसलिए व्रत, नियम या प्रत्याख्यान लेते समय उसके साथ रखी हुई मर्यादा, छूट, (यिायत या अपवाद) । किस-किस प्रत्याख्यान में कितने-कितने और कौन-कौन से आगार हैं ? इसके लिए वे क्रमशः बताते हैं -नमस्कार-उच्चारणपूर्वक पारने योग्य मुहर्तकाल-प्रमाण नौकारसी प्रत्याख्यान में दो आगार होते हैं, जिनके बारे में हम यथावसर अग्गे कहेंगे । यहां एक शंका होती है कि नौकारसी पच्चक्खाण में निश्चितरूप से कालमर्यादा मालूम नहीं होती, इसलिए इसे संकेतप्रत्याख्यान क्यों न कहा जाय ? इसका समाधान यों करते हैं कि यह बात यथार्थ नहीं