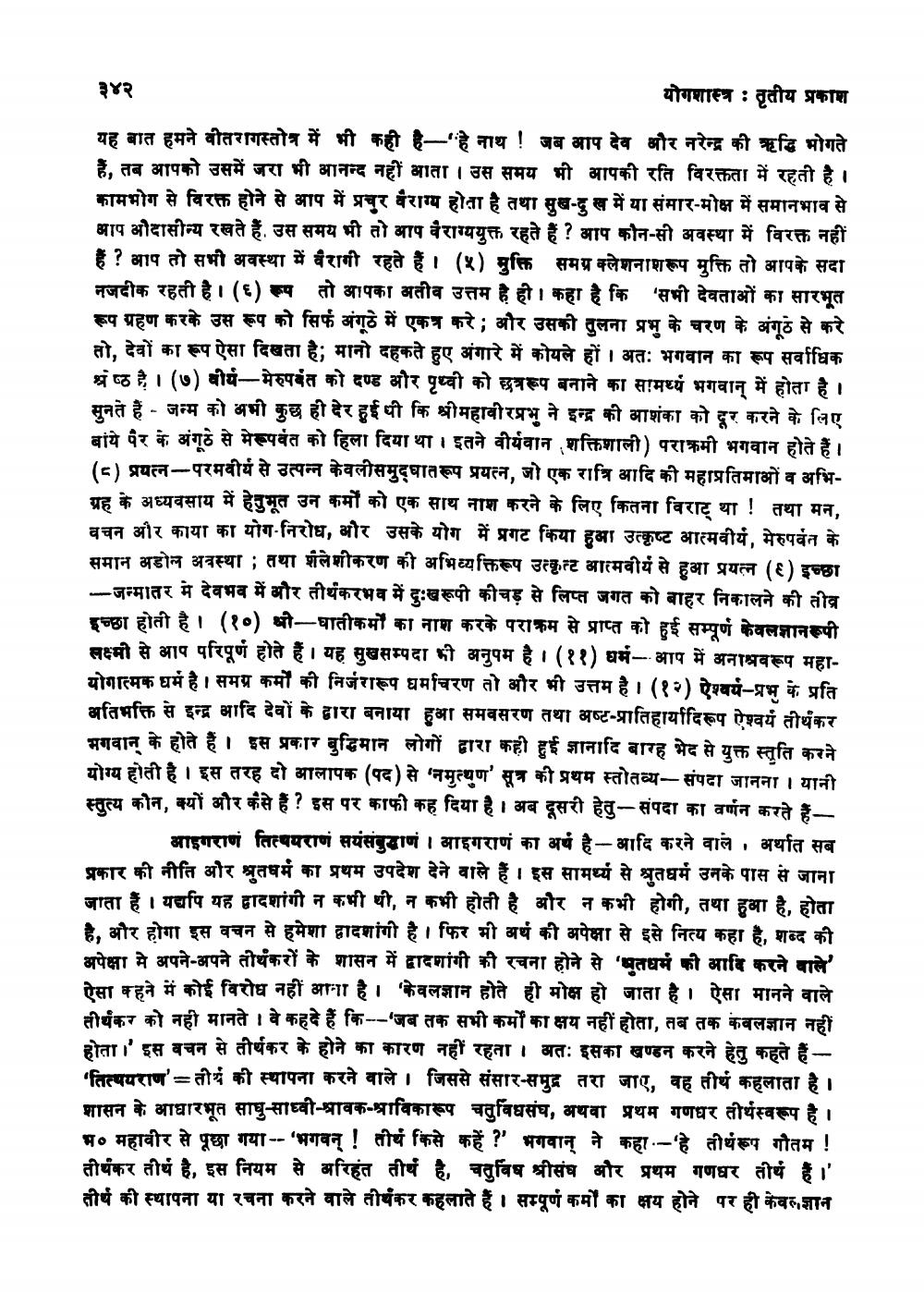________________
३४२
योगशास्त्र : तृतीय प्रकाश
यह बात हमने वीतरागस्तोत्र में भी कही है- हे नाथ ! जब आप देव और नरेन्द्र की ऋद्धि भोगते हैं, तब आपको उसमें जरा भी आनन्द नहीं आता । उस समय भी आपकी रति विरक्तता में रहती है । कामभोग से विरक्त होने से आप में प्रचुर वैराग्य होता है तथा सुख-दुख में या संमार-मोक्ष में समानभाव से आप औदासीन्य रखते हैं, उस समय भी तो आप वैराग्ययुक्त रहते हैं ? आप कौन-सी अवस्था में विरक्त नहीं हैं ? आप तो सभी अवस्था में वैरागी रहते हैं । (५) मुक्ति समग्र क्लेशनाशरूप मुक्ति तो आपके सदा नजदीक रहती है । (६) रूप तो आपका अतीव उत्तम है ही। कहा है कि 'सभी देवताओं का सारभूत रूप ग्रहण करके उस रूप को सिर्फ अंगूठे में एकत्र करे; और उसकी तुलना प्रभु के चरण के अंगूठे से करे तो, देवों का रूप ऐसा दिखता है; मानो दहकते हुए अंगारे में कोयले हों । अतः भगवान का रूप सर्वाधिक श्रं ष्ठ है । (७) वीर्य - मेरुपर्वत को दण्ड और पृथ्वी को छत्ररूप बनाने का सामथ्यं भगवान् में होता है । सुनते हैं - जन्म को अभी कुछ ही देर हुई थी कि श्रीमहावीरप्रभु ने इन्द्र की आशंका को दूर करने के लिए बांये पैर के अंगूठे से मेरूपवंत को हिला दिया था। इतने वीर्यवान शक्तिशाली) पराक्रमी भगवान होते हैं। (८) प्रयत्न - परमवीर्य से उत्पन्न केवलीसमुद्घातरूप प्रयत्न, जो एक रात्रि आदि की महाप्रतिमाओं व अभिग्रह के अध्यवसाय में हेतुभूत उन कर्मों को एक साथ नाश करने के लिए कितना विराट् था ! तथा मन, वचन और काया का योग निरोध, और उसके योग में प्रगट किया हुआ उत्कृष्ट आत्मवीर्यं, मेरुपर्वत के समान अडोल अवस्था ; तथा शंलेशीकरण की अभिव्यक्तिरूप उत्कृष्ट आत्मवीर्यं से हुआ प्रयत्न ( ६ ) इच्छा - जन्मातर मे देवभव में और तीर्थंकरभव में दुःखरूपी कीचड़ से लिप्त जगत को बाहर निकालने की तीव्र इच्छा होती है । (१०) श्री- घातीकर्मों का नाश करके पराक्रम से प्राप्त को हुई सम्पूर्ण केवलज्ञानरूपी लक्ष्मी से आप परिपूर्ण होते हैं। यह सुखसम्पदा की अनुपम है । (११) धर्म- आप में अनाश्रवरूप महायोगात्मक धर्म है । समग्र कर्मों की निर्जरारूप धर्माचरण तो और भी उत्तम है । ( १२ ) ऐश्वर्य - प्रभु के प्रति अतिभक्ति से इन्द्र आदि देवों के द्वारा बनाया हुआ समवसरण तथा अष्ट-प्रातिहार्यादिरूप ऐश्वर्यं तीर्थंकर भगवान् के होते हैं । इस प्रकार बुद्धिमान लोगों द्वारा कही हुई ज्ञानादि बारह भेद से युक्त स्तुति करने योग्य होती है । इस तरह दो आलापक (पद) से 'नमुत्थुण' सूत्र की प्रथम स्तोतव्य- संपदा जानना । यानी स्तुत्य कौन, क्यों और कैसे हैं ? इस पर काफी कह दिया है। अब दूसरी हेतु - संपदा का वर्णन करते हैंअर्थात सब प्रकार की नीति और श्रुतधर्म का प्रथम उपदेश देने वाले हैं। इस सामथ्यं से श्रुतधर्म उनके पास से जाना जाता हैं । यद्यपि यह द्वादशांगी न कभी थी, न कभी होती है और न कभी होगी, तथा हुआ है, होता है, और होगा इस वचन से हमेशा द्वादशांगी है। फिर भी अर्थ की अपेक्षा से इसे नित्य कहा है, शब्द की अपेक्षा मे अपने-अपने तीर्थंकरों के शासन में द्वादशांगी की रचना होने से 'भुतधर्म की आदि करने वाले ऐसा कहने में कोई विरोध नहीं आना है। 'केवलज्ञान होते ही मोक्ष हो जाता है। ऐसा मानने वाले तीर्थंकर को नही मानते। वे कहदे हैं कि-'जब तक सभी कर्मों का क्षय नहीं होता, तब तक कंवलज्ञान नहीं होता।' इस वचन से तीर्थकर के होने का कारण नहीं रहता । अतः इसका खण्डन करने हेतु कहते हैं - 'तित्थयराण' = तीर्थ की स्थापना करने वाले । जिससे संसार-समुद्र तरा जाए, वह तीर्थ कहलाता है । शासन के आधारभूत साधु-साध्वी श्रावक-श्राविकारूप चतुविधसंघ, अथवा प्रथम गणधर तीर्थस्वरूप है । कहा - 'हे तीर्थरूप गौतम ! प्रथम गणधर तीर्थं हैं ।' क्षय होने पर ही केवलज्ञान
आइगराणं तित्थयराणं सयंसंबुद्धाणं । आइगराणं का अर्थ है - आदि करने वाले
·
भ० महावीर से पूछा गया- 'भगवन् ! तीर्थं किसे कहें ?" भगवान् ने तीर्थंकर तीर्थ है, इस नियम से अरिहंत तीर्थं है, चतुविध श्रीसंघ और तीर्थ की स्थापना या रचना करने वाले तीर्थंकर कहलाते हैं । सम्पूर्ण कर्मों का