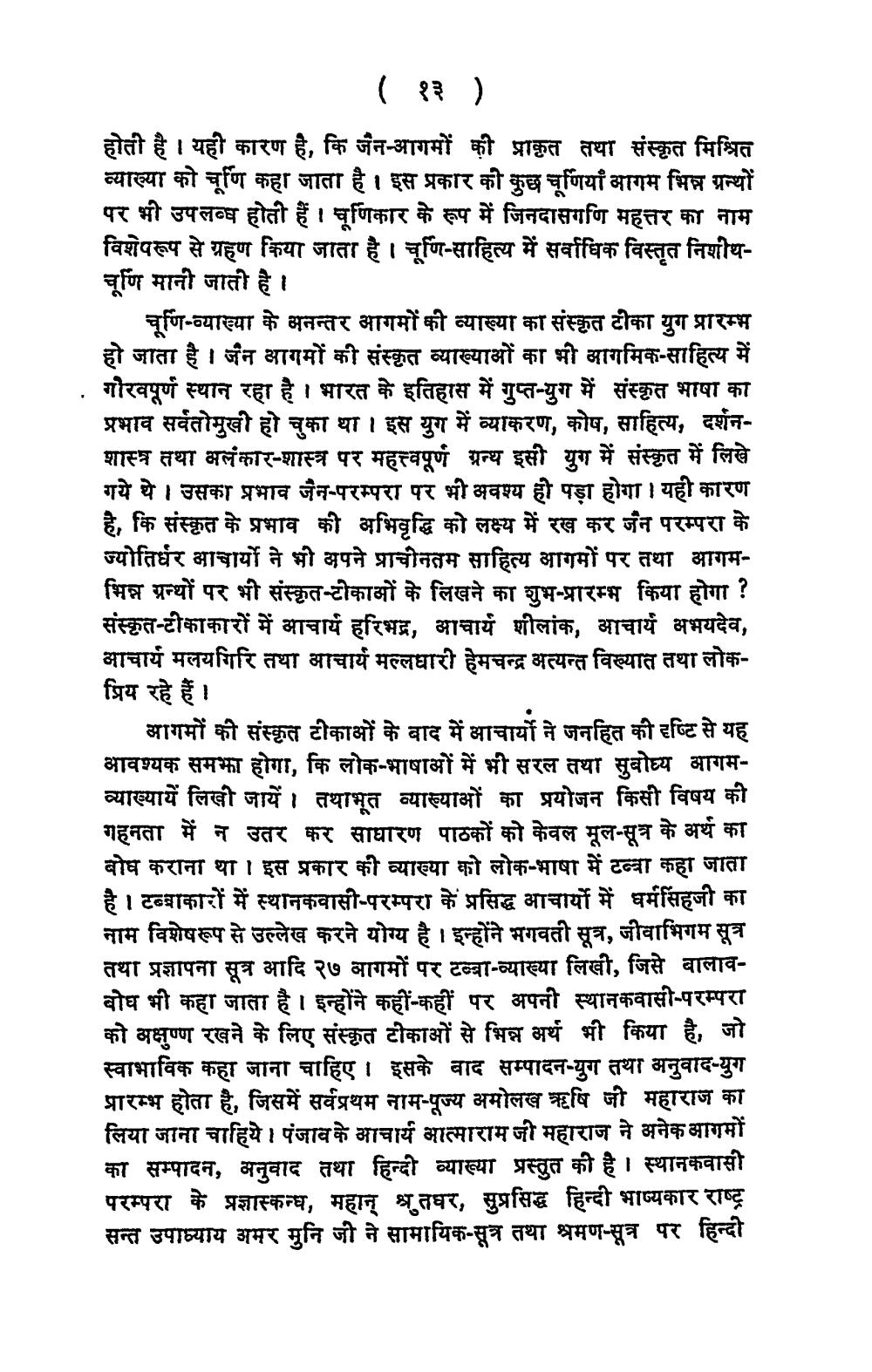________________
( १३ ) होती है । यही कारण है, कि जैन-आगमों की प्राकृत तथा संस्कृत मिश्रित व्याख्या को चूणि कहा जाता है । इस प्रकार को कुछ चूर्णियां आगम भिन्न ग्रन्थों पर भी उपलब्ध होती हैं। चूर्णिकार के रूप में जिनदासगणि महत्तर का नाम विशेषरूप से ग्रहण किया जाता है । चूणि-साहित्य में सर्वाधिक विस्तृत निशीथचूणि मानी जाती है।
चूर्णि-व्याख्या के अनन्तर आगमों की व्याख्या का संस्कृत टीका युग प्रारम्भ हो जाता है । जैन आगमों की संस्कृत व्याख्याओं का भी आगमिक-साहित्य में गौरवपूर्ण स्थान रहा है। भारत के इतिहास में गुप्त-युग में संस्कृत भाषा का प्रभाव सर्वतोमुखी हो चुका था। इस युग में व्याकरण, कोष, साहित्य, दर्शनशास्त्र तथा अलंकार-शास्त्र पर महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ इसी युग में संस्कृत में लिखे गये थे। उसका प्रभाव जैन-परम्परा पर भी अवश्य ही पड़ा होगा। यही कारण है, कि संस्कृत के प्रभाव की अभिवृद्धि को लक्ष्य में रख कर जैन परम्परा के ज्योतिर्धर आचार्यों ने भी अपने प्राचीनतम साहित्य आगमों पर तथा आगमभिन्न ग्रन्थों पर भी संस्कृत-टोकाओं के लिखने का शुभ-प्रारम्भ किया होगा? संस्कृत-टीकाकारों में आचार्य हरिभद्र, आचार्य शीलांक, आचार्य अभयदेव, आचार्य मलयगिरि तथा आचार्य मल्लधारी हेमचन्द्र अत्यन्त विख्यात तथा लोकप्रिय रहे हैं।
आगमों की संस्कृत टीकाओं के बाद में आचार्यों ने जनहित की दृष्टि से यह आवश्यक समझा होगा, कि लोक-भाषाओं में भी सरल तथा सुबोध्य आगमव्याख्यायें लिखी जायें। तथाभूत व्याख्याभों का प्रयोजन किसी विषय की गहनता में न उतर कर साधारण पाठकों को केवल मूल-सूत्र के अर्थ का बोध कराना था। इस प्रकार की व्याख्या को लोक-भाषा में टब्बा कहा जाता है। टब्बाकारों में स्थानकवासी-परम्परा के प्रसिद्ध आचार्यों में धर्मसिंहजी का नाम विशेषरूप से उल्लेख करने योग्य है । इन्होंने भगवती सूत्र, जीवाभिगम सूत्र तथा प्रज्ञापना सूत्र आदि २७ नागमों पर टब्बा-व्याख्या लिखी, जिसे बालावबोध भी कहा जाता है। इन्होंने कहीं-कहीं पर अपनी स्थानकवासी-परम्परा को अक्षुण्ण रखने के लिए संस्कृत टीकाओं से भिन्न अर्थ भी किया है, जो स्वाभाविक कहा जाना चाहिए। इसके बाद सम्पादन-युग तथा अनुवाद-युग प्रारम्भ होता है, जिसमें सर्वप्रथम नाम-पूज्य अमोलख ऋषि जी महाराज का लिया जाना चाहिये। पंजाव के आचार्य मात्माराम जी महाराज ने अनेक आगमों का सम्पादन, अनुवाद तथा हिन्दी व्याख्या प्रस्तुत की है । स्थानकवासी परम्परा के प्रज्ञास्कन्ध, महान् श्रुतघर, सुप्रसिद्ध हिन्दी भाज्यकार राष्ट्र सन्त उपाध्याय अमर मुनि जी ने सामायिक-सूत्र तथा श्रमण-सूत्र पर हिन्दी