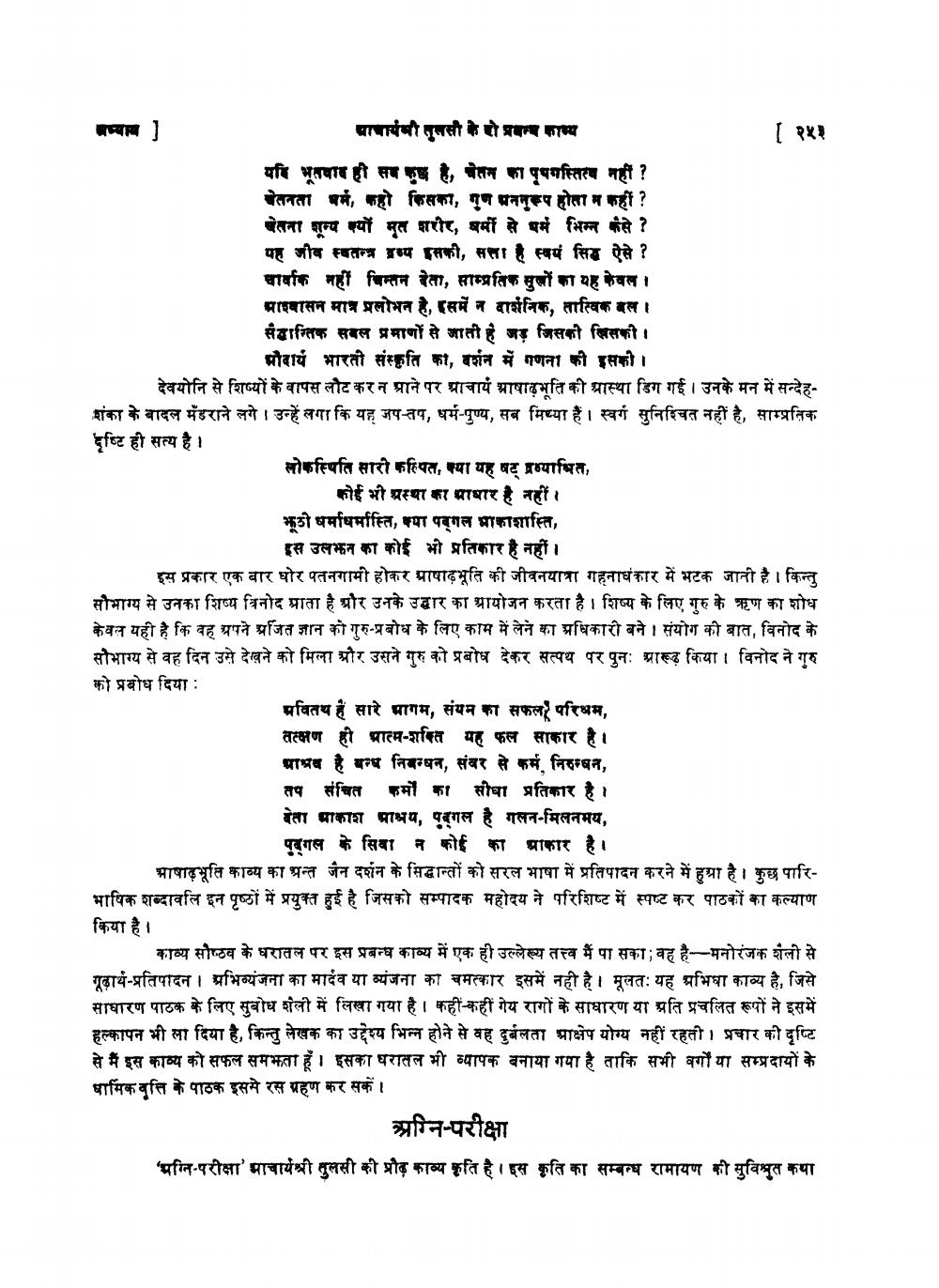________________
प्राचार्यवी तुलसी के दो प्रबन्ध काव्य
[ २५३
यदि भूतवाद ही सबकुछतनका पुषगस्तित्व नहीं? बेतनता धर्म, कहो किसका, गुण मनमुरूप होतामकहीं? चेतना मान्य क्यों मृत शरीर, धर्मी से धर्म भिन्न कैसे ? पह जीव स्वतन्त्र द्रव्य इसकी, सत्ता है स्वयं सिद्ध ऐसे ? चार्वाक नहीं चिन्तन देता, साम्प्रतिक सुखों का यह केवल । माश्वासन मात्र प्रलोभन है, इसमें न दार्शनिक, तात्विक बल । सैदान्तिक सबल प्रमाणों से जाती है जड़ जिसको खिसकी।
प्रौवार्य भारती संस्कृति का, वर्शन में गणना की इसकी। देवयोनि से शिष्यों के वापस लौट कर न पाने पर प्राचार्य आषाढभूति की प्रास्था डिग गई । उनके मन में सन्देहशंका के बादल मंडराने लगे। उन्हें लगा कि यह जप-तप, धर्म-पुण्य, सब मिथ्या हैं। स्वर्ग सुनिश्चित नहीं है, साम्प्रतिक दृष्टि ही सत्य है।
लोकस्थिति सारी करिपत, क्या यह षट् प्रध्याधित,
कोई भी प्रस्था कर माधार है नहीं। झूठी धर्माधर्मास्ति, क्या पद्गल माकाशास्ति,
इस उलझन का कोई भी प्रतिकार है नहीं। इस प्रकार एक बार घोर पतनगामी होकर प्राषाढ़भूति की जीवनयात्रा गहनाधकार में भटक जाती है। किन्तु सौभाग्य से उनका शिष्य विनोद पाता है और उनके उद्धार का आयोजन करता है। शिष्य के लिए गुरु के ऋण का शोध केवल यही है कि वह अपने अजित ज्ञान को गुरु-प्रबोध के लिए काम में लेने का अधिकारी बने। संयोग की बात, विनोद के सौभाग्य से वह दिन उसे देखने को मिला और उसने गुरु को प्रबोध देकर सत्पथ पर पुनः प्रारूढ़ किया। विनोद ने गुरु को प्रबोध दिया:
पवितय है सारे मागम, संयम का सफल परिश्रम, तत्क्षण ही प्रात्म-शक्ति यह फल साकार है। पाश्रय है बन्ध निबन्धन, संवर से कर्म, निहन्धन, तप संचित कर्मों का सीधा प्रतिकार है। बेता माकाश माश्रय, पुद्गल है गलन-मिलनमय,
पुदगल के सिवा न कोई का प्राकार है। भाषाढ़भूति काव्य का अन्त जैन दर्शन के सिद्धान्तों को सरल भाषा में प्रतिपादन करने में हुअा है। कुछ पारिभाषिक शब्दावलि इन पृष्ठों में प्रयुक्त हुई है जिसको सम्पादक महोदय ने परिशिष्ट में स्पष्ट कर पाठकों का कल्याण किया है।
काव्य सौष्ठव के धरातल पर इस प्रबन्ध काव्य में एक ही उल्लेख्य तत्त्व मैं पा सका; वह है-मनोरंजक शैली से गूढार्थ-प्रतिपादन । अभिव्यंजना का मार्दव या व्यंजना का चमत्कार इसमें नहीं है। मूलतः यह अभिधा काव्य है, जिसे साधारण पाठक के लिए सुबोध शैली में लिखा गया है। कहीं-कहीं गेय रागों के साधारण या प्रति प्रचलित रूपों ने इसमें हल्कापन भी ला दिया है, किन्तु लेखक का उद्देश्य भिन्न होने से वह दुर्बलता आक्षेप योग्य नहीं रहती। प्रचार की दृष्टि से मैं इस काव्य को सफल समझता हूँ। इसका धरातल भी व्यापक बनाया गया है ताकि सभी वर्गों या सम्प्रदायों के धार्मिक वृत्ति के पाठक इससे रस ग्रहण कर सकें।
अग्नि-परीक्षा 'मग्नि-परीक्षा'माचार्यश्री तुलसी की प्रौढ़ काव्य कृति है। इस कृति का सम्बन्ध रामायण की सुविश्रुत कया