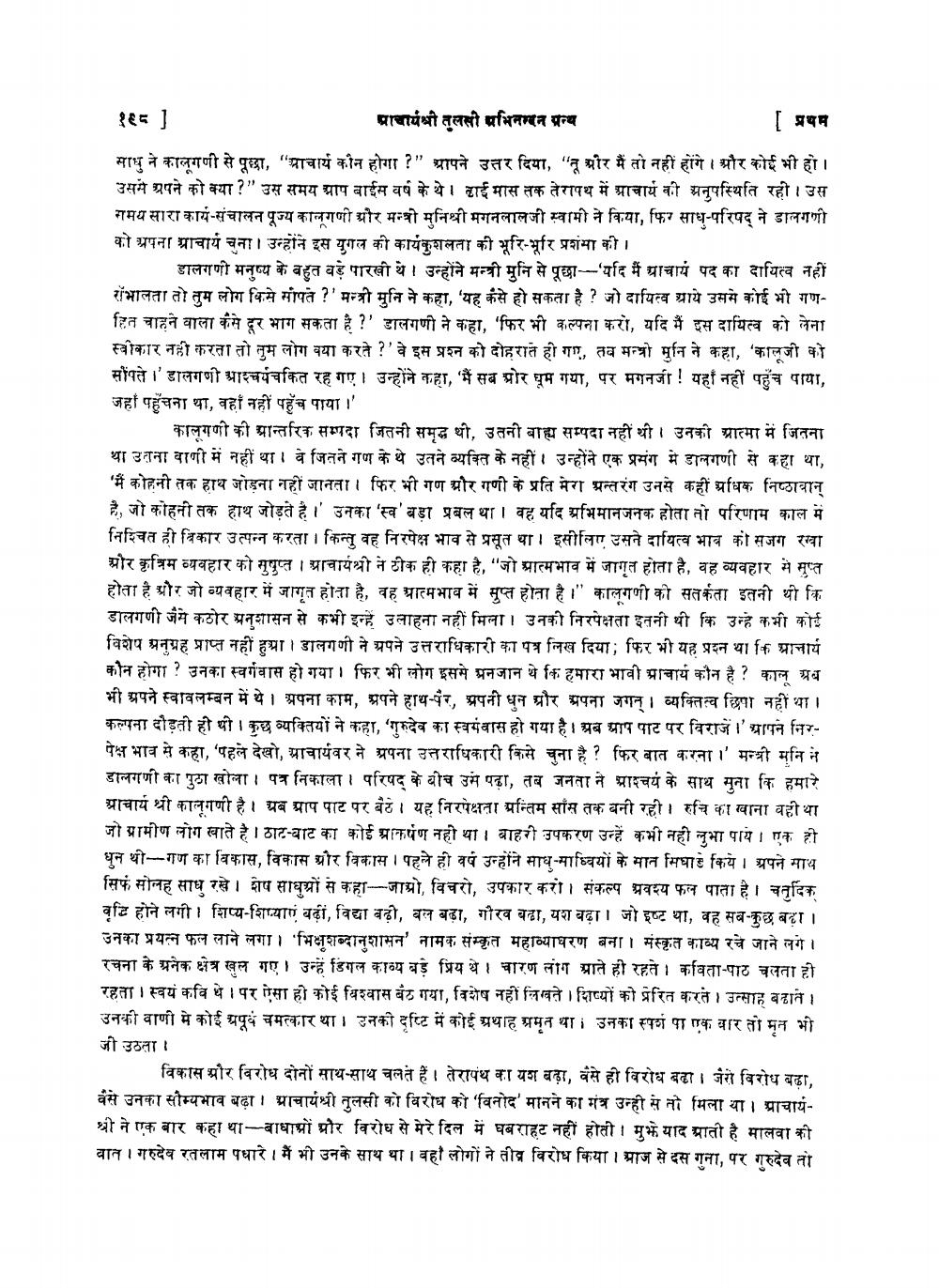________________
१९८ ] प्राचार्यश्री तुलसी अभिनम्वन ग्रन्थ
[ प्रथम माधु ने कालूगणी से पूछा, "माचार्य कौन होगा ?" अापने उत्तर दिया, "तू और मैं तो नहीं होंगे । और कोई भी हो । उसमे अपने को क्या?" उस समय आप बाईस वर्ष के थे। हाई मास तक तेरापथ में प्राचार्य की अनुपस्थिति रही। उस गमय सारा कार्य-संचालन पूज्य कालगणी और मन्त्री मुनिथी मगनलालजी स्वामी ने किया, फिर साधु-परिषद् ने डालगणी को अपना प्राचार्य चना। उन्होंने इस युगल की कार्यकुशलता की भूरि-भूरि प्रशंमा की।
डालगणी मनुष्य के बहुत बड़े पारखी थे। उन्होंने मन्त्री मुनि से पूछा--'यदि मैं ग्राचार्य पद का दायित्व नहीं रॉभालता तो तुम लोग बिसे सांपते?' मन्त्री मुनि ने कहा, 'यह कैसे हो सकता है ? जो दायित्व पाये उसमे कोई भी गणहित चाहने वाला कैसे दूर भाग सकता है ?' डालगणी ने कहा, "फिर भी कल्पना करो, यदि मैं इस दायित्व को लेना स्वीकार नहीं करता तो तुम लोग क्या करते ?' वे इस प्रश्न को दोहराते ही गए, तब मन्त्रो मुनि ने कहा, 'कालूजी को सौंपते।' डालगणी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा, 'मैं सब पोर घूम गया, पर मगनजी! यहाँ नहीं पहुंच पाया, जहाँ पहुँचना था, वहाँ नहीं पहुंच पाया।'
कालगणी की प्रान्तरिक सम्पदा जितनी समृद्ध थी, उतनी बाह्य सम्पदा नहीं थी। उनकी आत्मा में जितना था उतना वाणी में नहीं था। वे जितने गण के थे उतने व्यक्ति के नहीं। उन्होंने एक प्रसंग मे डालगणी से कहा था, 'मैं कोहनी तक हाथ जोड़ना नहीं जानता। फिर भी गण और गणी के प्रति मेग अन्तरंग उनसे कहीं अधिक निष्ठावान् है, जो कोहनी तक हाथ जोड़ते है।' उनका 'स्व' बड़ा प्रबल था। वह यदि अभिमानजनक होता तो परिणाम काल में निश्चित ही विकार उत्पन्न करता। किन्तु वह निरपेक्ष भाव से प्रसूत था। इसीलिए उसने दायित्व भाव को सजग रखा
और कृत्रिम व्यवहार को सुषुप्त । प्राचार्यश्री ने ठीक ही कहा है, "जो प्रात्मभाव में जागृत होता है, वह व्यवहार में सुप्त होता है और जो व्यवहार में जागृत होता है, वह अात्मभाव में सुप्त होता है।" कालगणी की सतर्कता इतनी थी कि डालगणी जैसे कठोर अनुशासन से कभी इन्हें उलाहना नहीं मिला। उनकी निरपेक्षता इतनी थी कि उन्हें कभी कोई विशेष अनुग्रह प्राप्त नहीं हया । डालगणी ने अपने उत्तराधिकारी का पत्र लिख दिया; फिर भी यह प्रश्न था कि प्राचार्य कौन होगा? उनका स्वर्गवास हो गया। फिर भी लोग इसमे अनजान थे कि हमारा भावी प्राचार्य कौन है ? काल अब भी अपने स्वावलम्बन में थे। अपना काम, अपने हाथ-पैर, अपनी धुन और अपना जगन् । व्यक्तित्व छिपा नहीं था। कल्पना दौड़ती ही थी। कुछ व्यक्तियों ने कहा, 'गुरुदेव का स्वर्गवास हो गया है। अब आप पाट पर विराज।' प्रापन निरपेक्ष भाव से कहा, 'पहले देखो, प्राचार्यवर ने अपना उत्तराधिकारी किसे चुना है ? फिर बात करना।' मन्त्री मनि ने डालगणी का पुठा खोला। पत्र निकाला। परिषद् के बीच उसे पढ़ा, तब जनता ने पाश्चयं के साथ मुना कि हमारे प्राचार्य श्री कालगणी है। अब पाप पाट पर बैठे। यह निरपेक्षता अन्तिम सांस तक बनी रही। रुचि का खाना वही था जो ग्रामीण लोग खाते है । ठाट-बाट का कोई प्राकर्षण नही था। बाहरी उपकरण उन्हें कभी नही लुभा पाये। एक ही धुन थी-गण का विकास, विकास और विकास । पहले ही वर्ष उन्होंने साधु-माध्वियों के मान मिधा किये । अपने माथ सिर्फ सोलह साधु रखे। शेष साधुओं से कहा-जामो, विचरो, उपकार करो। संकल्प अवश्य फल पाता है। चतुर्दिक वृद्धि होने लगी। शिप्य-शिष्याएं बढ़ीं, विद्या बढ़ी, बल बढ़ा, गौरव बढा, यश बढ़ा। जो इष्ट था, वह सब-कुछ बढ़ा । उनका प्रयत्न फल लाने लगा। 'भिक्षुशब्दानुशासन' नामक संस्कृत महाव्याघरण बना। संस्कृत काव्य रचे जाने लगे। रचना के अनेक क्षेत्र खुल गए। उन्हें डिगल काव्य बड़े प्रिय थे। चारण लोग पाते ही रहते। कविता-पाठ चलता ही रहता । स्वयं कवि थे। पर ऐसा हो कोई विश्वास बैठ गया, विशेष नहीं लिखते। शिष्यों को प्रेरित करते। उत्साह बढाते। उनकी वाणी मे कोई अपूर्व चमत्कार था। उनकी दृष्टि में कोई अथाह अमृत था। उनका स्पर्श पा एक बार तो मन भी जी उठता।
विकास और विरोध दोनों साथ-साथ चलते हैं। तेरापंथ का यश बढ़ा, वैसे ही विरोध बढा। जैसे विरोध बढ़ा, वैसे उनका सौम्यभाव बढ़ा। प्राचार्यश्री तुलसी को विरोध को 'विनोद' मानने का मंत्र उन्ही से तो मिला था। प्राचार्यश्री ने एक बार कहा था-बाधाओं और विरोध से मेरे दिल में घबराहट नहीं होती। मुझे याद आती है मालवा की वात । गरुदेव रतलाम पधारे । मैं भी उनके साथ था । वहाँ लोगों ने तीव्र विरोध किया। प्राज से दस गना, पर गरुदेव तो