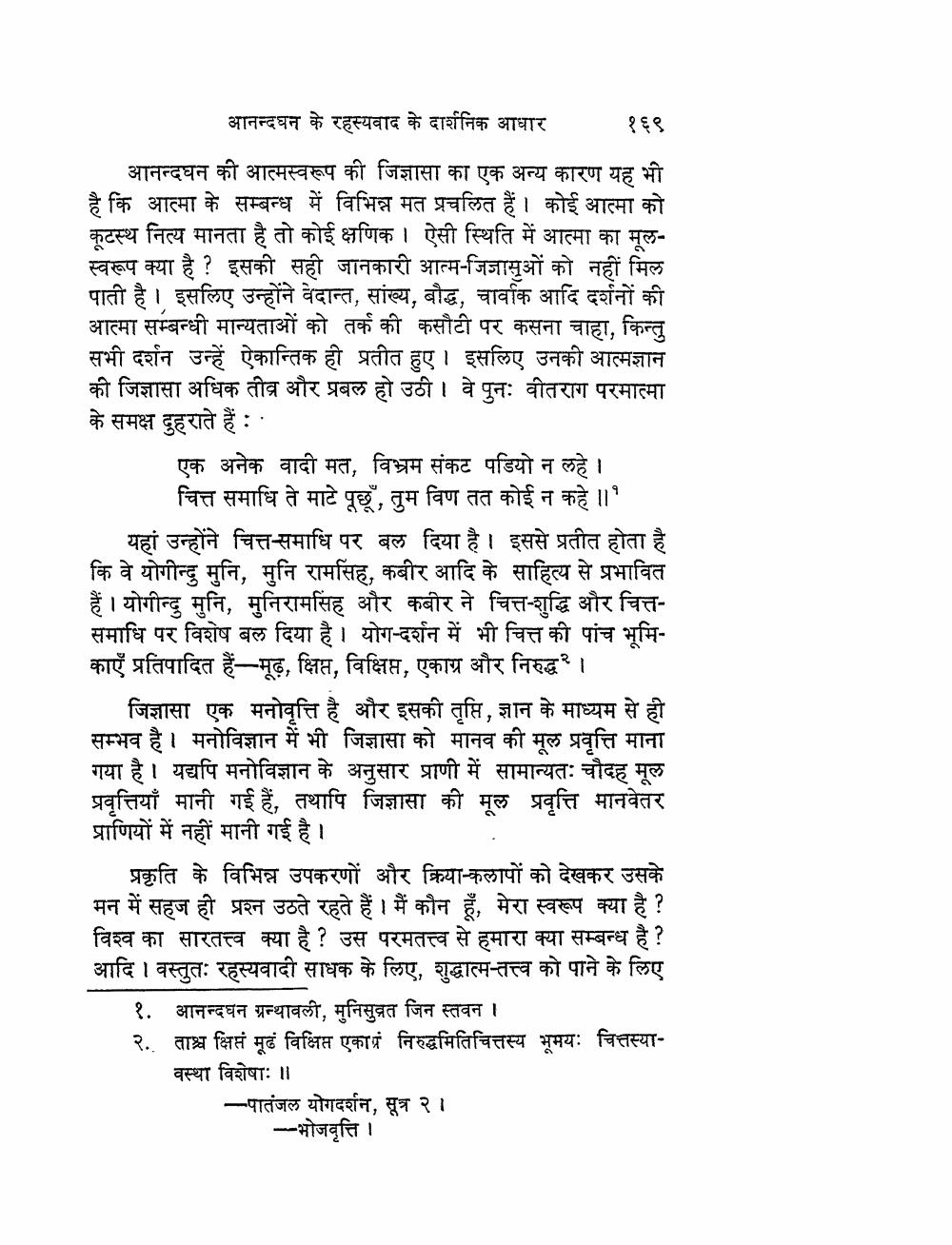________________
आनन्दघन के रहस्यवाद के दार्शनिक आधार
१६९
आनन्दघन की आत्मस्वरूप की जिज्ञासा का एक अन्य कारण यह भी है कि आत्मा के सम्बन्ध में विभिन्न मत प्रचलित हैं। कोई आत्मा को कूटस्थ नित्य मानता है तो कोई क्षणिक । ऐसी स्थिति में आत्मा का मूलस्वरूप क्या है ? इसकी सही जानकारी आत्म-जिज्ञासुओं को नहीं मिल पाती है। इसलिए उन्होंने वेदान्त, सांख्य, बौद्ध, चार्वाक आदि दर्शनों की आत्मा सम्बन्धी मान्यताओं को तर्क की कसौटी पर कसना चाहा, किन्तु सभी दर्शन उन्हें ऐकान्तिक ही प्रतीत हुए। इसलिए उनकी आत्मज्ञान की जिज्ञासा अधिक तीव्र और प्रबल हो उठी। वे पुनः वीतराग परमात्मा के समक्ष दुहराते हैं : .
एक अनेक वादी मत, विभ्रम संकट पडियो न लहे ।
चित्त समाधि ते माटे पूछू, तुम विण तत कोई न कहे ॥' यहां उन्होंने चित्त-समाधि पर बल दिया है। इससे प्रतीत होता है कि वे योगीन्दु मुनि, मुनि रामसिंह, कबीर आदि के साहित्य से प्रभावित हैं । योगीन्दु मुनि, मुनिरामसिंह और कबीर ने चित्त-शुद्धि और चित्तसमाधि पर विशेष बल दिया है। योग-दर्शन में भी चित्त की पांच भूमिकाएँ प्रतिपादित हैं-मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध ।
जिज्ञासा एक मनोवृत्ति है और इसकी तृप्ति , ज्ञान के माध्यम से ही सम्भव है। मनोविज्ञान में भी जिज्ञासा को मानव की मूल प्रवृत्ति माना गया है। यद्यपि मनोविज्ञान के अनुसार प्राणी में सामान्यतः चौदह मूल प्रवृत्तियाँ मानी गई हैं, तथापि जिज्ञासा की मूल प्रवृत्ति मानवेतर प्राणियों में नहीं मानी गई है।
प्रकृति के विभिन्न उपकरणों और क्रिया-कलापों को देखकर उसके मन में सहज ही प्रश्न उठते रहते हैं । मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है ? विश्व का सारतत्त्व क्या है ? उस परमतत्त्व से हमारा क्या सम्बन्ध है ? आदि । वस्तुतः रहस्यवादी साधक के लिए, शुद्धात्म-तत्त्व को पाने के लिए
१. आनन्दघन ग्रन्थावली, मुनिसुव्रत जिन स्तवन । २.. ताश्च क्षिप्तं मूढं विक्षिप्त एकाग्रं निरुद्धमितिचित्तस्य भूमयः चित्तस्यावस्था विशेषाः ॥ -पातंजल योगदर्शन, सूत्र २ ।
--भोजवृत्ति ।