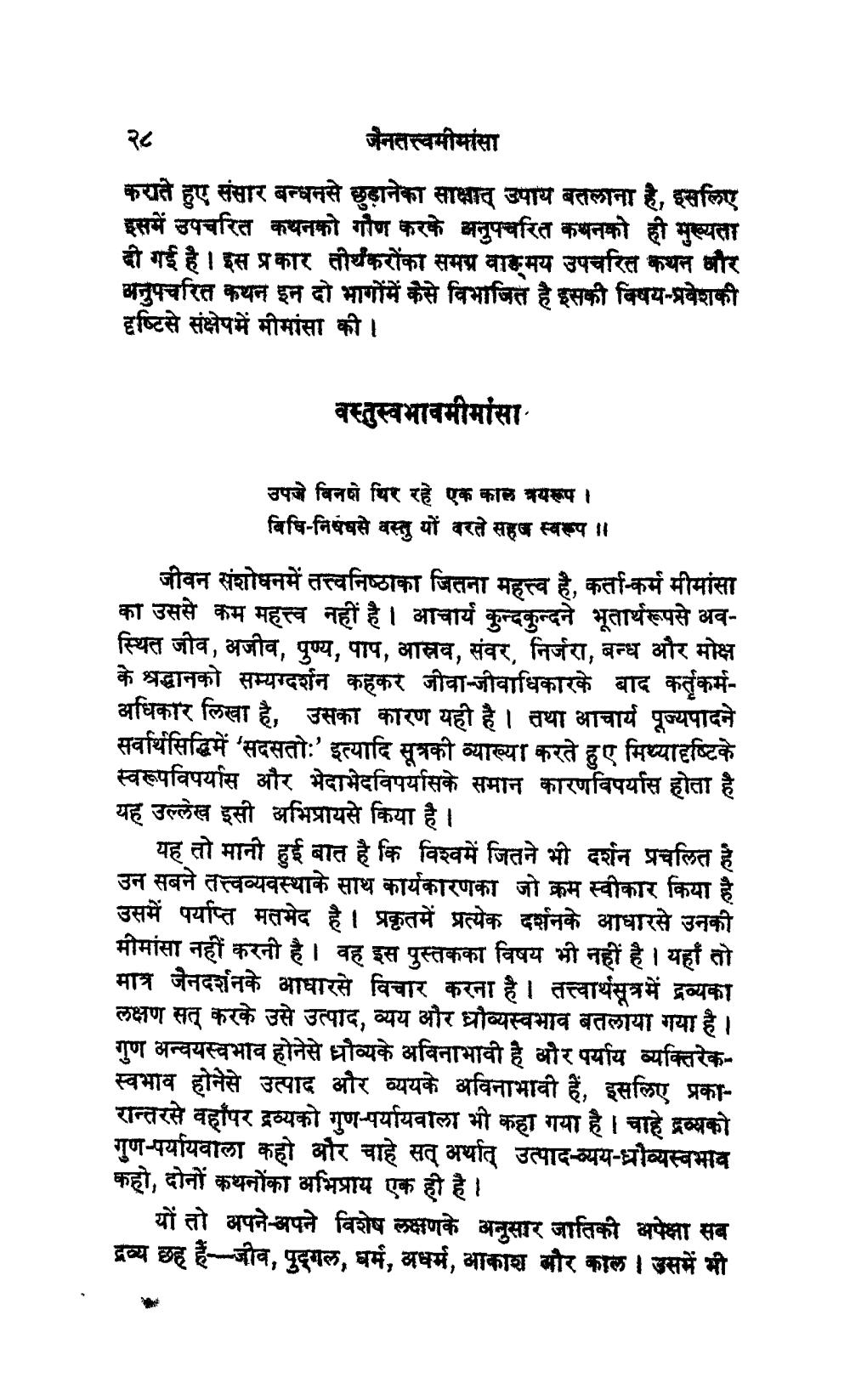________________
जेनतत्वमीमांसा कराते हुए संसार बन्धनसे छुड़ानेका साक्षात् उपाय बतलाना है, इसलिए इसमें उपचरित कथनको गौण करके अनुपचारित कथनको ही मुख्यता दी गई है। इस प्रकार तीर्थकरोंका समग्र वाङ्मय उपचरित कथन और अनुपचरित कथन इन दो भागोंमें कैसे विभाजित है इसकी विषय-प्रबेशकी दृष्टिसे संक्षेपमें मीमांसा की।
वस्तुस्वभावमीमांसा
उपजे विनशे थिर रहे एक काल यरूप ।
विधि-निषषसे वस्तु या वरते सहज स्वरूप ॥ जीवन संशोधनमें तत्त्वनिष्ठाका जितना महत्त्व है, कर्ता-कर्म मीमांसा का उससे कम महत्त्व नहीं है। आचार्य कुन्दकुन्दने भूतार्थरूपसे अवस्थित जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आस्रव, संवर, निर्जरा, बन्ध और मोक्ष के श्रद्धानको सम्यग्दर्शन कहकर जीवा-जीवाधिकारके बाद कर्तृकर्मअधिकार लिखा है, उसका कारण यही है। तथा आचार्य पूज्यपादने सर्वार्थसिद्धिमें 'सदसतोः' इत्यादि सूत्रकी व्याख्या करते हुए मिथ्यादृष्टिके स्वरूपविपर्यास और भेदाभेदविपर्यासके समान कारणविपर्यास होता है यह उल्लेख इसी अभिप्रायसे किया है।
यह तो मानी हुई बात है कि विश्वमें जितने भी दर्शन प्रचलित है उन सबने तत्त्वव्यवस्थाके साथ कार्यकारणका जो क्रम स्वीकार किया है उसमें पर्याप्त मतभेद है। प्रकृतमें प्रत्येक दर्शनके आधारसे उनकी मीमांसा नहीं करनी है। वह इस पुस्तकका विषय भी नहीं है । यहाँ तो मात्र जैनदर्शनके आधारसे विचार करना है। तत्त्वार्थसूत्र में द्रव्यका लक्षण सत् करके उसे उत्पाद, व्यय और ध्रौव्यस्वभाव बतलाया गया है। गुण अन्वयस्वभाव होनेसे ध्रौव्यके अविनाभावी है और पर्याय व्यक्तिरेकस्वभाव होनेसे उत्पाद और व्ययके अविनाभावी हैं, इसलिए प्रकारान्तरसे वहाँपर द्रव्यको गुण-पर्यायवाला भी कहा गया है। चाहे द्रव्यको गुण-पर्यायवाला कहो और चाहे सत् अर्थात् उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यस्वभाव कहो, दोनों कथनोंका अभिप्राय एक ही है।
यों तो अपने-अपने विशेष लक्षणके अनुसार जातिको अपेक्षा सब द्रव्य छह हैं-जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल । उसमें भी