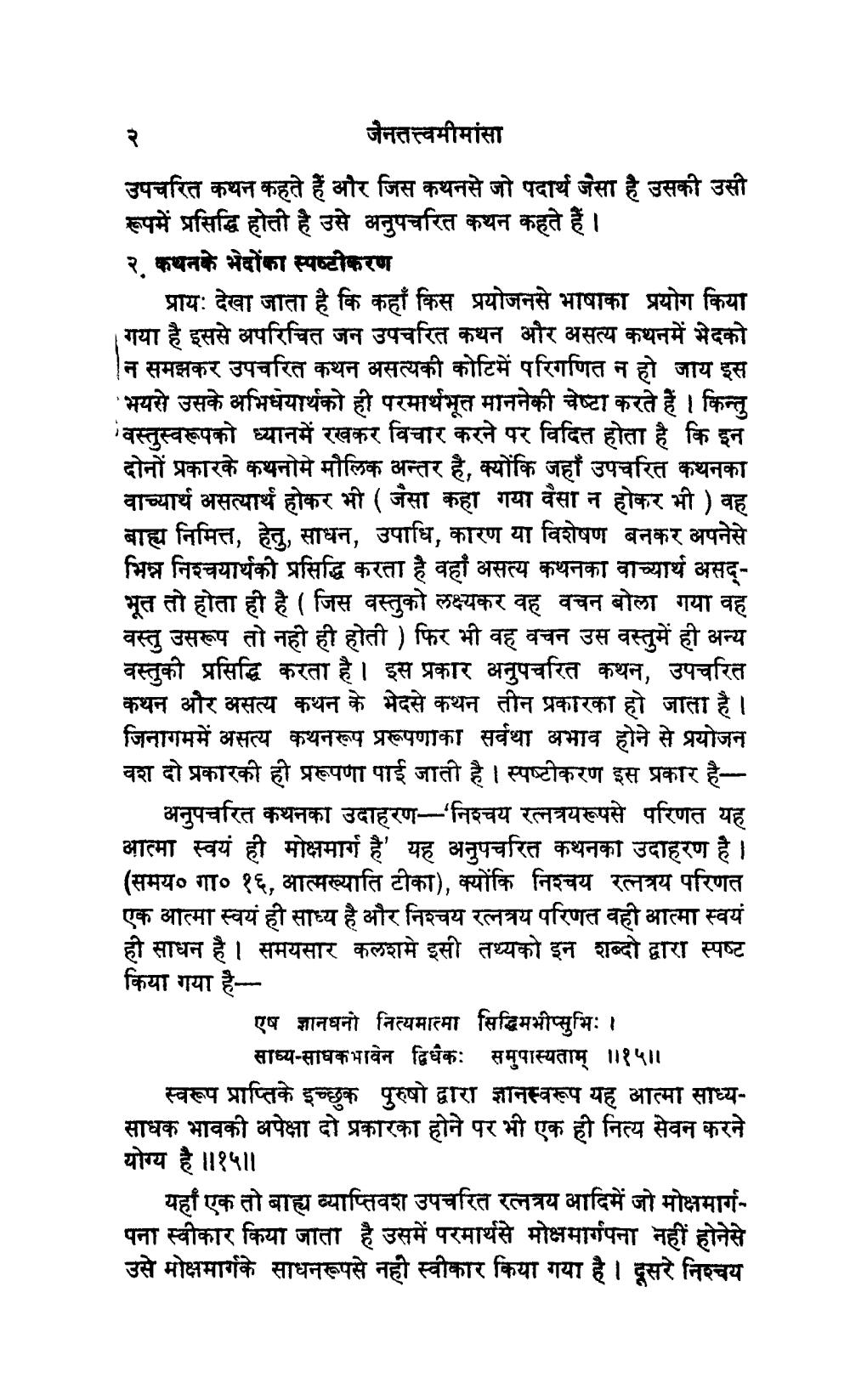________________
जैनतत्त्वमीमांसा उपचरित कथन कहते हैं और जिस कथनसे जो पदार्थ जैसा है उसकी उसी रूपमें प्रसिद्धि होती है उसे अनुपचरित कथन कहते हैं। २. कथनके भेदोंका स्पष्टीकरण
प्रायः देखा जाता है कि कहाँ किस प्रयोजनसे भाषाका प्रयोग किया गया है इससे अपरिचित जन उपचरित कथन और असत्य कथनमें भेदको न समझकर उपचरित कथन असत्यकी कोटिमें परिगणित न हो जाय इस 'भयसे उसके अभिधयार्थको ही परमार्थभूत माननेकी चेष्टा करते हैं । किन्तु वस्तुस्वरूपको ध्यानमें रखकर विचार करने पर विदित होता है कि इन दोनों प्रकारके कथनोमे मौलिक अन्तर है, क्योंकि जहाँ उपचरित कथनका वाच्यार्थ असत्यार्थ होकर भी ( जैसा कहा गया वैसा न होकर भी ) वह बाह्य निमित्त, हेतु, साधन, उपाधि, कारण या विशेषण बनकर अपनेसे भिन्न निश्चयार्थकी प्रसिद्धि करता है वहाँ असत्य कथनका वाच्यार्थ असद्भूत तो होता ही है ( जिस वस्तुको लक्ष्यकर वह वचन बोला गया वह वस्तु उसरूप तो नही ही होती ) फिर भी वह वचन उस वस्तुमें ही अन्य वस्तुकी प्रसिद्धि करता है। इस प्रकार अनुपरित कथन, उपचरित कथन और असत्य कथन के भेदसे कथन तीन प्रकारका हो जाता है। जिनागममें असत्य कथनरूप प्ररूपणाका सर्वथा अभाव होने से प्रयोजन वश दो प्रकारकी ही प्ररूपणा पाई जाती है । स्पष्टीकरण इस प्रकार है____ अनुपरित कथनका उदाहरण-'निश्चय रत्नत्रयरूपसे परिणत यह
आत्मा स्वयं ही मोक्षमार्ग है' यह अनुपचरित कथनका उदाहरण है। (समय० गा० १६, आत्मख्याति टीका), क्योंकि निश्चय रत्नत्रय परिणत एक आत्मा स्वयं ही साध्य है और निश्चय रत्नत्रय परिणत वही आत्मा स्वयं ही साधन है। समयसार कलशमे इसी तथ्यको इन शब्दो द्वारा स्पष्ट किया गया है
एष ज्ञानधनो नित्यमात्मा सिद्धिमभीप्सुभिः ।
साध्य-साधक भावेन द्विधकः समुपास्यताम् ॥१५॥ स्वरूप प्राप्तिके इच्छुक पुरुषो द्वारा ज्ञानस्वरूप यह आत्मा साध्यसाधक भावकी अपेक्षा दो प्रकारका होने पर भी एक ही नित्य सेवन करने योग्य है ॥१५॥
यहाँ एक तो बाह्य व्याप्तिवश उपचरित रत्नत्रय आदिमें जो मोक्षमार्गपना स्वीकार किया जाता है उसमें परमार्थसे मोक्षमार्गपना नहीं होनेसे उसे मोक्षमार्गके साधनरूपसे नही स्वीकार किया गया है। दूसरे निश्चय