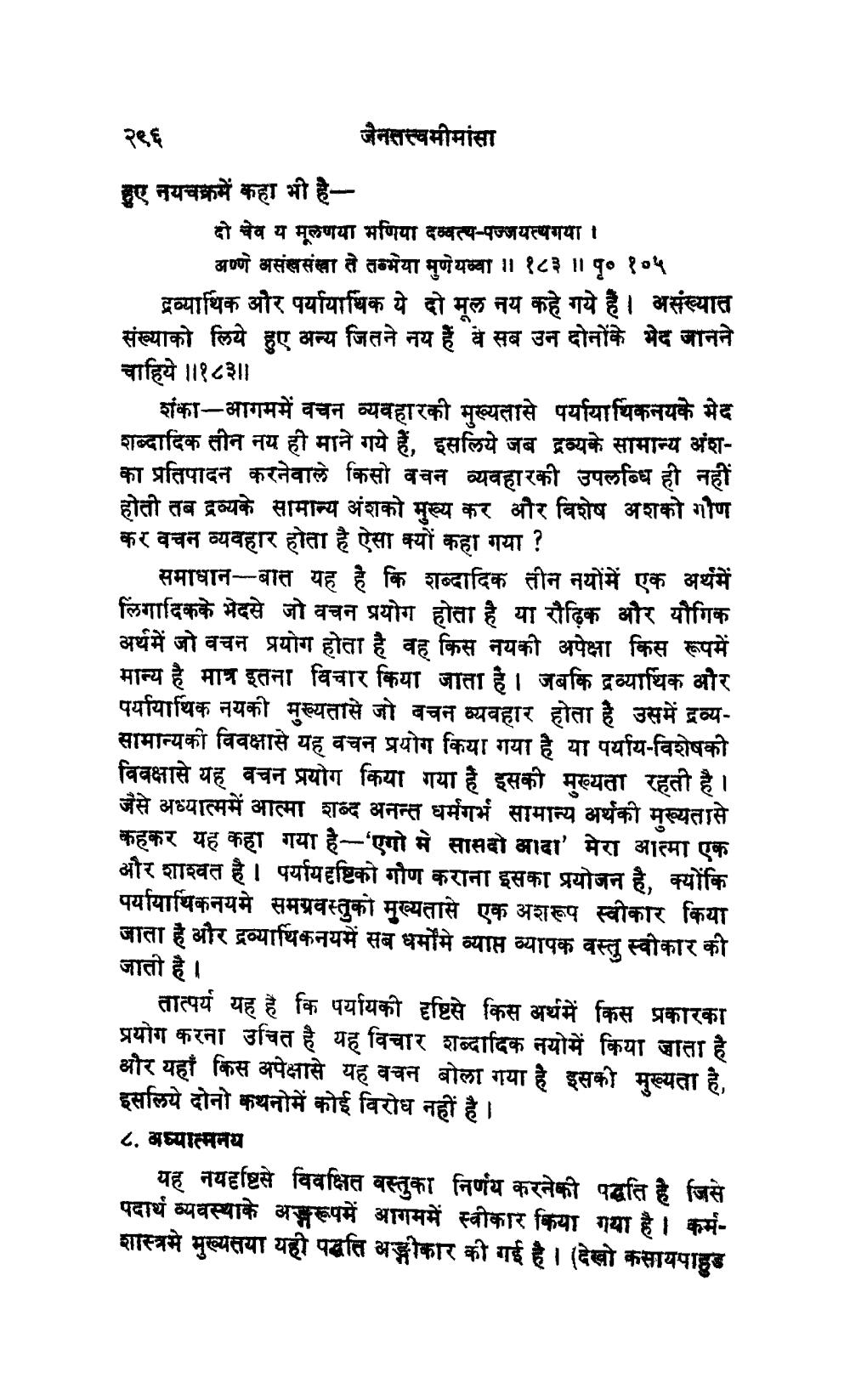________________
२९६
जैनतत्त्वमीमांसा हुए नयचक्रमें कहा भी है
दो चेव य मूलणया भणिया दव्यत्य-पज्जयत्यगया ।
अण्णे असंखसंखा ते तब्भेया मुणे यव्या ।। १८३ ।। पृ० १०५ द्रव्याथिक और पर्यायाधिक ये दो मूल नय कहे गये हैं। असंख्यात संख्याको लिये हुए अन्य जितने नय हैं वे सब उन दोनोंके भेद जानने चाहिये ॥१८३।।
शंका-आगममें वचन व्यवहारकी मुख्यतासे पर्यायाथिकनयके भेद शब्दादिक तीन नय ही माने गये हैं, इसलिये जब द्रव्यके सामान्य अंशका प्रतिपादन करनेवाले किसो वचन व्यवहारकी उपलब्धि ही नहीं होती तब द्रव्यके सामान्य अंशको मुख्य कर और विशेष अशको गौण कर वचन व्यवहार होता है ऐसा क्यों कहा गया ?
समाधान-बात यह है कि शब्दादिक तीन नयोंमें एक अर्थमें लिंगादिकके भेदसे जो वचन प्रयोग होता है या रौदिक और यौगिक अर्थमें जो वचन प्रयोग होता है वह किस नयकी अपेक्षा किस रूपमें मान्य है मात्र इतना विचार किया जाता है। जबकि द्रव्यार्थिक और पर्यायाथिक नयकी मुख्यतासे जो वचन व्यवहार होता है उसमें द्रव्यसामान्यकी विवक्षासे यह वचन प्रयोग किया गया है या पर्याय-विशेषको विवक्षासे यह वचन प्रयोग किया गया है इसकी मुख्यता रहती है। जैसे अध्यात्ममें आत्मा शब्द अनन्त धर्मगर्भ सामान्य अर्थकी मुख्यतासे कहकर यह कहा गया है-'एगो मे सासदो आदा' मेरा आत्मा एक और शाश्वत है। पर्याय दृष्टिको गौण कराना इसका प्रयोजन है, क्योंकि पर्यायाथिकनयमे समग्रवस्तुको मुख्यतासे एक अशरूप स्वीकार किया जाता है और द्रव्यार्थिकनयमें सब धर्मोमे व्याप्त व्यापक वस्तु स्वीकार की जाती है।
तात्पर्य यह है कि पर्यायकी दृष्टिसे किस अर्थमें किस प्रकारका प्रयोग करना उचित है यह विचार शब्दादिक नयोमें किया जाता है और यहाँ किस अपेक्षासे यह वचन बोला गया है इसकी मुख्यता है, इसलिये दोनो कथनोमें कोई विरोध नहीं है। ८. अध्यात्मनय ____ यह नयदृष्टि से विवक्षित वस्तुका निर्णय करनेकी पद्धति है जिसे पदार्थ व्यवस्थाके अङ्गरूपमें आगममें स्वीकार किया गया है। कर्मशास्त्रमे मुख्यतया यही पद्धति अङ्गीकार की गई है। (देखो कसायपाइड