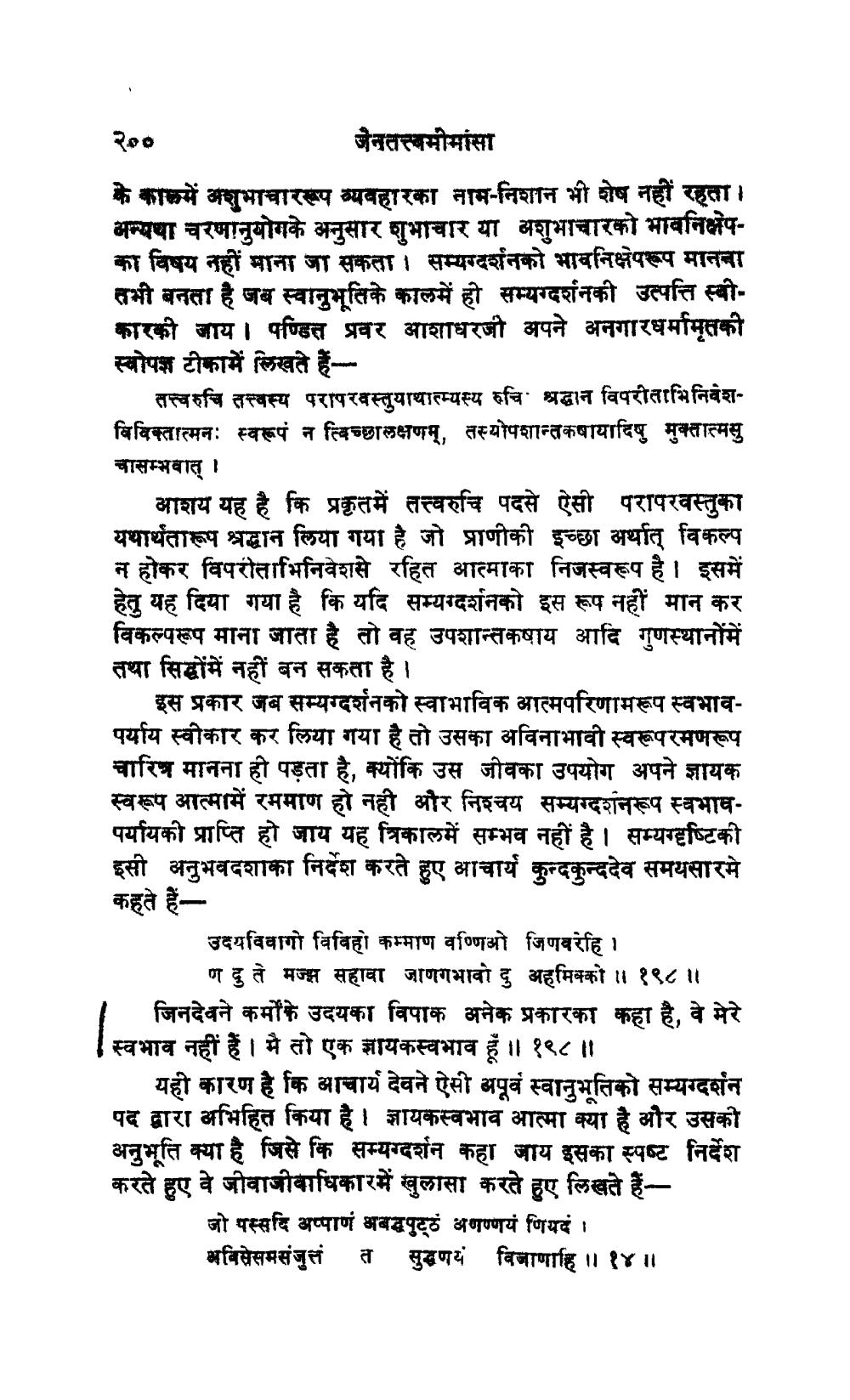________________
२००
जैनतत्त्वमीमांसा के काळमें अशुभाचाररूप व्यवहारका नाम-निशान भी शेष नहीं रहता। अन्यथा चरमानुयोगके अनुसार शुभाचार या अशुभाचारको भावनिक्षेपका विषय नहीं माना जा सकता। सम्यग्दर्शनको भावनिक्षेपरूप मानना तभी बनता है जब स्वानुभूतिके कालमें हो सम्यग्दर्शनकी उत्पत्ति स्वीकारकी जाय । पण्डित प्रवर आशाधरजी अपने अनगारधर्मामृतकी स्वोपक्ष टीकामें लिखते हैं
तत्त्वरुचि तत्त्वस्य परापरवस्तुयाथात्म्यस्य रुचि श्रद्धान विपरीताभिनिवेशविविक्तात्मनः स्वरूपं न विच्छालक्षणम्, तस्योपशान्तकषायादिषु मुक्तात्मसु चासम्भवात् ।
आशय यह है कि प्रकृतमें तत्त्वरुचि पदसे ऐसी परापरवस्तुका यथार्थतारूप श्रद्धान लिया गया है जो प्राणीकी इच्छा अर्थात् विकल्प न होकर विपरीताभिनिवेशसे रहित आत्माका निजस्वरूप है। इसमें हेतु यह दिया गया है कि यदि सम्यग्दर्शनको इस रूप नहीं मान कर विकल्परूप माना जाता है तो वह उपशान्तकषाय आदि गुणस्थानोंमें तथा सिद्धोंमें नहीं बन सकता है।
इस प्रकार जब सम्यग्दर्शनको स्वाभाविक आत्मपरिणामरूप स्वभावपर्याय स्वीकार कर लिया गया है तो उसका अविनाभावी स्वरूपरमणरूप चारित्र मानना ही पड़ता है, क्योंकि उस जीवका उपयोग अपने ज्ञायक स्वरूप आत्मामें रममाण हो नही और निश्चय सम्यग्दर्शनरूप स्वभावपर्यायकी प्राप्ति हो जाय यह त्रिकालमें सम्भव नहीं है। सम्यग्दृष्टिकी इसी अनुभवदशाका निर्देश करते हुए आचार्य कुन्दकुन्ददेव समयसारमे कहते हैं
उदयविवागो विविहो कम्माण वणिओ जिणवरहि ।
ण दु ते मझ सहावा जाणगभावो दु अहमिक्को ।। १९८॥ । जिनदेवने कर्मोंके उदयका विपाक अनेक प्रकारका कहा है, वे मेरे | स्वभाव नहीं हैं । मै तो एक ज्ञायकस्वभाव हूँ॥ १९८ ।।
यही कारण है कि आचार्य देवने ऐसी अपूर्व स्वानुभूतिको सम्यग्दर्शन पद द्वारा अभिहित किया है। ज्ञायकस्वभाव आत्मा क्या है और उसकी अनुभूति क्या है जिसे कि सम्यग्दर्शन कहा जाय इसका स्पष्ट निर्देश करते हुए वे जीवाजीवाधिकारमें खुलासा करते हुए लिखते हैं
जो पस्सदि अप्पाणं अबद्धपुढें अणण्णय णियदं । अविसेसमजुत्तं त सुद्धणयं विजाणाहि ॥ १४ ॥