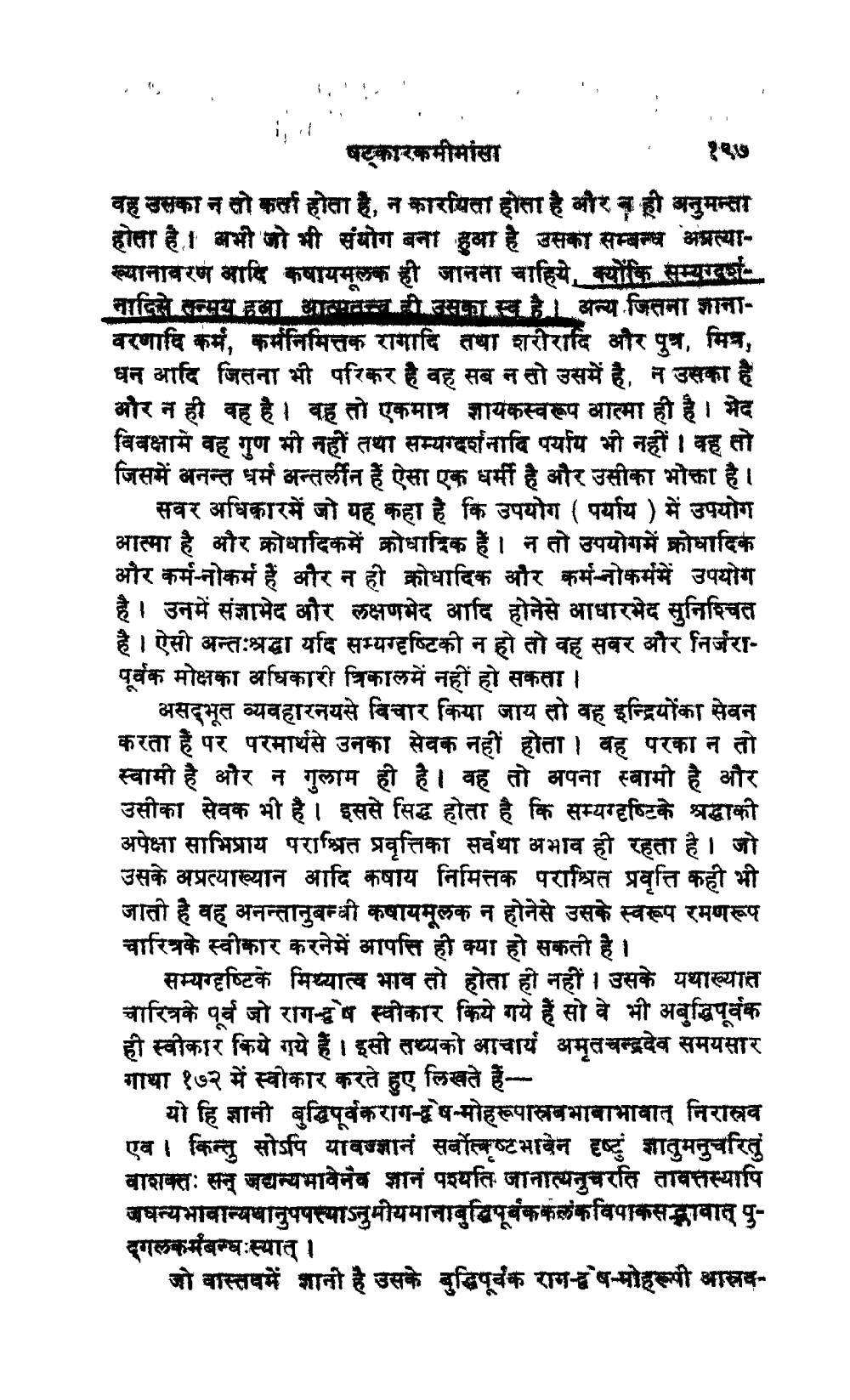________________
षटकारकमीमांसा
१९७ वह उसका न तो कर्ता होता है, न कारमिता होता है और न ही अनुमन्ता होता है। अभी जो भी संबोग बना हुआ है उसका सम्बन्ध अप्रत्याख्यानावरण आदि कषायमूलक ही जानना चाहिये, क्योंकि सम्यग्दर्शसादिले हन्सय हा सामनन ही उसका स्व है। अन्य जितना ज्ञानावरणादि कर्म, कर्मनिमित्तक रागादि तथा शरीरादि और पुत्र, मित्र, धन आदि जितना भी परिकर है वह सब न तो उसमें है, न उसका है
और न ही वह है। वह तो एकमात्र ज्ञायकस्वरूप आत्मा ही है । भेद विवक्षामें वह गुण भी नहों तथा सम्यग्दर्शनादि पर्याय भी नहीं। वह तो जिसमें अनन्त धर्म अन्तर्लीन हैं ऐसा एक धर्मी है और उसीका भोक्ता है।
सवर अधिकारमें जो यह कहा है कि उपयोग ( पर्याय ) में उपयोग आस्मा है और क्रोधादिकमें क्रोधादिक हैं। न तो उपयोगमें क्रोधादिक और कर्म-नोकर्म हैं और न ही क्रोधादिक और कर्म-नोकर्ममें उपयोग है। उनमें संज्ञाभेद और लक्षणभेद आदि होनेसे आधारभेद सुनिश्चित है। ऐसी अन्तःश्रद्धा यदि सम्यग्दृष्टिकी न हो तो वह सवर और निर्जरापूर्वक मोक्षका अधिकारी त्रिकालमें नहीं हो सकता।
असद्भूत व्यवहारनयसे विचार किया जाय तो वह इन्द्रियोंका सेवन करता हैं पर परमार्थसे उनका सेवक नहीं होता। वह परका न तो स्वामी है और न गुलाम ही है। वह तो अपना स्वामी है और उसीका सेवक भी है। इससे सिद्ध होता है कि सम्यग्दृष्टिके श्रद्धाकी अपेक्षा साभिप्राय पराश्रित प्रवृत्तिका सर्वथा अभाव ही रहता है। जो उसके अप्रत्याख्यान आदि कषाय निमित्तक पराश्रित प्रवृत्ति कही भी जाती है वह अनन्तानुबन्धी कषायमूलक न होनेसे उसके स्वरूप रमणरूप चारित्रके स्वीकार करनेमें आपत्ति ही क्या हो सकती है।
सम्यग्दृष्टिके मिथ्यात्व भाव तो होता ही नहीं। उसके यथाख्यात चारित्रके पूर्व जो राग-द्वष स्वीकार किये गये हैं सो वे भी अबुद्धिपूर्वक ही स्वीकार किये गये हैं। इसी तथ्यको आचार्य अमृतचन्द्रदेव समयसार गाथा १७२ में स्वीकार करते हुए लिखते हैं
यो हि ज्ञानी बुद्धिपूर्वकराग-द्वेष-मोहरूपासवभावाभावात् निरालव एव । किन्तु सोऽपि यावण्ज्ञानं सर्वोत्कृष्टभावेन दृष्टुं ज्ञातुमनुचरितुं वाशक्तः सन् जघन्यभावेनैव शानं पश्यति जानात्यनुचरति तावत्तस्यापि जघन्यभावान्यषानुपपस्याऽनुमीयमानाबुद्धिपूर्वककलंकविपाकसद्भावात् पुद्गलकर्मबन्धःस्यात् ।
जो वास्तवमें ज्ञानी है उसके बुद्धिपूर्वक राग-द्वेष-मोहरूपी आरक