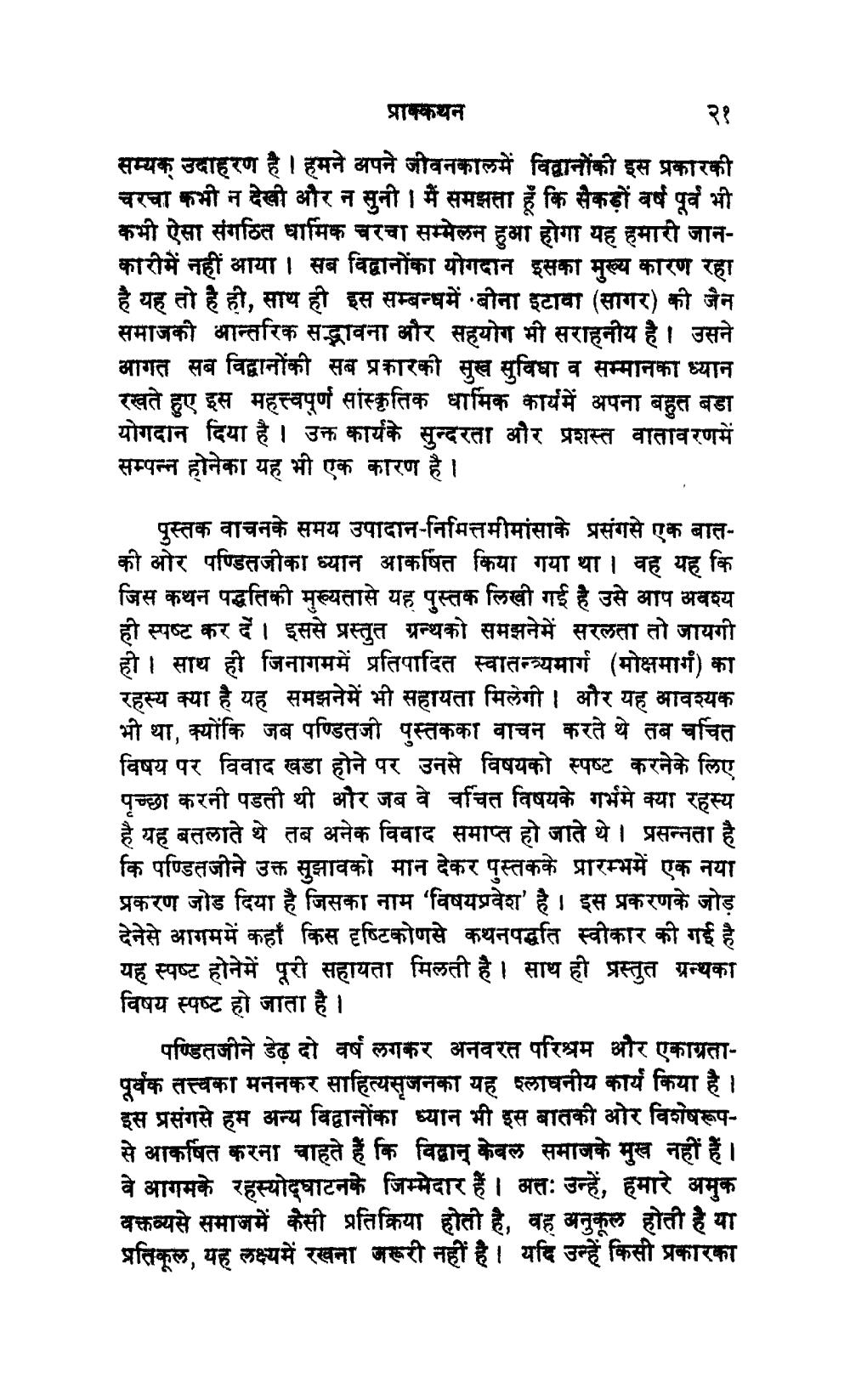________________
प्राक्कथन
सम्यक उदाहरण है। हमने अपने जीवनकालमें विद्वानोंकी इस प्रकारकी चरचा कभी न देखी और न सुनी । मैं समझता हूँ कि सैकड़ों वर्ष पूर्व भी कभी ऐसा संगठित धार्मिक चरचा सम्मेलन हुमा होगा यह हमारी जानकारीमें नहीं आया। सब विद्वानोंका योगदान इसका मुख्य कारण रहा है यह तो है ही, साथ ही इस सम्बन्ध में बीना इटावा (सागर) की जैन समाजकी आन्तरिक सद्भावना और सहयोग भी सराहनीय है। उसने आगत सब विद्वानोंकी सब प्रकारकी सुख सुविधा व सम्मानका ध्यान रखते हुए इस महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक धार्मिक कार्य में अपना बहुत बडा योगदान दिया है। उक्त कार्यके सुन्दरता और प्रशस्त वातावरणमें सम्पन्न होनेका यह भी एक कारण है।
पुस्तक वाचनके समय उपादान-निमित्तमीमांसाके प्रसंगसे एक बातकी ओर पण्डितजीका ध्यान आकर्षित किया गया था। वह यह कि जिस कथन पद्धतिकी मुख्यतासे यह पुस्तक लिखी गई है उसे आप अवश्य ही स्पष्ट कर दें। इससे प्रस्तुत ग्रन्थको समझनेमें सरलता तो जायगी ही। साथ ही जिनागममें प्रतिपादित स्वातन्त्र्यमार्ग (मोक्षमार्ग) का रहस्य क्या है यह समझने में भी सहायता मिलेगी। और यह आवश्यक भी था, क्योंकि जब पण्डितजी पुस्तकका वाचन करते थे तब चचित विषय पर विवाद खडा होने पर उनसे विषयको स्पष्ट करनेके लिए पृच्छा करनी पडती थी और जब वे चचित विषयके गर्भमे क्या रहस्य है यह बतलाते थे तब अनेक विवाद समाप्त हो जाते थे। प्रसन्नता है कि पण्डितजीने उक्त सुझावको मान देकर पुस्तकके प्रारम्भमें एक नया प्रकरण जोड दिया है जिसका नाम 'विषयप्रवेश' है । इस प्रकरणके जोड़ देनेसे आगममें कहाँ किस दृष्टिकोणसे कथनपद्धति स्वीकार की गई है यह स्पष्ट होनेमें पूरी सहायता मिलती है। साथ ही प्रस्तुत ग्रन्थका विषय स्पष्ट हो जाता है।
पण्डितजीने डेढ़ दो वर्ष लगकर अनवरत परिश्रम और एकाग्रतापूर्वक तत्त्वका मननकर साहित्यसृजनका यह श्लाघनीय कार्य किया है। इस प्रसंगसे हम अन्य विद्वानोंका ध्यान भी इस बातकी ओर विशेषरूपसे आकर्षित करना चाहते हैं कि विद्वान् केवल समाजके मुख नहीं हैं। वे आगमके रहस्योद्घाटनके जिम्मेदार हैं। अतः उन्हें, हमारे अमुक वक्तव्यसे समाजमें केसी प्रतिक्रिया होती है, वह अनुकूल होती है या प्रतिकूल, यह लक्ष्यमें रखना जरूरी नहीं है। यदि उन्हें किसी प्रकारका