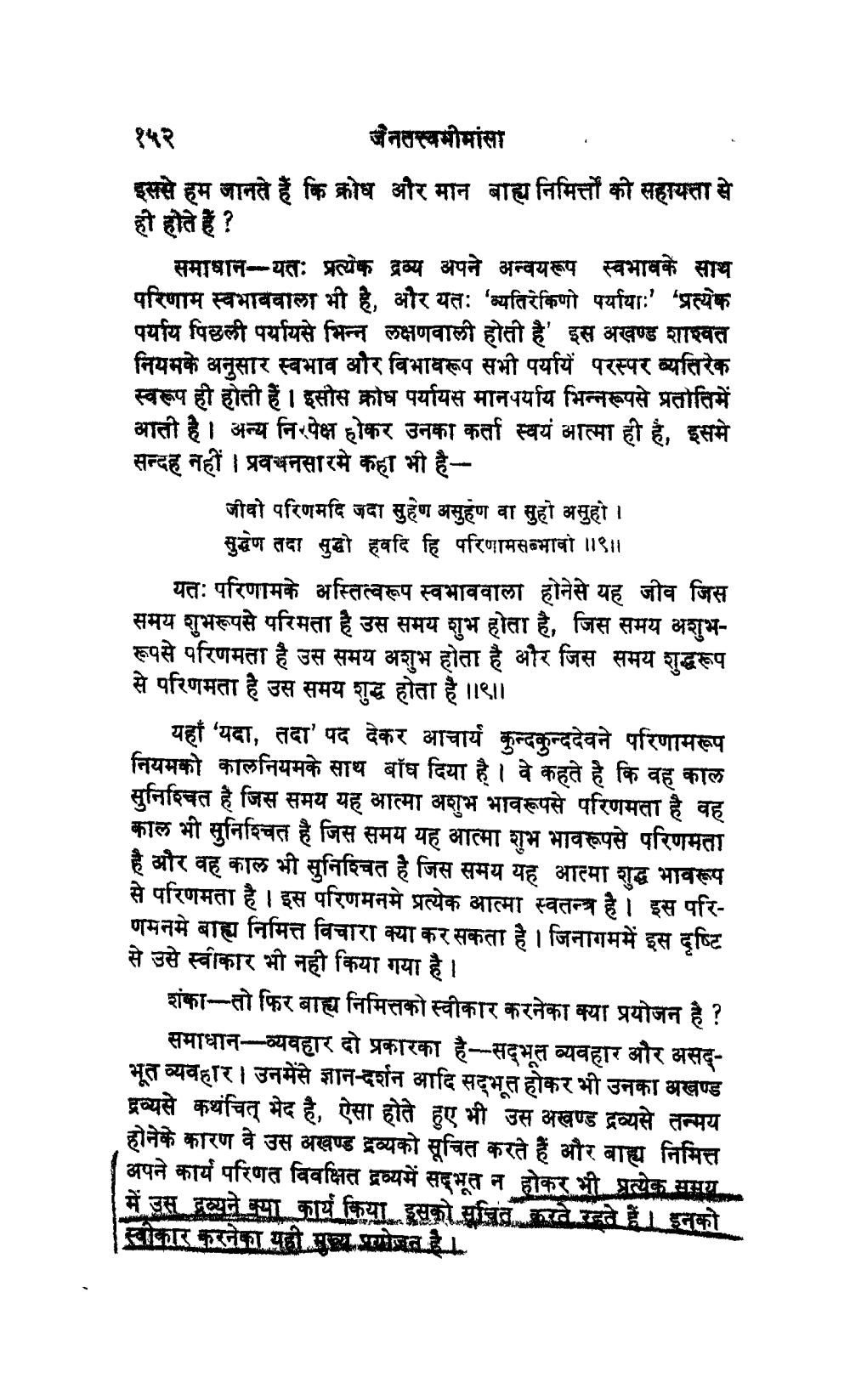________________
१५२
जनतत्त्वमीमांसा इससे हम जानते हैं कि क्रोध और मान बाह्य निमित्तों को सहायता से ही होते हैं ?
समाधान-यतः प्रत्येक द्रव्य अपने अन्वयरूप स्वभावके साथ परिणाम स्वभाववाला भी है, और यतः 'व्यतिरेकिणो पर्यायाः' 'प्रत्येक पर्याय पिछली पर्यायसे भिन्न लक्षणवाली होती है। इस अखण्ड शाश्वत नियमके अनुसार स्वभाव और विभावरूप सभी पर्यायें परस्पर व्यतिरेक स्वरूप ही होती हैं । इसीस क्रोध पर्यायस मानपर्याय भिन्नरूपसे प्रतोतिमें आती है। अन्य निरपेक्ष होकर उनका कर्ता स्वयं आत्मा ही है, इसमे सन्दह नहीं । प्रवचनसारमे कहा भी है
जीवो परिणमदि जदा सुहेण असुहण वा सुहो असुहो।
सुद्धेण तदा सुद्धो हवदि हि परिणामसब्भावो ॥९॥ यतः परिणामके अस्तित्वरूप स्वभाववाला होनेसे यह जीव जिस समय शुभरूपसे परिमता है उस समय शुभ होता है, जिस समय अशुभरूपसे परिणमता है उस समय अशुभ होता है और जिस समय शुद्धरूप से परिणमता है उस समय शुद्ध होता है ॥९॥
यहाँ 'यदा, तदा' पद देकर आचार्य कुन्दकुन्ददेवने परिणामरूप नियमको कालनियमके साथ बाँध दिया है। वे कहते है कि वह काल सुनिश्चित है जिस समय यह आत्मा अशुभ भावरूपसे परिणमता है वह काल भी सुनिश्चित है जिस समय यह आत्मा शुभ भावरूपसे परिणमता है और वह काल भी सुनिश्चित है जिस समय यह आत्मा शुद्ध भावरूप से परिणमता है । इस परिणमनमे प्रत्येक आत्मा स्वतन्त्र है। इस परिणमनमे बाह्य निमित्त विचारा क्या कर सकता है । जिनागममें इस दृष्टि से उसे स्वीकार भी नही किया गया है ।
शंका-तो फिर बाह्य निमित्तको स्वीकार करनेका क्या प्रयोजन है ?
समाधान-व्यवहार दो प्रकारका है-सद्भुत व्यवहार और असद्भूत व्यवहार। उनमेंसे ज्ञान-दर्शन आदि सद्भूत होकर भी उनका अखण्ड द्रव्यसे कथंचित् भेद है, ऐसा होते हुए भी उस अखण्ड द्रव्यसे तन्मय होनेके कारण वे उस अखण्ड द्रव्यको सूचित करते हैं और बाह्य निमित्त अपने कार्य परिणत विवक्षित द्रव्यमें सद्भूत न होकर भी प्रत्येक समय ... में उस व्यने क्या कार्य किया इसको सचित करते रहते हैं। इनको स्वीकार करने का यही मुख्य प्रयोजन है ।
BR
PRANASI