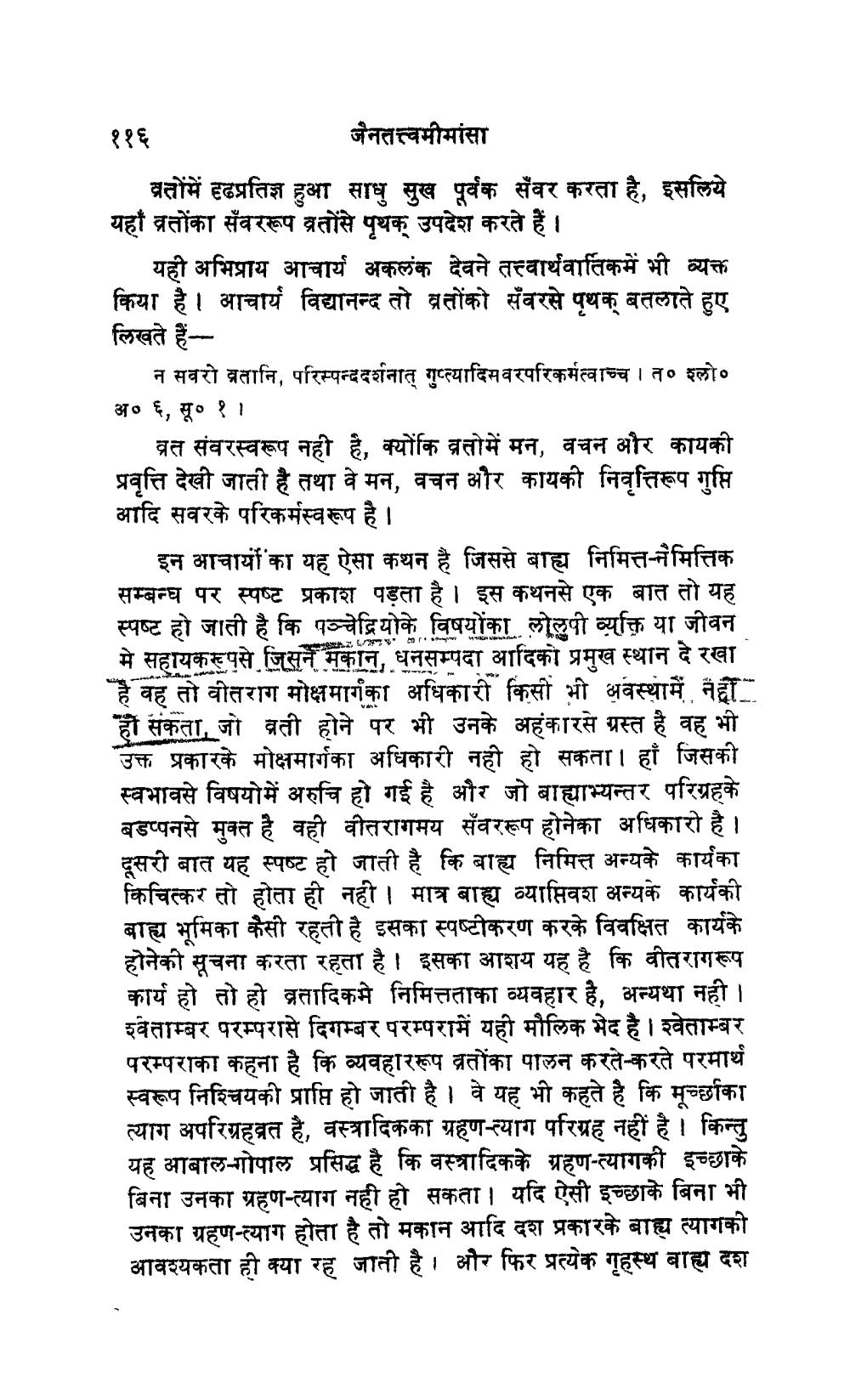________________
११६
जैनतत्त्वमीमांसा व्रतोंमें दृढप्रतिज्ञ हुआ साधु सुख पूर्वक सँवर करता है, इसलिये यहाँ व्रतोंका सँवररूप व्रतोंसे पृथक् उपदेश करते हैं । ___ यही अभिप्राय आचार्य अकलंक देवने तत्त्वार्थवातिकमें भी व्यक्त किया है। आचार्य विद्यानन्द तो व्रतोंको सँवरसे पृथक् बतलाते हुए लिखते हैं
न सवरो व्रतानि, परिस्पन्ददर्शनात् गुप्त्यादिसवरपरिकर्मत्वाच्च । त० श्लो० अ० ६, सू० १।
व्रत संवरस्वरूप नहीं है, क्योंकि व्रतोमें मन, वचन और कायकी प्रवृत्ति देखी जाती है तथा वे मन, वचन और कायकी निवृत्तिरूप गुप्ति आदि सवरके परिकर्मस्वरूप है।
इन आचार्यों का यह ऐसा कथन है जिससे बाह्य निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध पर स्पष्ट प्रकाश पड़ता है। इस कथनसे एक बात तो यह स्पष्ट हो जाती है कि पञ्चेद्रियोके विषयोंका लोलुपी व्यक्ति या जीवन मे सहायकरूपसे जिसने मकान, धनसम्पदा आदिको प्रमुख स्थान दे रखा है वह तो वीतराग मोक्षमार्गका अधिकारी किसी भी अवस्थामें नहीं हो सकता, जो व्रती होने पर भी उनके अहंकारसे ग्रस्त है वह भी उक्त प्रकारके मोक्षमार्गका अधिकारी नही हो सकता। हाँ जिसकी स्वभावसे विषयोमें अरुचि हो गई है और जो बाह्याभ्यन्तर परिग्रहके बडप्पनसे मुक्त है वही वीतरागमय सँवररूप होनेका अधिकारी है। दूसरी बात यह स्पष्ट हो जाती है कि बाह्य निमित्त अन्यके कार्यका किचित्कर तो होता ही नही। मात्र बाह्य व्याप्तिवश अन्यके कार्यकी बाह्य भूमिका कैसी रहती है इसका स्पष्टीकरण करके विवक्षित कार्यके होनेकी सूचना करता रहता है। इसका आशय यह है कि वीतरागरूप कार्य हो तो हो व्रतादिकमे निमित्तताका व्यवहार है, अन्यथा नही । श्वेताम्बर परम्परासे दिगम्बर परम्परामें यही मौलिक भेद है। श्वेताम्बर परम्पराका कहना है कि व्यवहाररूप व्रतोंका पालन करते-करते परमार्थ स्वरूप निश्चियकी प्राप्ति हो जाती है। वे यह भी कहते है कि मीका त्याग अपरिग्रहव्रत है, वस्त्रादिकका ग्रहण-त्याग परिग्रह नहीं है। किन्तु यह आबाल-गोपाल प्रसिद्ध है कि वस्त्रादिकके ग्रहण-त्यागकी इच्छाके बिना उनका ग्रहण-त्याग नहीं हो सकता। यदि ऐसी इच्छाके बिना भी उनका ग्रहण-त्याग होता है तो मकान आदि दश प्रकारके बाह्य त्यागकी आवश्यकता ही क्या रह जाती है। और फिर प्रत्येक गृहस्थ बाह्य दश