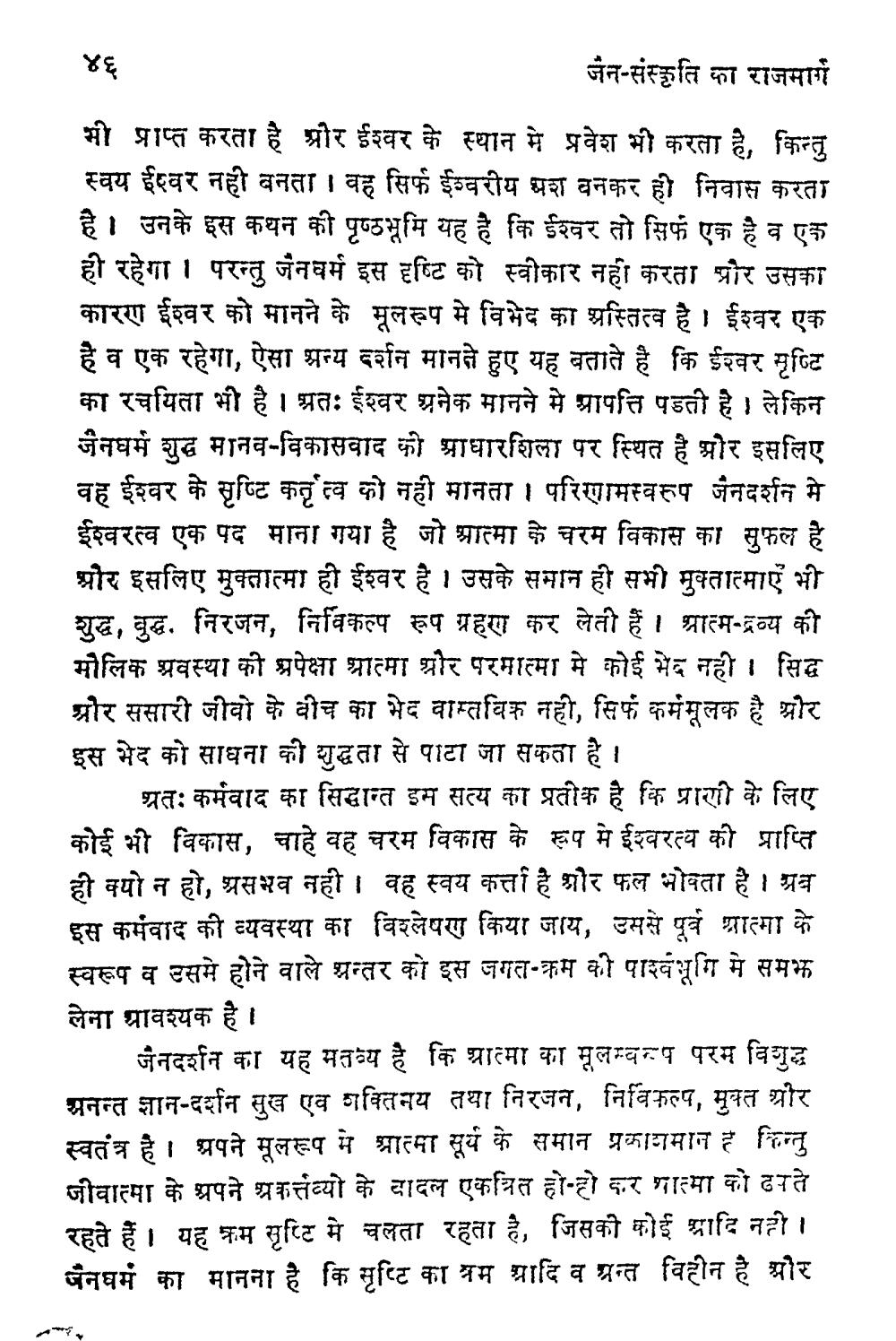________________
जैन-संस्कृति का राजमार्ग भी प्राप्त करता है और ईश्वर के स्थान में प्रवेश भी करता है, किन्तु स्वय ईश्वर नही बनता । वह सिर्फ ईश्वरीय प्रश बनकर ही निवास करता है। उनके इस कथन की पृष्ठभूमि यह है कि ईश्वर तो सिर्फ एक है व एक ही रहेगा। परन्तु जैनधर्म इस दृष्टि को स्वीकार नहीं करता और उसका कारण ईश्वर को मानने के मूलरूप मे विभेद का अस्तित्व है। ईश्वर एक है व एक रहेगा, ऐसा अन्य दर्शन मानते हुए यह बताते है कि ईश्वर मृष्टि का रचयिता भी है । अतः ईश्वर अनेक मानने मे आपत्ति पड़ती है। लेकिन जैनधर्म शुद्ध मानव-विकासवाद की आधारशिला पर स्थित है और इसलिए वह ईश्वर के सृष्टि कर्तृत्व को नही मानता । परिणामस्वरूप जनदर्शन मे ईश्वरत्व एक पद माना गया है जो प्रात्मा के चरम विकास का सुफल है और इसलिए मुक्तात्मा ही ईश्वर है । उसके समान ही सभी मुक्तात्माएं भी शुद्ध, बुद्ध. निरजन, निर्विकल्प रूप ग्रहण कर लेती हैं। प्रात्म-द्रव्य की मौलिक अवस्था की अपेक्षा श्रात्मा और परमात्मा मे कोई भेद नहीं। सिद्ध और ससारी जीवो के बीच का भेद वास्तविक नही, सिर्फ कर्ममूलक है और इस भेद को साधना की शुद्धता से पाटा जा सकता है।
श्रतः कर्मवाद का सिद्धान्त इम सत्य का प्रतीक है कि प्रासी के लिए कोई भी विकास, चाहे वह चरम विकास के रूप मे ईश्वरत्व की प्राप्ति ही क्यो न हो, असभव नही। वह स्वय कर्ता है और फल भोक्ता है । अब इस कर्मवाद की व्यवस्था का विश्लेषण किया जाय, उससे पूर्व प्रात्मा के स्वरूप व उसमे होने वाले अन्तर को इस जगत-क्रम की पाश्वभूमि मे समझ लेना पावश्यक है।
जैनदर्शन का यह मतव्य है कि प्रात्मा का मूलम्बम्प परम विगुद्ध अनन्त ज्ञान-दर्शन सुख एव शक्तिनय तथा निरजन, निर्विकल्प, मुक्त और स्वतंत्र है। अपने मूलरूप मे प्रात्मा सूर्य के समान प्रकागमान है किन्तु जीवात्मा के अपने कर्तव्यो के दादल एकत्रित हो-हो कर पात्मा को ढरते रहते हैं। यह क्रम सृष्टि मे चलता रहता है, जिसकी कोई प्रादि नहीं । जैनधर्म का मानना है कि सृष्टि का श्रम प्रादि व अन्त विहीन है और