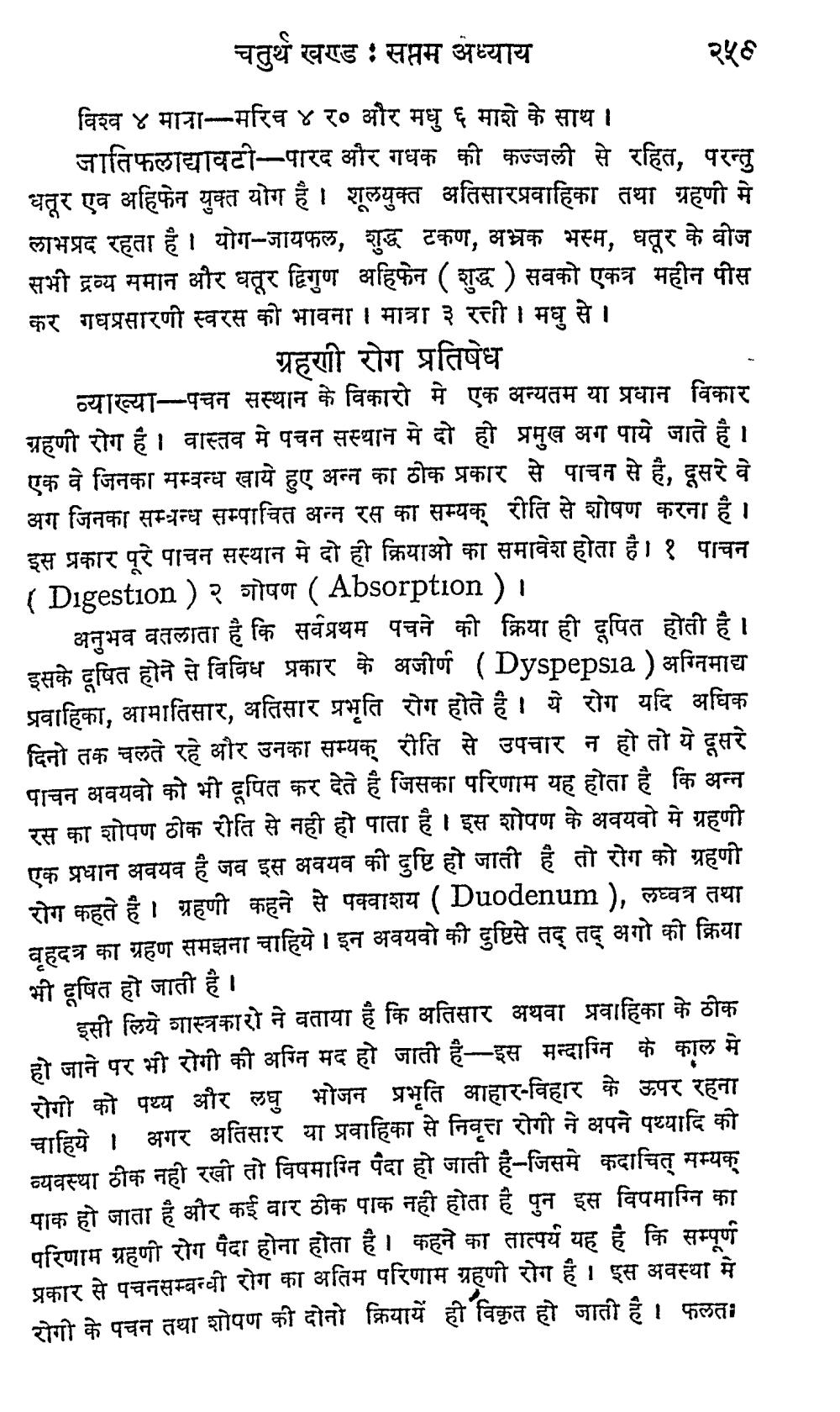________________
२५०
चतुर्थ खण्ड : सप्तम अध्याय विश्व ४ माना-मरिच ४ र० और मधु ६ माशे के साथ ।
जातिफलाद्यावटी-पारद और गधक की कज्जली से रहित, परन्तु धतूर एव अहिफेन युक्त योग है। शूलयुक्त अतिसारप्रवाहिका तथा ग्रहणी मे लाभप्रद रहता है। योग-जायफल, शुद्ध टकण, अभ्रक भस्म, धतूर के बीज सभी द्रव्य समान और धतूर द्विगुण' अहिफेन (शुद्ध) सवको एकत्र महीन पीस कर गधप्रसारणी स्वरस को भावना । मात्रा ३ रत्ती। मधु से।
ग्रहणी रोग प्रतिषेध व्याख्या-पचन संस्थान के विकारो मे एक अन्यतम या प्रधान विकार ग्रहणी रोग है। वास्तव मे पचन संस्थान मे दो हो प्रमुख अग पाये जाते है। एक वे जिनका सम्बन्ध खाये हुए अन्न का ठोक प्रकार से पाचन से है, दूसरे वे अग जिनका सम्बन्ध सम्पाचित अन्न रस का सम्यक् रीति से शोषण करना है। इस प्रकार पूरे पाचन सस्थान मे दो ही क्रियाओ का समावेश होता है। १ पाचन ( Digestion ) २ गोषण ( Absorption )।
अनुभव बतलाता है कि सर्वप्रथम पचने की क्रिया ही दूपित होती है। इसके दूषित होने से विविध प्रकार के अजीर्ण ( Dyspepsia) अग्निमाद्य प्रवाहिका, आमातिसार, अतिसार प्रभृति रोग होते है। ये रोग यदि अधिक दिनो तक चलते रहे और उनका सम्यक् रीति से उपचार न हो तो ये दूसरे पाचन अवयवो को भी दूपित कर देते है जिसका परिणाम यह होता है कि अन्न रस का शोपण ठोक रीति से नही हो पाता है । इस शोपण के अवयवो मे ग्रहणी एक प्रधान अवयव है जव इस अवयव की दुष्टि हो जाती है तो रोग को ग्रहणी रोग कहते है । ग्रहणी कहने से पक्वाशय ( Duodenum ), लघ्वत्र तथा बृहदत्र का ग्रहण समझना चाहिये । इन अवयवो की दुष्टिसे तद् तद् अगो को क्रिया भी दूषित हो जाती है।
इसी लिये शास्त्रकारो ने बताया है कि अतिसार अथवा प्रवाहिका के ठीक हो जाने पर भी रोगी की अग्नि मद हो जाती है-इस मन्दाग्नि के काल मे रोगी को पथ्य और लघु भोजन प्रभृति आहार-विहार के ऊपर रहना चाहिये । अगर अतिसार या प्रवाहिका से निवृत्त रोगी ने अपने पथ्यादि को व्यवस्था ठीक नहीं रखी तो विषमाग्नि पैदा हो जाती है-जिसमे कदाचित् सम्यक् पाक हो जाता है और कई बार ठीक पाक नही होता है पुन इस विपमाग्नि का परिणाम ग्रहणी रोग पैदा होना होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सम्पर्ण प्रकार से पचनसम्बन्धी रोग का अतिम परिणाम ग्रहणी रोग है। इस अवस्था में रोगी के पचन तथा शोपण की दोनो क्रियायें ही विकृत हो जाती है। फलतः