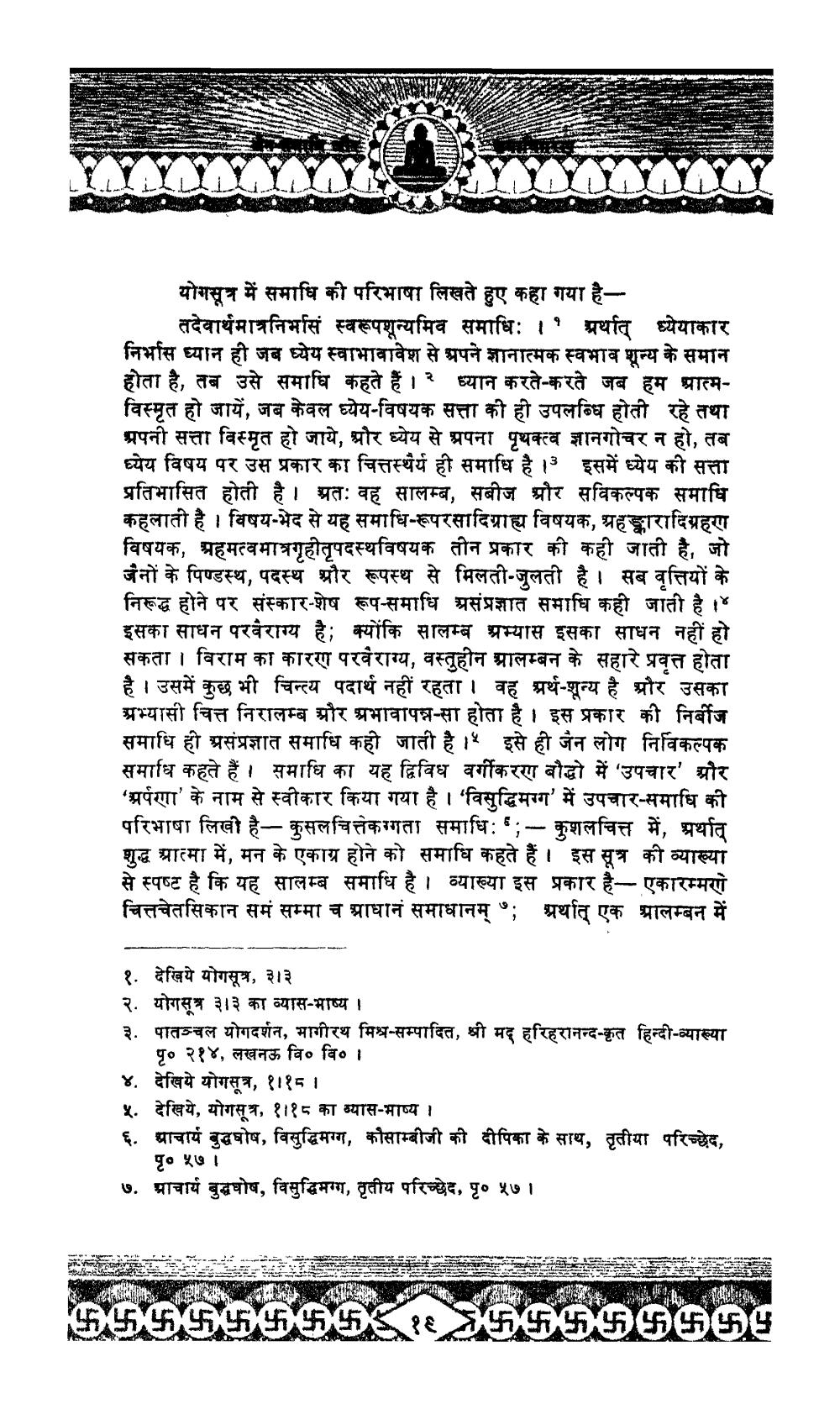________________
योगसूत्र में समाधि की परिभाषा लिखते हुए कहा गया है
तदेवार्थमात्रनिर्मासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः । श्रर्थात् ध्येयाकार निर्भास ध्यान ही जब ध्येय स्वाभावावेश से अपने ज्ञानात्मक स्वभाव शून्य के समान होता है, तब उसे समाधि कहते हैं । २ ध्यान करते-करते जब हम श्रात्मविस्मृत हो जायें, जब केवल ध्येय-विषयक सत्ता की ही उपलब्धि होती रहे तथा अपनी सत्ता विस्मृत हो जाये, श्रौर ध्येय से अपना पृथक्त्व ज्ञानगोचर न हो, तब ध्येय विषय पर उस प्रकार का चित्तस्थैर्य ही समाधि है । इसमें ध्येय की सत्ता प्रतिभासित होती है । अतः वह सालम्ब, सबीज और सविकल्पक समाधि कहलाती है । विषय-भेद से यह समाधि-रूपरसादिग्राह्य विषयक, ग्रहङ्कारादिग्रहरण विषयक, अहमत्वमात्रगृहीतृपदस्थविषयक तीन प्रकार की कही जाती है, जो जैनों के पिण्डस्थ, पदस्थ और रूपस्थ से मिलती-जुलती है। सब वृत्तियों के निरूद्ध होने पर संस्कार- शेष रूप-समाधि प्रसंप्रज्ञात समाधि कही जाती है । ४ इसका साधन परवैराग्य है; क्योंकि सालम्ब अभ्यास इसका साधन नहीं हो सकता । विराम का कारण परवैराग्य, वस्तुहीन प्रालम्बन के सहारे प्रवृत्त होता है । उसमें कुछ भी चिन्त्य पदार्थ नहीं रहता । वह अर्थ शून्य है और उसका अभ्यासी चित्त निरालम्ब और अभावापन्न-सा होता है। इस प्रकार की निर्बीज समाधि ही प्रसंप्रज्ञात समाधि कही जाती है। इसे ही जैन लोग निर्विकल्पक समाधि कहते हैं । समाधि का यह द्विविध वर्गीकरण बौद्धो में 'उपचार' और 'अर्पणा' के नाम से स्वीकार किया गया है । 'विसुद्धिमग्ग' में उपचार- समाधि की परिभाषा लिखी है - कुसल चित्तेकग्गता समाधि: : - कुशलचित्त में, अर्थात् शुद्ध आत्मा में, मन के एकाग्र होने को समाधि कहते हैं । इस सूत्र की व्याख्या स्पष्ट है कि यह सालम्ब समाधि है । व्याख्या इस प्रकार है- एकारम्भणे चित्तचेतसिकान समं सम्मा च प्रधानं समाधानम् ; अर्थात् एक श्रालम्बन में
१. देखिये योगसूत्र, ३।३
२. योगसूत्र ३ । ३ का व्यास भाष्य ।
३. पातञ्चल योगदर्शन, भागीरथ मिश्र सम्पादित, श्री मद् हरिहरानन्द- कृत हिन्दी व्याख्या पृ० २१४, लखनऊ वि० वि० ।
४. देखिये योगसूत्र, १1१८ ।
५. देखिये, योगसूत्र, ११८ का व्यास भाष्य ।
६. आचार्य बुद्धघोष, विसुद्धिमग्ग, कोसाम्बीजी की दीपिका के साथ, तृतीया परिच्छेद,
पृ० ५७ ।
७. प्राचार्य बुद्धघोष, विसुद्धिमग्ग, तृतीय परिच्छेद, पृ० ५७ ।
55555555555555559