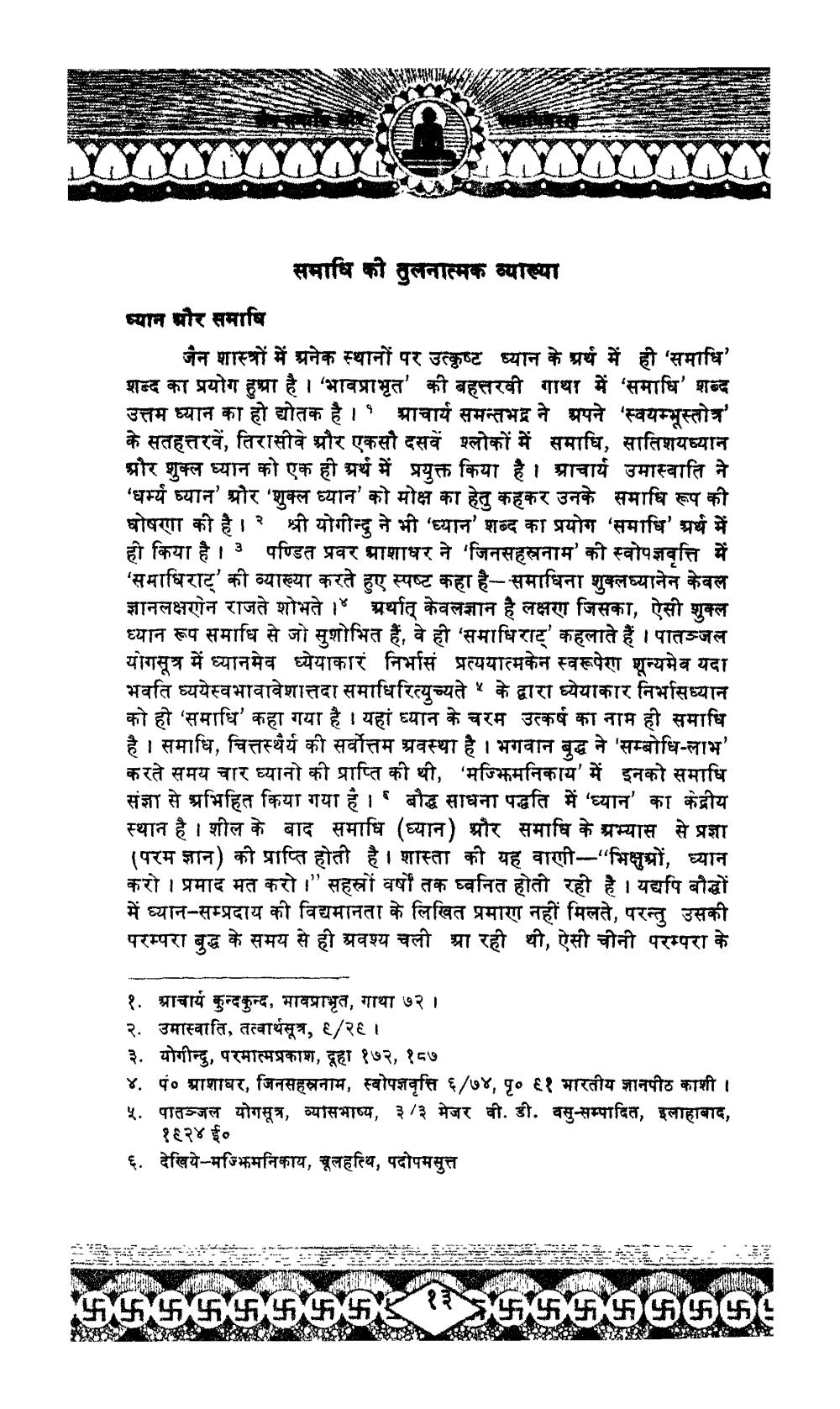________________
समाधि की तुलनात्मक व्याख्या
ध्यान और समाधि
जैन शास्त्रों में अनेक स्थानों पर उत्कृष्ट ध्यान के अर्थ में ही 'समाधि' शब्द का प्रयोग हुआ है । 'भावप्राभृत' की बहत्तरवी गाथा में 'समाधि' शब्द उत्तम ध्यान का हो द्योतक है । १ प्राचार्य समन्तभद्र ने अपने 'स्वयम्भूस्तोत्र' के सतहत्तरवें, तिरासीवे और एकसौ दसवें श्लोकों में समाधि, सातिशयध्यान और शुक्ल ध्यान को एक ही अर्थ में प्रयुक्त किया है । प्राचार्य उमास्वाति ने 'धर्म्य ध्यान' और 'शुक्ल ध्यान' को मोक्ष का हेतु कहकर उनके समाधि रूप की घोषणा की है । २ 1 श्री योगीन्दु ने भी 'ध्यान' शब्द का प्रयोग 'समाधि' अर्थ में ही किया है । पण्डित प्रवर प्राशावर ने 'जिनसहस्रनाम' की स्वोपज्ञवृत्ति में 'समाधिराट्' की व्याख्या करते हुए स्पष्ट कहा है- समाधिना शुक्लध्यानेन केवल ज्ञानलक्षणेन राजते शोभते । अर्थात् केवलज्ञान है लक्षरण जिसका, ऐसी शुक्ल ध्यान रूप समाधि से जो सुशोभित हैं, वे ही 'समाधिराट्' कहलाते हैं । पातञ्जल योगसूत्र में ध्यानमेव ध्येयाकारं निर्भासं प्रत्ययात्मकेन स्वरूपेण शून्यमेव यदा भवति ध्ययेस्वभावावेशात्तदा समाधिरित्युच्यते ५ के द्वारा ध्येयाकार निर्भासध्यान को हो 'समाधि' कहा गया है। यहां ध्यान के चरम उत्कर्ष का नाम ही समाधि है । समाधि, चित्तस्थैर्य की सर्वोत्तम अवस्था है । भगवान बुद्ध ने 'सम्बोधि-लाभ' करते समय चार ध्यानो की प्राप्ति की थी, 'मज्झिमनिकाय' में इनको समाधि संज्ञा से अभिहित किया गया है । बौद्ध साधना पद्धति में 'ध्यान' का केंद्रीय स्थान है । शील के बाद समाधि ( ध्यान ) और समाधि के अभ्यास से प्रज्ञा (परम ज्ञान ) की प्राप्ति होती है। शास्ता की यह वाणी - “भिक्षुत्रों, ध्यान करो । प्रमाद मत करो।" सहस्रों वर्षों तक ध्वनित होती रही है । यद्यपि बौद्धों
ध्यान - सम्प्रदाय की विद्यमानता के लिखित प्रमाण नहीं मिलते, परन्तु उसकी परम्परा बुद्ध के समय से ही अवश्य चली आ रही थी, ऐसी चीनी परम्परा के
१. आचार्य कुन्दकुन्द, भावप्राभृत, गाथा ७२ ।
२. उमास्वाति, तत्वार्थसूत्र, ६ / २६ ।
३. योगीन्दु, परमात्मप्रकाश, दूहा १७२, १८७
४. पं० प्रशाघर, जिनसहस्रनाम, स्वोपज्ञवृत्ति ६ / ७४, पृ० ६१ भारतीय ज्ञानपीठ काशी । ५. पातञ्जल योगसूत्र, व्यासभाष्य, ३ / ३ मेजर वी. डी. वसु-सम्पादित, इलाहाबाद, १६२४ ई०
६. देखिये - मज्झिमनिकाय, चूलहत्थि, पदोपमसुत्त
5555555555$$$$!