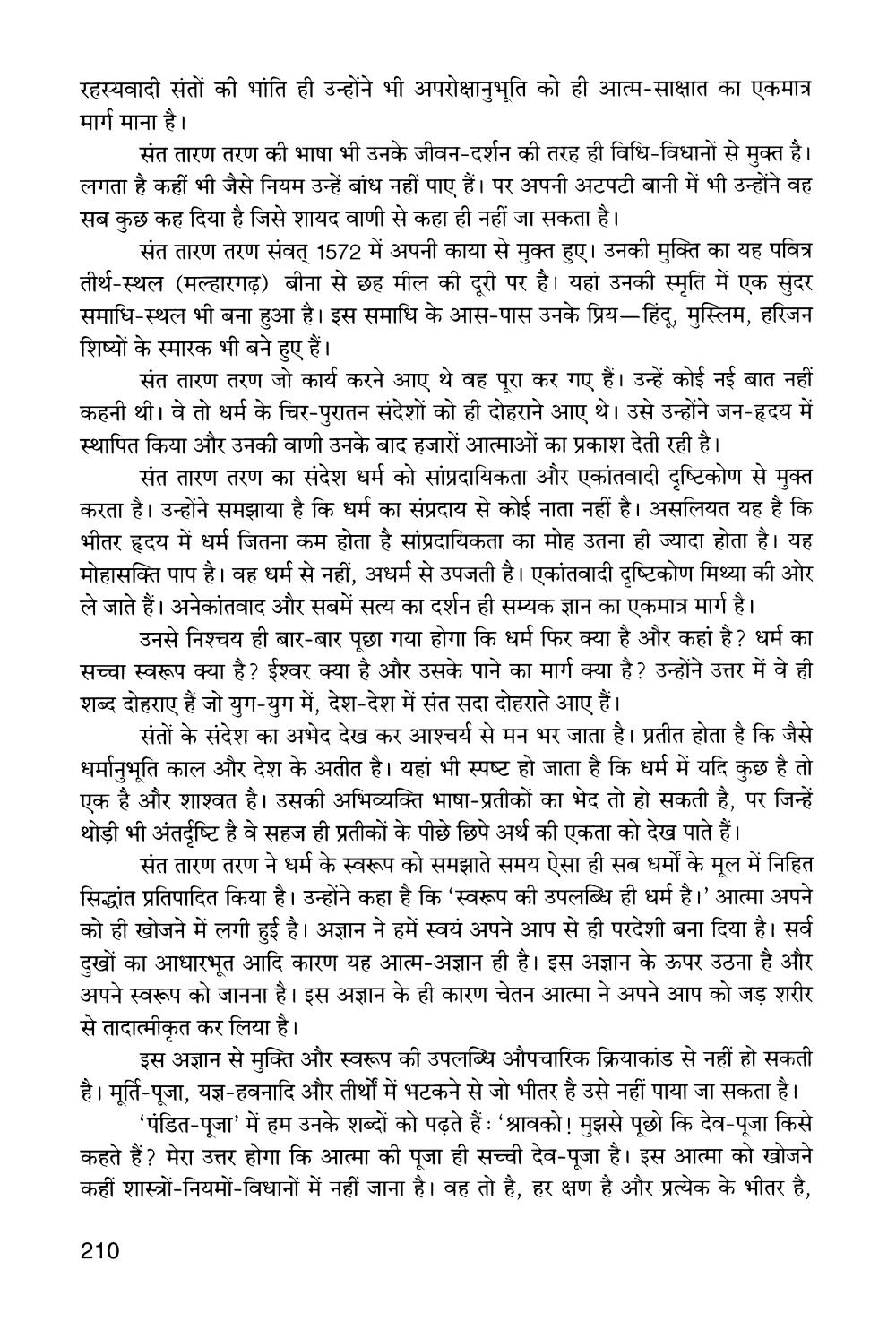________________
रहस्यवादी संतों की भांति ही उन्होंने भी अपरोक्षानुभूति को ही आत्म-साक्षात का एकमात्र मार्ग माना है।
संत तारण तरण की भाषा भी उनके जीवन-दर्शन की तरह ही विधि-विधानों से मुक्त है। लगता है कहीं भी जैसे नियम उन्हें बांध नहीं पाए हैं। पर अपनी अटपटी बानी में भी उन्होंने वह सब कुछ कह दिया है जिसे शायद वाणी से कहा ही नहीं जा सकता है।
संत तारण तरण संवत 1572 में अपनी काया से मक्त हए। उनकी मक्ति का यह पवित्र तीर्थ-स्थल (मल्हारगढ़) बीना से छह मील की दूरी पर है। यहां उनकी स्मृति में एक सुंदर समाधि-स्थल भी बना हुआ है। इस समाधि के आस-पास उनके प्रिय-हिंदू, मुस्लिम, हरिजन शिष्यों के स्मारक भी बने हुए हैं।
संत तारण तरण जो कार्य करने आए थे वह पूरा कर गए हैं। उन्हें कोई नई बात नहीं कहनी थी। वे तो धर्म के चिर-पुरातन संदेशों को ही दोहराने आए थे। उसे उन्होंने जन-हृदय में स्थापित किया और उनकी वाणी उनके बाद हजारों आत्माओं का प्रकाश देती रही है।
संत तारण तरण का संदेश धर्म को सांप्रदायिकता और एकांतवादी दृष्टिकोण से मुक्त करता है। उन्होंने समझाया है कि धर्म का संप्रदाय से कोई नाता नहीं है। असलियत यह है कि भीतर हृदय में धर्म जितना कम होता है सांप्रदायिकता का मोह उतना ही ज्यादा होता है। यह मोहासक्ति पाप है। वह धर्म से नहीं, अधर्म से उपजती है। एकांतवादी दृष्टिकोण मिथ्या की ओर ले जाते हैं। अनेकांतवाद और सबमें सत्य का दर्शन ही सम्यक ज्ञान का एकमात्र मार्ग है।।
उनसे निश्चय ही बार-बार पूछा गया होगा कि धर्म फिर क्या है और कहां है? धर्म का सच्चा स्वरूप क्या है? ईश्वर क्या है और उसके पाने का मार्ग क्या है? उन्होंने उत्तर में वे ही शब्द दोहराए हैं जो युग-युग में, देश-देश में संत सदा दोहराते आए हैं।
संतों के संदेश का अभेद देख कर आश्चर्य से मन भर जाता है। प्रतीत होता है कि जैसे धर्मानुभूति काल और देश के अतीत है। यहां भी स्पष्ट हो जाता है कि धर्म में यदि कुछ है तो एक है और शाश्वत है। उसकी अभिव्यक्ति भाषा-प्रतीकों का भेद तो हो सकती है, पर जिन्हें थोड़ी भी अंतर्दृष्टि है वे सहज ही प्रतीकों के पीछे छिपे अर्थ की एकता को देख पाते हैं।
संत तारण तरण ने धर्म के स्वरूप को समझाते समय ऐसा ही सब धर्मों के मूल में निहित सिद्धांत प्रतिपादित किया है। उन्होंने कहा है कि 'स्वरूप की उपलब्धि ही धर्म है।' आत्मा अपने को ही खोजने में लगी हुई है। अज्ञान ने हमें स्वयं अपने आप से ही परदेशी बना दिया है। सर्व दुखों का आधारभूत आदि कारण यह आत्म-अज्ञान ही है। इस अज्ञान के ऊपर उठना है और अपने स्वरूप को जानना है। इस अज्ञान के ही कारण चेतन आत्मा ने अपने आप को जड़ शरीर से तादात्मीकृत कर लिया है।
इस अज्ञान से मुक्ति और स्वरूप की उपलब्धि औपचारिक क्रियाकांड से नहीं हो सकती है। मूर्ति-पूजा, यज्ञ-हवनादि और तीर्थों में भटकने से जो भीतर है उसे नहीं पाया जा सकता है।
'पंडित-पूजा' में हम उनके शब्दों को पढ़ते हैं : 'श्रावको! मुझसे पूछो कि देव-पूजा किसे कहते हैं? मेरा उत्तर होगा कि आत्मा की पूजा ही सच्ची देव-पूजा है। इस आत्मा को खोजने कहीं शास्त्रों-नियमों-विधानों में नहीं जाना है। वह तो है, हर क्षण है और प्रत्येक के भीतर है,
210