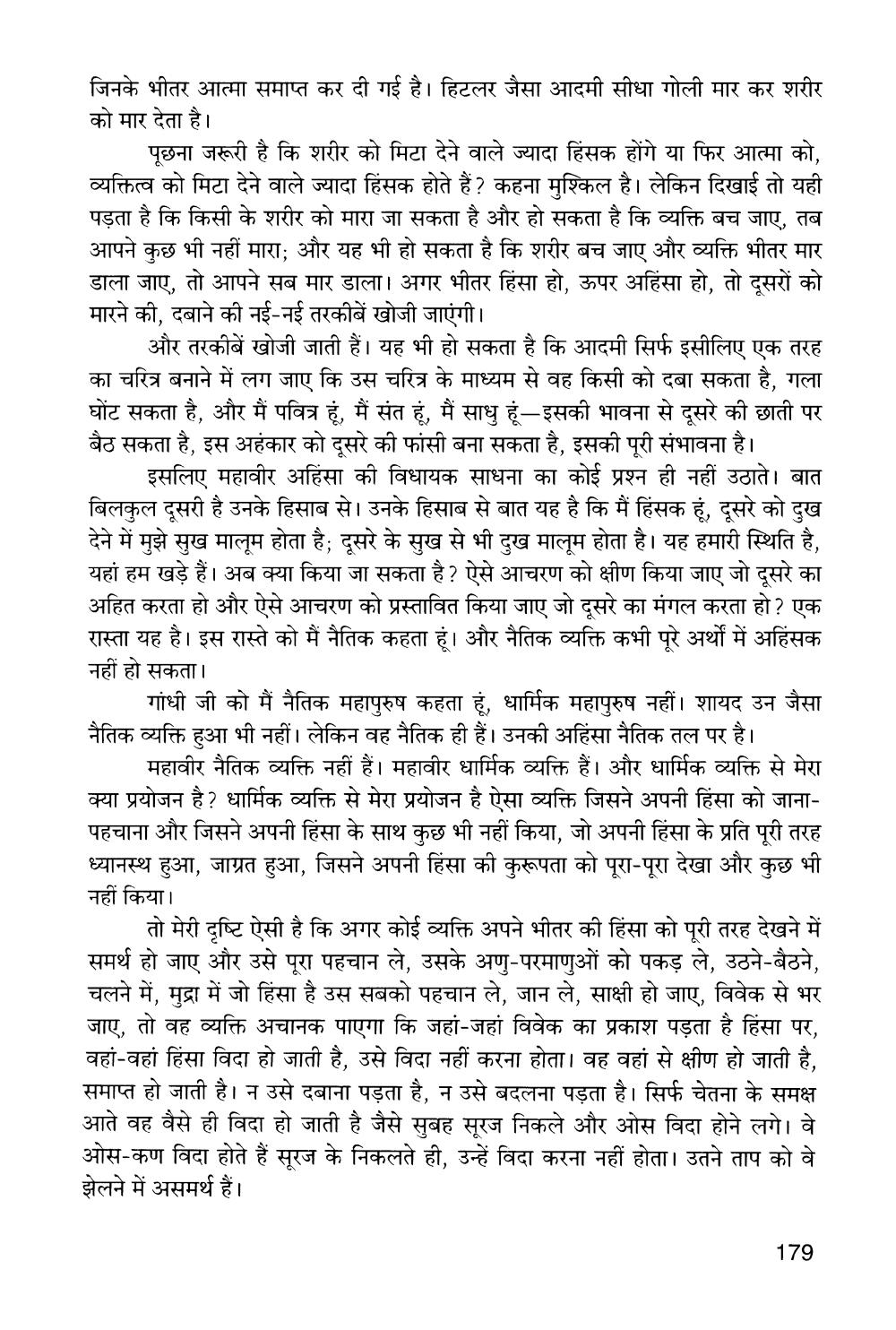________________
जिनके भीतर आत्मा समाप्त कर दी गई है। हिटलर जैसा आदमी सीधा गोली मार कर शरीर को मार देता है।
पूछना जरूरी है कि शरीर को मिटा देने वाले ज्यादा हिंसक होंगे या फिर आत्मा को, व्यक्तित्व को मिटा देने वाले ज्यादा हिंसक होते हैं? कहना मुश्किल है। लेकिन दिखाई तो यही पड़ता है कि किसी के शरीर को मारा जा सकता है और हो सकता है कि व्यक्ति बच जाए, तब आपने कुछ भी नहीं मारा; और यह भी हो सकता है कि शरीर बच जाए और व्यक्ति भीतर मार डाला जाए, तो आपने सब मार डाला। अगर भीतर हिंसा हो, ऊपर अहिंसा हो, तो दूसरों को मारने की, दबाने की नई-नई तरकीबें खोजी जाएंगी।
और तरकीबें खोजी जाती हैं। यह भी हो सकता है कि आदमी सिर्फ इसीलिए एक तरह का चरित्र बनाने में लग जाए कि उस चरित्र के माध्यम से वह किसी को दबा सकता है, गला घोंट सकता है, और मैं पवित्र हूं, मैं संत हूं, मैं साधु हूं-इसकी भावना से दूसरे की छाती पर बैठ सकता है, इस अहंकार को दूसरे की फांसी बना सकता है, इसकी पूरी संभावना है।
इसलिए महावीर अहिंसा की विधायक साधना का कोई प्रश्न ही नहीं उठाते। बात बिलकुल दूसरी है उनके हिसाब से। उनके हिसाब से बात यह है कि मैं हिंसक हूं, दूसरे को दुख देने में मुझे सुख मालूम होता है; दूसरे के सुख से भी दुख मालूम होता है। यह हमारी स्थिति है, यहां हम खड़े हैं। अब क्या किया जा सकता है? ऐसे आचरण को क्षीण किया जाए जो दूसरे का अहित करता हो और ऐसे आचरण को प्रस्तावित किया जाए जो दूसरे का मंगल करता हो? एक रास्ता यह है। इस रास्ते को मैं नैतिक कहता हूं। और नैतिक व्यक्ति कभी पूरे अर्थों में अहिंसक नहीं हो सकता।
गांधी जी को मैं नैतिक महापुरुष कहता हूं, धार्मिक महापुरुष नहीं। शायद उन जैसा नैतिक व्यक्ति हुआ भी नहीं। लेकिन वह नैतिक ही हैं। उनकी अहिंसा नैतिक तल पर है।
महावीर नैतिक व्यक्ति नहीं हैं। महावीर धार्मिक व्यक्ति हैं। और धार्मिक व्यक्ति से मेरा क्या प्रयोजन है? धार्मिक व्यक्ति से मेरा प्रयोजन है ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी हिंसा को जानापहचाना और जिसने अपनी हिंसा के साथ कुछ भी नहीं किया, जो अपनी हिंसा के प्रति पूरी तरह ध्यानस्थ हुआ, जाग्रत हुआ, जिसने अपनी हिंसा की कुरूपता को पूरा-पूरा देखा और कुछ भी नहीं किया।
तो मेरी दृष्टि ऐसी है कि अगर कोई व्यक्ति अपने भीतर की हिंसा को पूरी तरह देखने में समर्थ हो जाए और उसे पूरा पहचान ले, उसके अणु-परमाणुओं को पकड़ ले, उठने-बैठने, चलने में, मुद्रा में जो हिंसा है उस सबको पहचान ले, जान ले, साक्षी हो जाए, विवेक से भर जाए, तो वह व्यक्ति अचानक पाएगा कि जहां-जहां विवेक का प्रकाश पड़ता है हिंसा पर, वहां-वहां हिंसा विदा हो जाती है, उसे विदा नहीं करना होता। वह वहां से क्षीण हो जाती है, समाप्त हो जाती है। न उसे दबाना पड़ता है, न उसे बदलना पड़ता है। सिर्फ चेतना के समक्ष आते वह वैसे ही विदा हो जाती है जैसे सुबह सूरज निकले और ओस विदा होने लगे। वे ओस-कण विदा होते हैं सूरज के निकलते ही, उन्हें विदा करना नहीं होता। उतने ताप को वे झेलने में असमर्थ हैं।
179