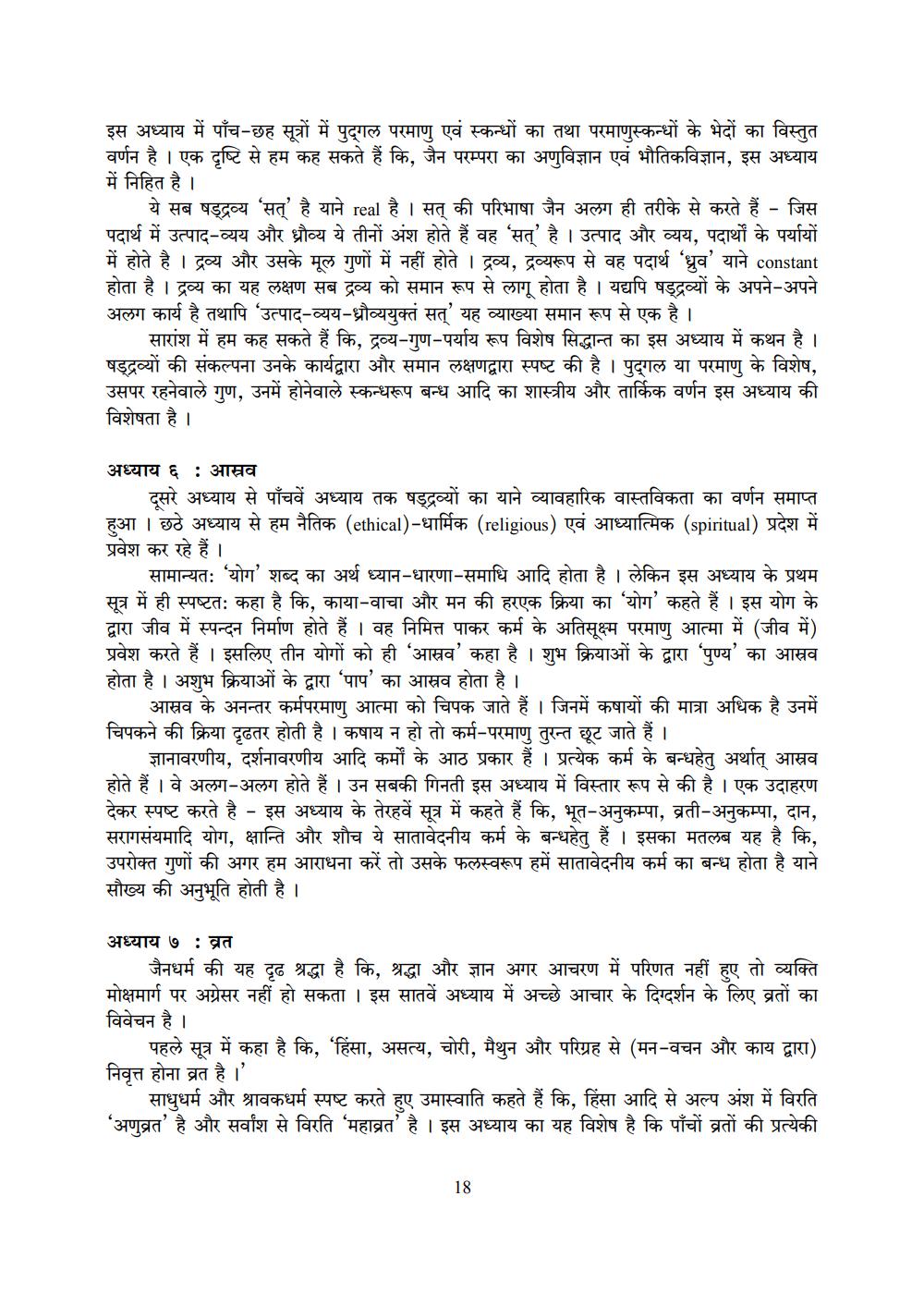________________
इस अध्याय में पाँच-छह सूत्रों में पुद्गल परमाणु एवं स्कन्धों का तथा परमाणुस्कन्धों के भेदों का विस्तुत वर्णन है । एक दृष्टि से हम कह सकते हैं कि, जैन परम्परा का अणुविज्ञान एवं भौतिकविज्ञान, इस अध्याय में निहित है।
ये सब षड्द्रव्य 'सत्' है याने real है । सत् की परिभाषा जैन अलग ही तरीके से करते हैं - जिस पदार्थ में उत्पाद-व्यय और ध्रौव्य ये तीनों अंश होते हैं वह 'सत्' है । उत्पाद और व्यय, पदार्थों के पर्यायों में होते है । द्रव्य और उसके मूल गुणों में नहीं होते । द्रव्य, द्रव्यरूप से वह पदार्थ 'ध्रुव' याने constant होता है । द्रव्य का यह लक्षण सब द्रव्य को समान रूप से लागू होता है । यद्यपि षड्द्रव्यों के अपने-अपने अलग कार्य है तथापि 'उत्पाद-व्यय-ध्रौव्ययुक्तं सत्' यह व्याख्या समान रूप से एक है।
सारांश में हम कह सकते हैं कि, द्रव्य-गुण-पर्याय रूप विशेष सिद्धान्त का इस अध्याय में कथन है । षड्द्रव्यों की संकल्पना उनके कार्यद्वारा और समान लक्षणद्वारा स्पष्ट की है । पुद्गल या परमाणु के विशेष, उसपर रहनेवाले गुण, उनमें होनेवाले स्कन्धरूप बन्ध आदि का शास्त्रीय और तार्किक वर्णन इस अध्याय की विशेषता है।
अध्याय ६ : आस्रव
दुसरे अध्याय से पाँचवें अध्याय तक षड्द्रव्यों का याने व्यावहारिक वास्तविकता का वर्णन समाप्त हुआ । छठे अध्याय से हम नैतिक (ethical)-धार्मिक (religious) एवं आध्यात्मिक (spiritual) प्रदेश में प्रवेश कर रहे हैं।
सामान्यतः 'योग' शब्द का अर्थ ध्यान-धारणा-समाधि आदि होता है । लेकिन इस अध्याय के प्रथम सूत्र में ही स्पष्टत: कहा है कि, काया-वाचा और मन की हरएक क्रिया का 'योग' कहते हैं । इस योग के द्वारा जीव में स्पन्दन निर्माण होते हैं । वह निमित्त पाकर कर्म के अतिसूक्ष्म परमाणु आत्मा में (जीव में) प्रवेश करते हैं । इसलिए तीन योगों को ही ‘आस्रव' कहा है । शुभ क्रियाओं के द्वारा 'पुण्य' का आस्रव होता है । अशुभ क्रियाओं के द्वारा 'पाप' का आस्रव होता है।
आस्रव के अनन्तर कर्मपरमाणु आत्मा को चिपक जाते हैं। जिनमें कषायों की मात्रा अधिक है उनमें चिपकने की क्रिया दृढतर होती है । कषाय न हो तो कर्म-परमाणु तुरन्त छूट जाते हैं ।
ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय आदि कर्मों के आठ प्रकार हैं । प्रत्येक कर्म के बन्धहेतु अर्थात् आस्रव होते हैं । वे अलग-अलग होते हैं। उन सबकी गिनती इस अध्याय में विस्तार रूप से की है । एक उदाहरण देकर स्पष्ट करते है - इस अध्याय के तेरहवें सूत्र में कहते हैं कि, भूत-अनुकम्पा, व्रती-अनुकम्पा, दान, सरागसंयमादि योग, क्षान्ति और शौच ये सातावेदनीय कर्म के बन्धहेतु हैं । इसका मतलब यह है कि, उपरोक्त गुणों की अगर हम आराधना करें तो उसके फलस्वरूप हमें सातावेदनीय कर्म का बन्ध होता है याने सौख्य की अनुभूति होती है ।
अध्याय ७ : व्रत
जैनधर्म की यह दृढ श्रद्धा है कि, श्रद्धा और ज्ञान अगर आचरण में परिणत नहीं हुए तो व्यक्ति मोक्षमार्ग पर अग्रेसर नहीं हो सकता । इस सातवें अध्याय में अच्छे आचार के दिग्दर्शन के लिए व्रतों का विवेचन है।
पहले सूत्र में कहा है कि, 'हिंसा, असत्य, चोरी, मैथुन और परिग्रह से (मन-वचन और काय द्वारा) निवृत्त होना व्रत है।'
साधुधर्म और श्रावकधर्म स्पष्ट करते हुए उमास्वाति कहते हैं कि, हिंसा आदि से अल्प अंश में विरति 'अणुव्रत' है और सर्वांश से विरति 'महाव्रत' है । इस अध्याय का यह विशेष है कि पाँचों व्रतों की प्रत्येकी