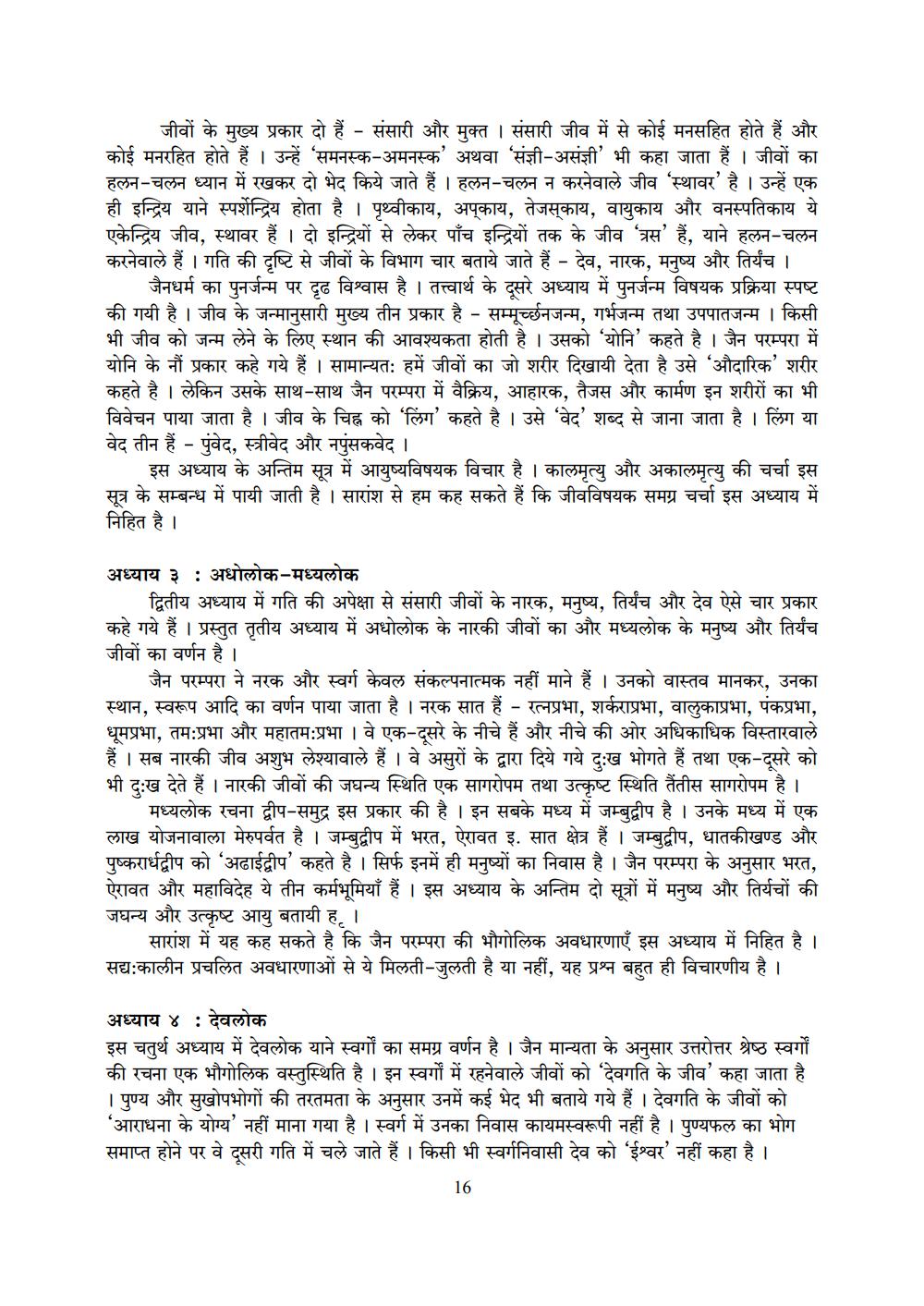________________
जीवों के मुख्य प्रकार दो हैं - संसारी और मुक्त । संसारी जीव में से कोई मनसहित होते हैं और कोई मनरहित होते हैं । उन्हें 'समनस्क-अमनस्क' अथवा 'संज्ञी-असंज्ञी' भी कहा जाता हैं । जीवों का हलन-चलन ध्यान में रखकर दो भेद किये जाते हैं । हलन-चलन न करनेवाले जीव 'स्थावर' है । उन्हें एक ही इन्द्रिय याने स्पर्शेन्द्रिय होता है । पृथ्वीकाय, अप्काय, तेजस्काय, वायुकाय और वनस्पतिकाय ये एकेन्द्रिय जीव, स्थावर हैं । दो इन्द्रियों से लेकर पाँच इन्द्रियों तक के जीव त्रस' हैं, याने हलन-चलन करनेवाले हैं । गति की दृष्टि से जीवों के विभाग चार बताये जाते हैं - देव, नारक, मनुष्य और तिर्यंच ।
जैनधर्म का पुनर्जन्म पर दृढ विश्वास है । तत्त्वार्थ के दूसरे अध्याय में पुनर्जन्म विषयक प्रक्रिया स्पष्ट की गयी है । जीव के जन्मानुसारी मुख्य तीन प्रकार है - सम्मूर्च्छनजन्म, गर्भजन्म तथा उपपातजन्म । किसी भी जीव को जन्म लेने के लिए स्थान की आवश्यकता होती है । उसको ‘योनि' कहते है । जैन परम्परा में योनि के नौं प्रकार कहे गये हैं । सामान्यत: हमें जीवों का जो शरीर दिखायी देता है उसे 'औदारिक' शरीर कहते है । लेकिन उसके साथ-साथ जैन परम्परा में वैक्रिय, आहारक, तैजस और कार्मण इन शरीरों का भी विवेचन पाया जाता है । जीव के चिह्न को 'लिंग' कहते है । उसे 'वेद' शब्द से जाना जाता है । लिंग या वेद तीन हैं - पुंवेद, स्त्रीवेद और नपुंसकवेद ।।
इस अध्याय के अन्तिम सूत्र में आयुष्यविषयक विचार है । कालमृत्यु और अकालमृत्यु की चर्चा इस सूत्र के सम्बन्ध में पायी जाती है । साराश से हम कह सकते है कि जीवविषयक समग्र चर्चा इस अध्याय में निहित है।
अध्याय ३ : अधोलोक-मध्यलोक
द्वितीय अध्याय में गति की अपेक्षा से संसारी जीवों के नारक, मनुष्य, तिर्यंच और देव ऐसे चार प्रकार कहे गये हैं। प्रस्तुत तृतीय अध्याय में अधोलोक के नारकी जीवों का और मध्यलोक के मनुष्य और तिर्यंच जीवों का वर्णन है।
जैन परम्परा ने नरक और स्वर्ग केवल संकल्पनात्मक नहीं माने हैं । उनको वास्तव मानकर, उनका स्थान, स्वरूप आदि का वर्णन पाया जाता है । नरक सात हैं - रत्नप्रभा, शर्कराप्रभा, वालुकाप्रभा, पंकप्रभा, धूमप्रभा, तम:प्रभा और महातम:प्रभा । वे एक-दूसरे के नीचे हैं और नीचे की ओर अधिकाधिक विस्तारवाले हैं । सब नारकी जीव अशुभ लेश्यावाले हैं । वे असुरों के द्वारा दिये गये दुःख भोगते हैं तथा एक-दूसरे को भी दुःख देते हैं । नारकी जीवों की जघन्य स्थिति एक सागरोपम तथा उत्कृष्ट स्थिति तैंतीस सागरोपम है।
मध्यलोक रचना द्वीप-समुद्र इस प्रकार की है । इन सबके मध्य में जम्बुद्वीप है । उनके मध्य में एक लाख योजनावाला मेरुपर्वत है । जम्बुद्वीप में भरत, ऐरावत इ. सात क्षेत्र हैं । जम्बुद्वीप, धातकीखण्ड और पुष्करार्धद्वीप को 'अढाईद्वीप' कहते है । सिर्फ इनमें ही मनुष्यों का निवास है । जैन परम्परा के अनुसार भरत, ऐरावत और महाविदेह ये तीन कर्मभूमियाँ हैं । इस अध्याय के अन्तिम दो सूत्रों में मनुष्य और तिर्यचों की जघन्य और उत्कृष्ट आय बतायी ह।
सारांश में यह कह सकते है कि जैन परम्परा की भौगोलिक अवधारणाएँ इस अध्याय में निहित है। सद्य:कालीन प्रचलित अवधारणाओं से ये मिलती-जुलती है या नहीं, यह प्रश्न बहुत ही विचारणीय है।
अध्याय ४ : देवलोक इस चतुर्थ अध्याय में देवलोक याने स्वर्गों का समग्र वर्णन है । जैन मान्यता के अनुसार उत्तरोत्तर श्रेष्ठ स्वर्गों की रचना एक भौगोलिक वस्तुस्थिति है । इन स्वर्गों में रहनेवाले जीवों को 'देवगति के जीव' कहा जाता है । पुण्य और सुखोपभोगों की तरतमता के अनुसार उनमें कई भेद भी बताये गये हैं । देवगति के जीवों को 'आराधना के योग्य' नहीं माना गया है । स्वर्ग में उनका निवास कायमस्वरूपी नहीं है । पुण्यफल का भोग समाप्त होने पर वे दुसरी गति में चले जाते हैं । किसी भी स्वर्गनिवासी देव को 'ईश्वर' नहीं कहा है ।
16