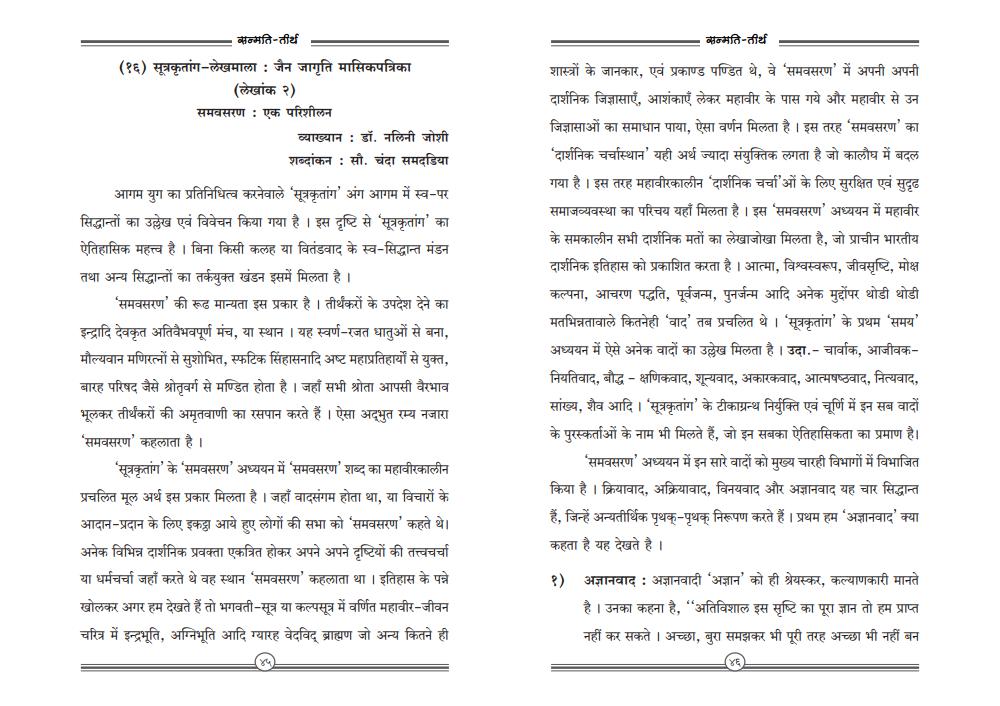________________
सन्मति-तीर्थ
(१६) सूत्रकृतांग - लेखमाला : जैन जागृति मासिकपत्रिका
(लेखांक २)
समवसरण एक परिशीलन
व्याख्यान : डॉ. नलिनी जोशी शब्दांकन : सौ. चंदा समदडिया
आगम युग का प्रतिनिधित्व करनेवाले 'सूत्रकृतांग' अंग आगम में स्व-पर सिद्धान्तों का उल्लेख एवं विवेचन किया गया है। इस दृष्टि से 'सूत्रकृतांग' का ऐतिहासिक महत्त्व है । बिना किसी कलह या वितंडवाद के स्व-सिद्धान्त मंडन तथा अन्य सिद्धान्तों का तर्कयुक्त खंडन इसमें मिलता है।
'समवसरण' की रूढ मान्यता इस प्रकार है। तीर्थंकरों के उपदेश देने का इन्द्रादि देवकृत अतिवैभवपूर्ण मंच, या स्थान । यह स्वर्ण-रजत धातुओं से बना, मौल्यवान मणिरत्नों से सुशोभित, स्फटिक सिंहासनादि अष्ट महाप्रतिहार्यों से युक्त, बारह परिषद जैसे श्रोतृवर्ग से मण्डित होता है। जहाँ सभी श्रोता आपसी वैरभाव भूलकर तीर्थंकरों की अमृतवाणी का रसपान करते हैं। ऐसा अद्भुत रम्य नजारा 'समवसरण' कहलाता है।
'सूत्रकृतांग' के 'समवसरण' अध्ययन में 'समवसरण' शब्द का महावीरकालीन प्रचलित अर्थ इस प्रकार मिलता है। जहाँ वादसंगम होता था, या विचारों के मूल आदान-प्रदान के लिए इकट्ठा आये हुए लोगों की सभा को 'समवसरण' कहते थे। अनेक विभिन्न दार्शनिक प्रवक्ता एकत्रित होकर अपने अपने दृष्टियों की तत्त्वचर्चा या धर्मचर्चा जहाँ करते थे वह स्थान 'समवसरण' कहलाता था । इतिहास के पन्ने खोलकर अगर हम देखते हैं तो भगवती सूत्र या कल्पसूत्र में वर्णित महावीर जीवन चरित्र में इन्द्रभूति, अग्निभूति आदि ग्यारह वेदविद् ब्राह्मण जो अन्य कितने ही
सन्मति - तीर्थ
शास्त्रों के जानकार एवं प्रकाण्ड पण्डित थे, वे 'समवसरण' में अपनी अपनी दार्शनिक जिज्ञासाएँ, आशंकाएँ लेकर महावीर के पास गये और महावीर से उन जिज्ञासाओं का समाधान पाया, ऐसा वर्णन मिलता है। इस तरह 'समवसरण' का 'दार्शनिक चर्चास्थान' यही अर्थ ज्यादा संयुक्तिक लगता है जो कालौघ में बदल गया है। इस तरह महावीरकालीन 'दार्शनिक चर्चा'ओं के लिए सुरक्षित एवं सुदृढ समाजव्यवस्था का परिचय यहाँ मिलता है। इस 'समवसरण' अध्ययन में महावीर के समकालीन सभी दार्शनिक मतों का लेखाजोखा मिलता है, जो प्राचीन भारतीय दार्शनिक इतिहास को प्रकाशित करता है। आत्मा, विश्वस्वरूप, जीवसृष्टि, मोक्ष कल्पना, आचरण पद्धति, पूर्वजन्म, पुनर्जन्म आदि अनेक मुद्दोंपर थोडी थोडी मतभिन्नतावाले कितनेही 'वाद' तब प्रचलित थे । 'सूत्रकृतांग' के प्रथम 'समय' अध्ययन में ऐसे अनेक वादों का उल्लेख मिलता है । उदा. चार्वाक, आजीवकनियतिवाद, बौद्ध क्षणिकवाद, शून्यवाद, अकारकवाद, आत्मषष्ठवाद, नित्यवाद, सांख्य, शैव आदि। ‘सूत्रकृतांग' के टीकाग्रन्थ निर्युक्ति एवं चूर्णि में इन सब वादों के पुरस्कर्ताओं के नाम भी मिलते हैं, जो इन सबका ऐतिहासिकता का प्रमाण है।
'समवसरण' अध्ययन में इन सारे वादों को मुख्य चारही विभागों में विभाजित किया है । क्रियावाद, अक्रियावाद, विनयवाद और अज्ञानवाद यह चार सिद्धान्त हैं, जिन्हें अन्यतीर्थिक पृथक्-पृथक् निरूपण करते हैं। प्रथम हम 'अज्ञानवाद' क्या कहता है यह देखते है ।
१)
अज्ञानवाद अज्ञानवादी 'अज्ञान' को ही श्रेयस्कर, कल्याणकारी मानते है। उनका कहना है, “अतिविशाल इस सृष्टि का पूरा ज्ञान तो हम प्राप्त नहीं कर सकते। अच्छा, बुरा समझकर भी पूरी तरह अच्छा भी नहीं बन
४६