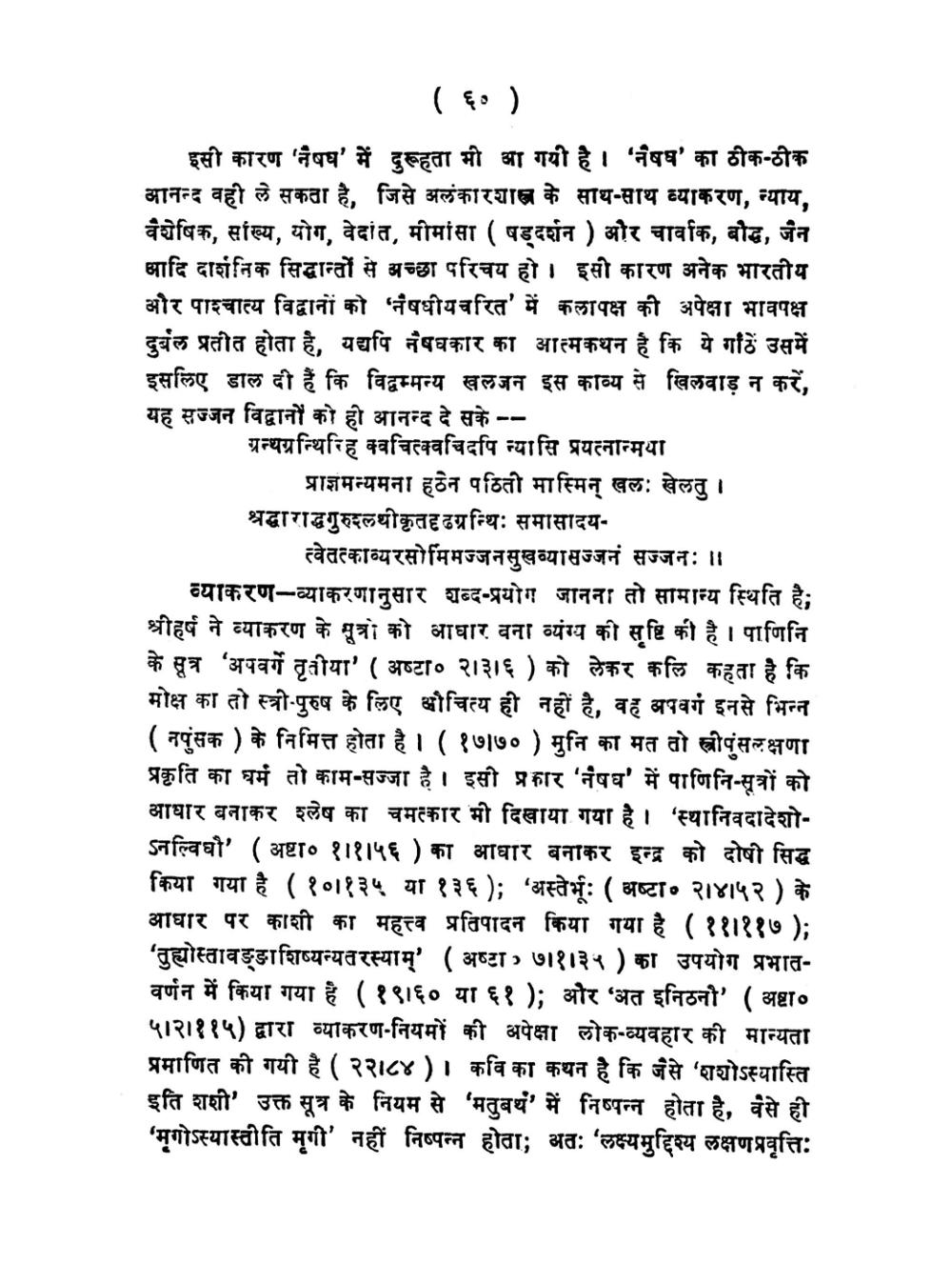________________
( ६. ) इसी कारण 'नैषध' में दुरूहता भी आ गयी है । 'नैषध' का ठीक-ठीक आनन्द वही ले सकता है, जिसे अलंकारशास्त्र के साथ-साथ व्याकरण, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, वेदांत, मीमांसा ( षड्दर्शन ) और चार्वाक, बौद्ध, जैन आदि दार्शनिक सिद्धान्तों से अच्छा परिचय हो। इसी कारण अनेक भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों को 'नैषधीयचरित' में कलापक्ष की अपेक्षा भावपक्ष दुर्बल प्रतीत होता है, यद्यपि नैषधकार का आत्मकथन है कि ये गाँठे उसमें इसलिए डाल दी हैं कि विद्वम्मन्य खलजन इस काव्य से खिलवाड़ न करें, यह सज्जन विद्वानों को ही आनन्द दे सके --
ग्रन्थग्रन्थिन्हि क्वचित्क्वचिदपि न्यासि प्रयत्नान्मया
प्राज्ञमन्यमना हठेन पठिती मास्मिन् खल: खेलतु । श्रद्धाराद्धगुरुदलथीकृत ढग्रन्थिः समासादय
त्वेतत्काव्यरसोनिमज्जनसुखव्यासज्जनं सज्जनः ।। व्याकरण-व्याकरणानुसार शब्द-प्रयोग जानना तो सामान्य स्थिति है; श्रीहर्ष ने व्याकरण के सूत्रों को आधार बना व्यंग्य की सृष्टि की है । पाणिनि के सूत्र 'अपवर्गे तृतीया' ( अष्टा० २।३।६ ) को लेकर कलि कहता है कि मोक्ष का तो स्त्री-पुरुष के लिए औचित्य ही नहीं है, वह अपवगं इनसे भिन्न ( नपुंसक ) के निमित्त होता है । ( १७७० ) मुनि का मत तो स्त्रीपुंसलक्षणा प्रकृति का धर्म तो काम-सज्जा है। इसी प्रकार 'नषध' में पाणिनि-सूत्रों को आधार बनाकर श्लेष का चमत्कार भी दिखाया गया है। 'स्थानिवदादेशोऽनल्विधौ' ( अष्टा० ११११५६ ) का आधार बनाकर इन्द्र को दोषी सिद्ध किया गया है (१०।१३५ या १३६); 'अस्तेर्भूः ( अष्टा० २।४।५२ ) के आधार पर काशी का महत्त्व प्रतिपादन किया गया है ( १११११७ ); 'तुह्योस्तावडाशिष्यन्यतरस्याम्' ( अष्टा, ७१।३५ ) का उपयोग प्रभातवर्णन में किया गया है ( १९।६० या ६१ ); और 'अत इनिठनी' ( अष्टा० ५।२।११५) द्वारा व्याकरण-नियमों की अपेक्षा लोक-व्यवहार की मान्यता प्रमाणित की गयी है ( २२१८४)। कवि का कथन है कि जैसे 'शशोऽस्यास्ति इति शशी' उक्त सूत्र के नियम से 'मतुबर्थ' में निष्पन्न होता है, वैसे ही 'मृगोऽस्यास्तीति मृगी' नहीं निष्पन्न होता; अत: 'लक्ष्यमुद्दिश्य लक्षणप्रवृत्तिः