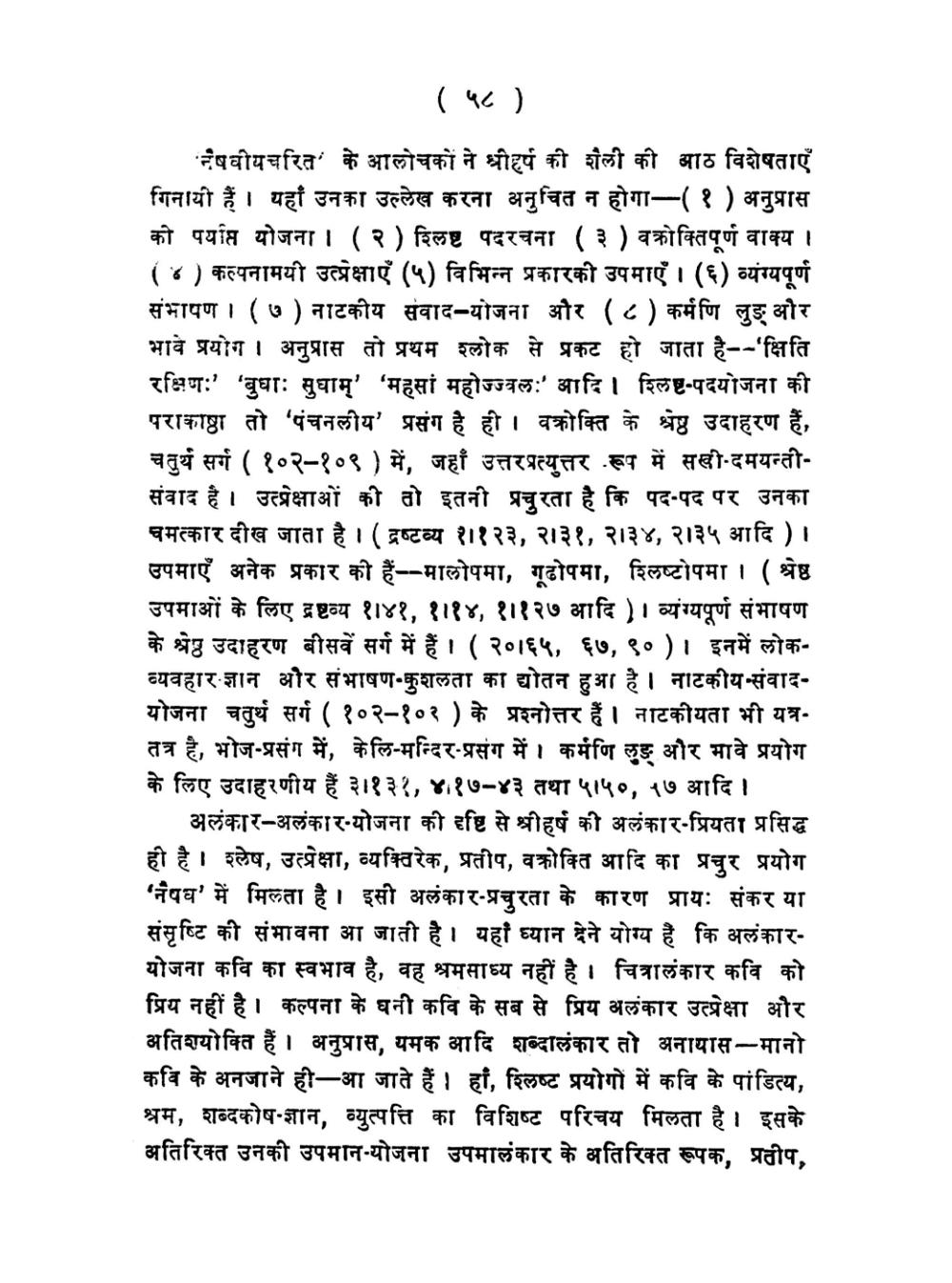________________
( ५८ ) 'नैषधीयचरित' के आलोचकों ने श्रीहर्ष की शैली की आठ विशेषताएँ गिनायी हैं। यहां उनका उल्लेख करना अनुचित न होगा-(१) अनुप्रास को पर्याप्त योजना । (२) शिलष्ट पदरचना ( ३ ) वक्रोक्तिपूर्ण वाक्य । ( ४ ) कल्पनामयी उत्प्रेक्षाएँ (५) विभिन्न प्रकारकी उपमाएँ । (६) व्यंग्यपूर्ण संभाषण । (७) नाटकीय संवाद-योजना और (८) कर्मणि लुङ् और भावे प्रयोग । अनुप्रास तो प्रथम श्लोक से प्रकट हो जाता है--'क्षिति रक्षिणः' 'बुधाः सुधाम्' 'महसां महोज्ज्वलः' आदि । श्लिष्ट-पदयोजना की पराकाष्ठा तो 'पंचनलीय' प्रसंग है ही। वक्रोक्ति के श्रेष्ठ उदाहरण हैं, चतुर्थ सर्ग ( १०२-१०९ ) में, जहाँ उत्तरप्रत्युत्तर रूप में सखी-दमयन्तीसंवाद है। उत्प्रेक्षाओं की तो इतनी प्रचुरता है कि पद-पद पर उनका चमत्कार दीख जाता है । ( द्रष्टव्य १११२३, २।३१, २।३४, २।३५ आदि )। उपमाएँ अनेक प्रकार की हैं--मालोपमा, गूढोपमा, श्लिष्टोपमा । ( श्रेष्ठ उपमाओं के लिए द्रष्टव्य २४१, १३१४, १११२७ आदि ) । व्यंग्यपूर्ण संभाषण के श्रेष्ठ उदाहरण बीसवें सर्ग में हैं । ( २०६५, ६७, ९० )। इनमें लोकव्यवहार ज्ञान और संभाषण-कुशलता का द्योतन हुआ है । नाटकीय-संवादयोजना चतुर्थ सर्ग ( १०२-१०२ ) के प्रश्नोत्तर हैं। नाटकीयता भी यत्रतत्र है, भोज-प्रसंग में, केलि-मन्दिर-प्रसंग में। कर्मणि लुङ्ग और मावे प्रयोग के लिए उदाहरणीय हैं ३।१३१, ४.१७-४३ तथा ५।५०, १७ आदि ।
अलंकार-अलंकार-योजना की दृष्टि से श्रीहर्ष की अलंकार-प्रियता प्रसिद्ध ही है। श्लेष, उत्प्रेक्षा, व्यक्तिरेक, प्रतीप, वक्रोक्ति आदि का प्रचुर प्रयोग 'नैषध' में मिलता है। इसी अलंकार-प्रचुरता के कारण प्रायः संकर या संसृष्टि की संभावना आ जाती है। यहां ध्यान देने योग्य है कि अलंकारयोजना कवि का स्वभाव है, वह श्रमसाध्य नहीं है। चित्रालंकार कवि को प्रिय नहीं है। कल्पना के घनी कवि के सब से प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति हैं। अनुप्रास, यमक आदि शब्दालंकार तो अनायास-मानो कवि के अनजाने ही-आ जाते हैं। हां, श्लिष्ट प्रयोगों में कवि के पांडित्य, श्रम, शब्दकोष-ज्ञान, व्युत्पत्ति का विशिष्ट परिचय मिलता है। इसके अतिरिक्त उनकी उपमान-योजना उपमालंकार के अतिरिक्त रूपक, प्रतीप,