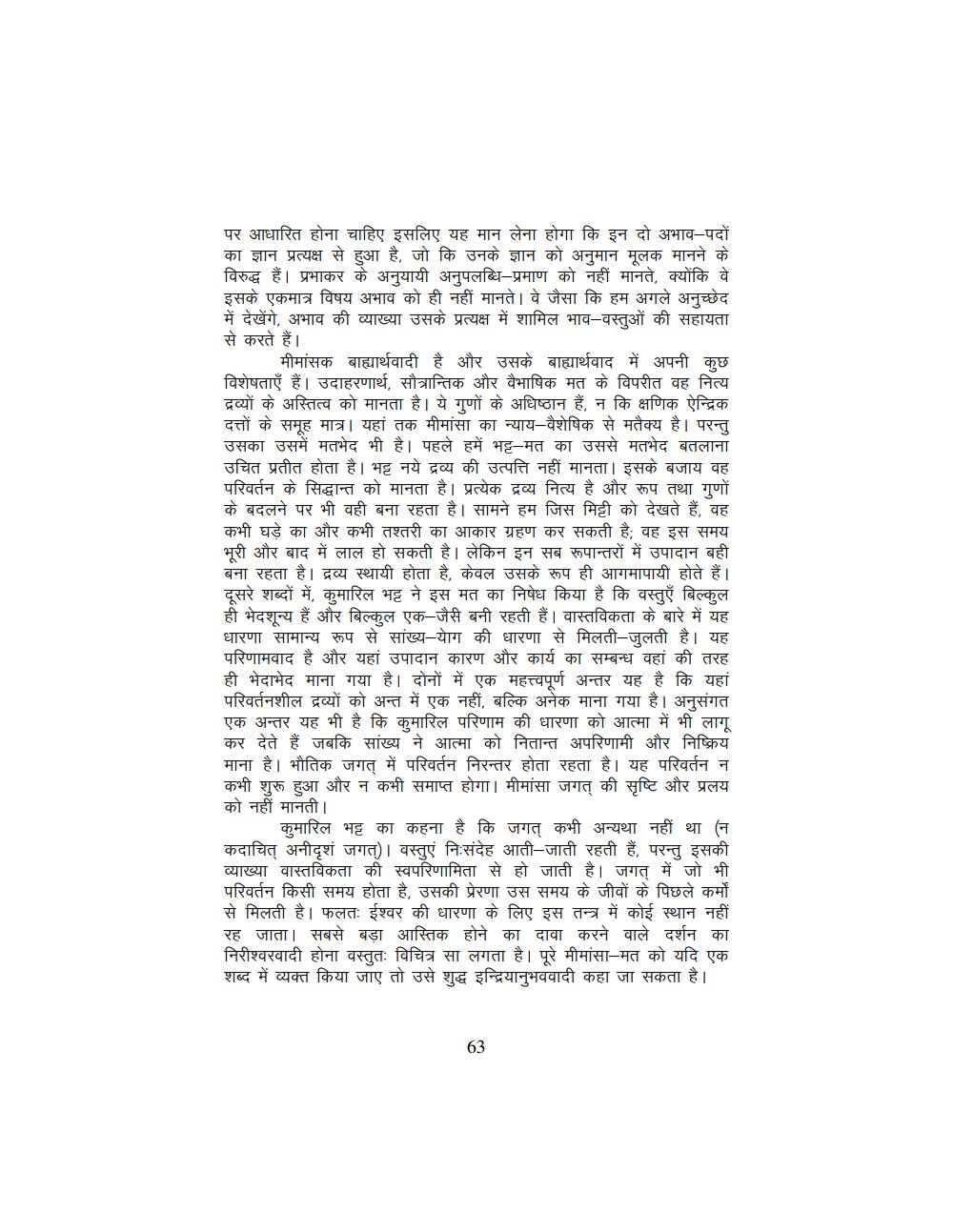________________
पर आधारित होना चाहिए इसलिए यह मान लेना होगा कि इन दो अभाव-पदों का ज्ञान प्रत्यक्ष से हुआ है, जो कि उनके ज्ञान को अनुमान मूलक मानने के विरुद्ध हैं। प्रभाकर के अनुयायी अनुपलब्धि-प्रमाण को नहीं मानते. क्योंकि वे इसके एकमात्र विषय अभाव को ही नहीं मानते। वे जैसा कि हम अगले अनुच्छेद में देखेंगे, अभाव की व्याख्या उसके प्रत्यक्ष में शामिल भाव-वस्तुओं की सहायता से करते हैं।
मीमांसक बाह्यार्थवादी है और उसके बाह्यार्थवाद में अपनी कुछ विशेषताएँ हैं। उदाहरणार्थ, सौत्रान्तिक और वैभाषिक मत के विपरीत वह नित्य द्रव्यों के अस्तित्व को मानता है। ये गुणों के अधिष्ठान हैं, न कि क्षणिक ऐन्द्रिक दत्तों के समूह मात्र। यहां तक मीमांसा का न्याय-वैशेषिक से मतैक्य है। परन्तु उसका उसमें मतभेद भी है। पहले हमें भट्ट-मत का उससे मतभेद बतलाना उचित प्रतीत होता है। भट्ट नये द्रव्य की उत्पत्ति नहीं मानता। इसके बजाय वह परिवर्तन के सिद्धान्त को मानता है। प्रत्येक द्रव्य नित्य है और रूप तथा गुणों के बदलने पर भी वही बना रहता है। सामने हम जिस मिट्टी को देखते हैं, वह कभी घडे का और कभी तश्तरी का आकार ग्रहण कर सकती है। वह इस समय भूरी और बाद में लाल हो सकती है। लेकिन इन सब रूपान्तरों में उपादान बही बना रहता है। द्रव्य स्थायी होता है, केवल उसके रूप ही आगमापायी होते हैं। दूसरे शब्दों में, कुमारिल भट्ट ने इस मत का निषेध किया है कि वस्तुएँ बिल्कुल ही भेदशून्य हैं और बिल्कुल एक-जैसे बनी रहती हैं। वास्तविकता के बारे में यह धारणा सामान्य रूप से सांख्य-योग की धारणा से मिलती-जुलती है। यह परिणामवाद है और यहां उपादान कारण और कार्य का सम्बन्ध वहां की तरह ही भेदाभेद माना गया है। दोनों में एक महत्त्वपूर्ण अन्तर यह है कि यहां परिवर्तनशील द्रव्यों को अन्त में एक नहीं, बल्कि अनेक माना गया है। अनुसंगत एक अन्तर यह भी है कि कमारिल परिणाम की धारणा को आत्मा में भी लाग कर देते हैं जबकि सांख्य ने आत्मा को नितान्त अपरिणामी और निष्क्रिय माना है। भौतिक जगत् में परिवर्तन निरन्तर होता रहता है। यह परिवर्तन न कभी शुरू हुआ और न कभी समाप्त होगा। मीमांसा जगत् की सृष्टि और प्रलय को नहीं मानती।
कुमारिल भट्ट का कहना है कि जगत् कभी अन्यथा नहीं था (न कदाचित् अनीदृशं जगत्)। वस्तुएं निःसंदेह आती-जाती रहती हैं, परन्तु इसकी व्याख्या वास्तविकता की स्वपरिणामिता से हो जाती है। जगत् में जो भी परिवर्तन किसी समय होता है, उसकी प्रेरणा उस समय के जीवों के पिछले कर्मों से मिलती है। फलतः ईश्वर की धारणा के लिए इस तन्त्र में कोई स्थान नहीं रह जाता। सबसे बड़ा आस्तिक होने का दावा करने वाले दर्शन का निरीश्वरवादी होना वस्तुतः विचित्र सा लगता है। पूरे मीमांसा-मत को यदि एक शब्द में व्यक्त किया जाए तो उसे शुद्ध इन्द्रियानुभववादी कहा जा सकता है।