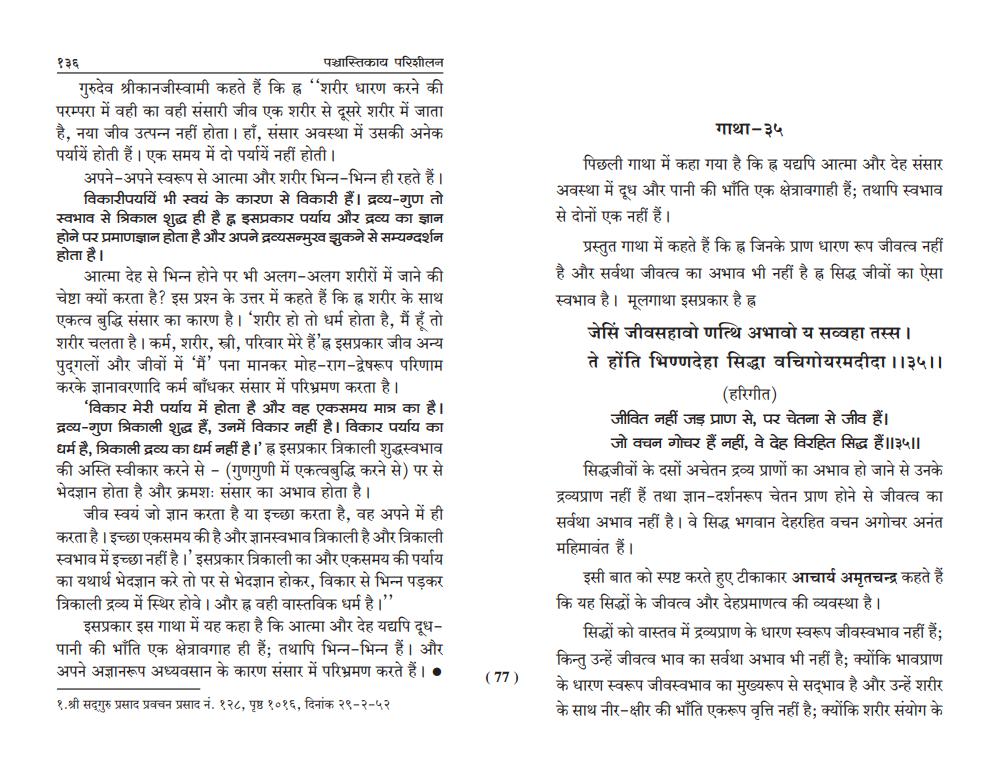________________
पञ्चास्तिकाय परिशीलन
गुरुदेव श्रीकानजीस्वामी कहते हैं कि ह्न “शरीर धारण करने की परम्परा में वही का वही संसारी जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, नया जीव उत्पन्न नहीं होता। हाँ, संसार अवस्था में उसकी अनेक पर्यायें होती हैं। एक समय में दो पर्यायें नहीं होती ।
१३६
अपने-अपने स्वरूप से आत्मा और शरीर भिन्न-भिन्न ही रहते हैं। विकारीपर्यायें भी स्वयं के कारण से विकारी हैं। द्रव्य-गुण तो स्वभाव से त्रिकाल शुद्ध ही है ह्र इसप्रकार पर्याय और द्रव्य का ज्ञान होने पर प्रमाणज्ञान होता है और अपने द्रव्यसन्मुख झुकने से सम्यग्दर्शन होता है।
आत्मा देह से भिन्न होने पर भी अलग-अलग शरीरों में जाने की चेष्टा क्यों करता है ? इस प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि ह्न शरीर के साथ एकत्व बुद्धि संसार का कारण है। 'शरीर हो तो धर्म होता है, मैं हूँ तो शरीर चलता है। कर्म, शरीर, स्त्री, परिवार मेरे हैं'ह्र इसप्रकार जीव अन्य पुद्गलों और जीवों में 'मैं' पना मानकर मोह - राग-द्वेषरूप परिणाम करके ज्ञानावरणादि कर्म बाँधकर संसार में परिभ्रमण करता है।
'विकार मेरी पर्याय में होता है और वह एकसमय मात्र का है। द्रव्य-गुण त्रिकाली शुद्ध हैं, उनमें विकार नहीं है। विकार पर्याय का धर्म है, त्रिकाली द्रव्य का धर्म नहीं है।' ह्र इसप्रकार त्रिकाली शुद्धस्वभाव की अस्ति स्वीकार करने से (गुणगुणी में एकत्वबुद्धि करने से ) पर से भेदज्ञान होता है और क्रमशः संसार का अभाव होता है।
जीव स्वयं जो ज्ञान करता है या इच्छा करता है, वह अपने में ही करता है । इच्छा एकसमय की है और ज्ञानस्वभाव त्रिकाली है और त्रिकाली स्वभाव में इच्छा नहीं है ।' इसप्रकार त्रिकाली का और एकसमय की पर्याय का यथार्थ भेदज्ञान करे तो पर से भेदज्ञान होकर, विकार से भिन्न पड़कर त्रिकाली द्रव्य में स्थिर होवे। और ह्न वही वास्तविक धर्म है। "
इसप्रकार इस गाथा में यह कहा है कि आत्मा और देह यद्यपि दूधपानी की भाँति एक क्षेत्रावगाह ही हैं; तथापि भिन्न-भिन्न हैं । और अपने अज्ञानरूप अध्यवसान के कारण संसार में परिभ्रमण करते हैं। •
१. श्री सद्गुरु प्रसाद प्रवचन प्रसाद नं. १२८, पृष्ठ १०१६, दिनांक २९-२-५२
(77)
गाथा-३५
पिछली गाथा में कहा गया है कि ह्न यद्यपि आत्मा और देह संसार अवस्था में दूध और पानी की भाँति एक क्षेत्रावगाही हैं; तथापि स्वभाव से दोनों एक नहीं हैं।
प्रस्तुत गाथा में कहते हैं कि ह्न जिनके प्राण धारण रूप जीवत्व नहीं है और सर्वथा जीवत्व का अभाव भी नहीं है ह्र सिद्ध जीवों का ऐसा स्वभाव है। मूलगाथा इसप्रकार है ह्र
जेसिं जीवसहावो णत्थि अभावो य सव्वहा तस्स । ते होंति भिण्णदेहा सिद्धा वचिगोयरमदीदा ||३५||
(हरिगीत)
जीवित नहीं जड़ प्राण से, पर चेतना से जीव हैं।
जो वचन गोचर हैं नहीं, वे देह विरहित सिद्ध हैं ||३५|| सिद्धजीवों के दसों अचेतन द्रव्य प्राणों का अभाव हो जाने से उनके द्रव्यप्राण नहीं हैं तथा ज्ञान-दर्शनरूप चेतन प्राण होने से जीवत्व का सर्वथा अभाव नहीं है। वे सिद्ध भगवान देहरहित वचन अगोचर अनंत महिमावंत हैं।
इसी बात को स्पष्ट करते हुए टीकाकार आचार्य अमृतचन्द्र कहते हैं कि यह सिद्धों के जीवत्व और देहप्रमाणत्व की व्यवस्था है।
सिद्धों को वास्तव में द्रव्यप्राण के धारण स्वरूप जीवस्वभाव नहीं हैं; किन्तु उन्हें जीवत्व भाव का सर्वथा अभाव भी नहीं है; क्योंकि भावप्राण के धारण स्वरूप जीवस्वभाव का मुख्यरूप से सद्भाव है और उन्हें शरीर के साथ नीर-क्षीर की भाँति एकरूप वृत्ति नहीं है; क्योंकि शरीर संयोग के