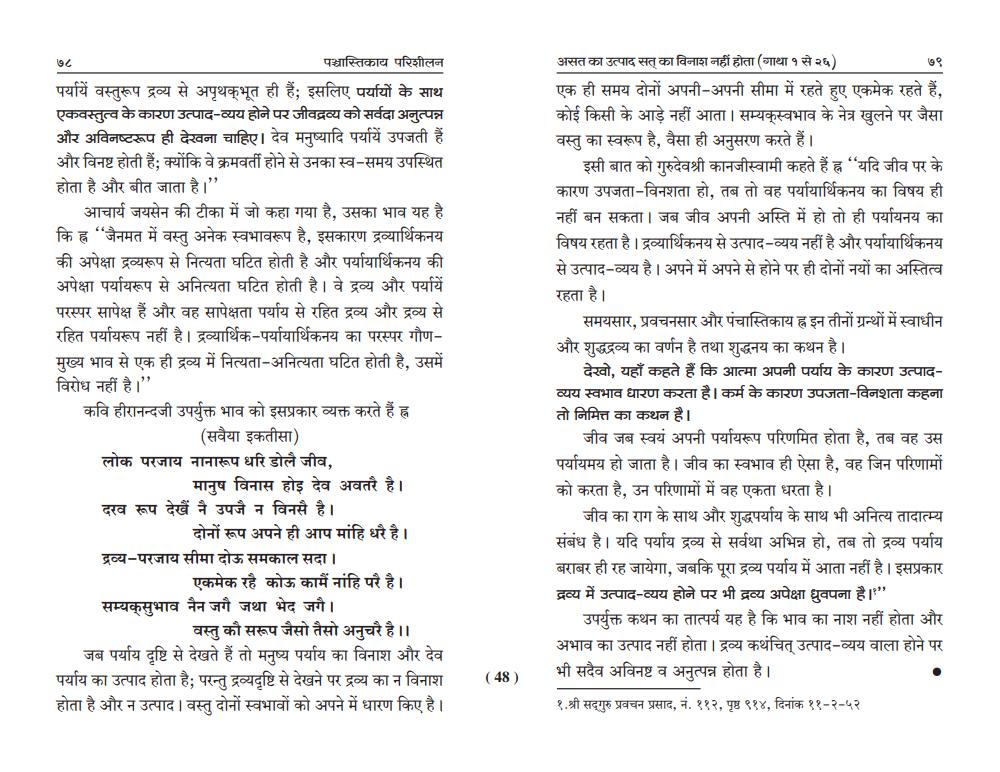________________
७८
पञ्चास्तिकाय परिशीलन पर्यायें वस्तुरूप द्रव्य से अपृथक्भूत ही हैं; इसलिए पर्यायों के साथ एकवस्तुत्व के कारण उत्पाद-व्यय होने पर जीवद्रव्य को सर्वदा अनुत्पन्न और अविनष्टरूप ही देखना चाहिए। देव मनुष्यादि पर्यायें उपजती हैं। और विनष्ट होती हैं; क्योंकि वे क्रमवर्ती होने से उनका स्व-समय उपस्थि होता है और बीत जाता है।"
आचार्य जयसेन की टीका में जो कहा गया है, उसका भाव यह है कि ह्न “जैनमत में वस्तु अनेक स्वभावरूप है, इसकारण द्रव्यार्थिक की अपेक्षा द्रव्यरूप से नित्यता घटित होती है और पर्यायार्थिकनय की अपेक्षा पर्यायरूप से अनित्यता घटित होती है। वे द्रव्य और पर्यायें परस्पर सापेक्ष हैं और वह सापेक्षता पर्याय से रहित द्रव्य और द्रव्य से रहित पर्यायरूप नहीं है। द्रव्यार्थिक-पर्यायार्थिकनय का परस्पर गौणमुख्य भाव से एक ही द्रव्य में नित्यता- अनित्यता घटित होती है, उसमें विरोध नहीं है।"
कवि हीरानन्दजी उपर्युक्त भाव को इसप्रकार व्यक्त करते हैं ह्र (सवैया इकतीसा ) लोक परजाय नानारूप धरि डोलै जीव,
मानुष विनास होइ देव अवतर है। दरव रूप देखें नै उपजै न विनसै है ।
दोनों रूप अपने ही आप मांहि धरै है। द्रव्य-परजाय सीमा दोऊ समकाल सदा ।
एकमेक रहै कोऊ कामैं नांहि परै है ।
सम्यक्सुभाव नैन जगै जथा भेद जगै ।
वस्तु कौ सरूप जैसो तैसो अनुचरै है ।। जब पर्याय दृष्टि से देखते हैं तो मनुष्य पर्याय का विनाश और देव पर्याय का उत्पाद होता है; परन्तु द्रव्यदृष्टि से देखने पर द्रव्य का न विनाश होता है और न उत्पाद । वस्तु दोनों स्वभावों को अपने में धारण किए है।
(48)
असत का उत्पाद सत् का विनाश नहीं होता ( गाथा १ से २६ )
७९
एक ही समय दोनों अपनी-अपनी सीमा में रहते हुए एकमेक रहते हैं, कोई किसी के आड़े नहीं आता । सम्यक्स्वभाव के नेत्र खुलने पर जैसा वस्तु का स्वरूप है, वैसा ही अनुसरण करते हैं।
इसी बात को गुरुदेव श्री कानजीस्वामी कहते हैं ह्न “यदि जीव पर के कारण उपजता- विनशता हो, तब तो वह पर्यायार्थिकनय का विषय ही नहीं बन सकता। जब जीव अपनी अस्ति में हो तो ही पर्यायनय का विषय रहता है। द्रव्यार्थिकनय से उत्पाद-व्यय नहीं है और पर्यायार्थिकनय से उत्पाद-व्यय है। अपने में अपने से होने पर ही दोनों नयों का अस्तित्व रहता है।
समयसार, प्रवचनसार और पंचास्तिकाय ह्न इन तीनों ग्रन्थों में स्वाधीन और शुद्धद्रव्य का वर्णन है तथा शुद्धनय का कथन है।
देखो, यहाँ कहते हैं कि आत्मा अपनी पर्याय के कारण उत्पादव्यय स्वभाव धारण करता है। कर्म के कारण उपजता-विनशता कहना तो निमित्त का कथन है।
जीव जब स्वयं अपनी पर्यायरूप परिणमित होता है, तब वह उस पर्यायमय हो जाता है। जीव का स्वभाव ही ऐसा है, वह जिन परिणामों को करता है, उन परिणामों में वह एकता धरता है।
जीव का राग के साथ और शुद्धपर्याय के साथ भी अनित्य तादात्म्य संबंध है। यदि पर्याय द्रव्य से सर्वथा अभिन्न हो, तब तो द्रव्य पर्याय बराबर ही रह जायेगा, जबकि पूरा द्रव्य पर्याय में आता नहीं है। इसप्रकार द्रव्य में उत्पाद-व्यय होने पर भी द्रव्य अपेक्षा ध्रुवपना है। "
उपर्युक्त कथन का तात्पर्य यह है कि भाव का नाश नहीं होता और अभाव का उत्पाद नहीं होता। द्रव्य कथंचित् उत्पाद-व्यय वाला होने पर भी सदैव अविनष्ट व अनुत्पन्न होता है ।
·
१. श्री सद्गुरु प्रवचन प्रसाद, नं. ११२, पृष्ठ ९१४, दिनांक १९-२-५२