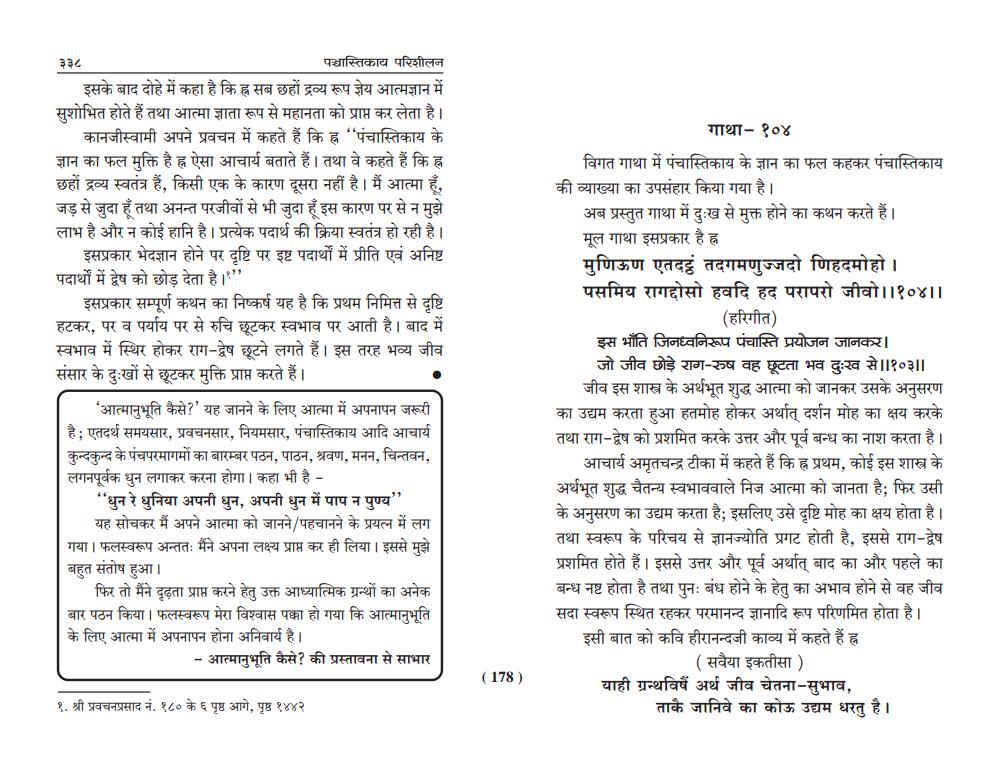________________
पञ्चास्तिकाय परिशीलन इसके बाद दोहे में कहा है कि ह्र सब छहों द्रव्य रूप ज्ञेय आत्मज्ञान में सुशोभित होते हैं तथा आत्मा ज्ञाता रूप से महानता को प्राप्त कर लेता है। कानजीस्वामी अपने प्रवचन में कहते हैं कि ह्न “पंचास्तिकाय के ज्ञान का फल मुक्ति है ऐसा आचार्य बताते हैं। तथा वे कहते हैं कि ह्र छहों द्रव्य स्वतंत्र हैं, किसी एक के कारण दूसरा नहीं है। आत्मा हूँ, जड़ से जुदा हूँ तथा अनन्त परजीवों से भी जुदा हूँ इस कारण पर से न मुझे लाभ है और न कोई हानि है। प्रत्येक पदार्थ की क्रिया स्वतंत्र हो रही है। इसप्रकार भेदज्ञान होने पर दृष्टि पर इष्ट पदार्थों में प्रीति एवं अनिष्ट पदार्थों में द्वेष को छोड़ देता है। "
३३८
इसप्रकार सम्पूर्ण कथन का निष्कर्ष यह है कि प्रथम निमित्त से दृष्टि हटकर, पर व पर्याय पर से रुचि छूटकर स्वभाव पर आती है। बाद में स्वभाव में स्थिर होकर राग-द्वेष छूटने लगते हैं। इस तरह भव्य जीव संसार के दुःखों से छूटकर मुक्ति प्राप्त करते हैं।
•
'आत्मानुभूति कैसे?' यह जानने के लिए आत्मा में अपनापन जरूरी है; एतदर्थ समयसार, प्रवचनसार, नियमसार, पंचास्तिकाय आदि आचार्य कुन्दकुन्द के पंचपरमागमों का बारम्बर पठन पाठन, श्रवण, मनन, चिन्तवन, लगनपूर्वक धुन लगाकर करना होगा। कहा भी है
“धुन रे धुनिया अपनी धुन, अपनी धुन में पाप न पुण्य”
यह सोचकर मैं अपने आत्मा को जानने / पहचानने के प्रयत्न में लग गया। फलस्वरूप अन्ततः मैंने अपना लक्ष्य प्राप्त कर ही लिया। इससे मुझे बहुत संतोष हुआ।
फिर तो मैंने दृढ़ता प्राप्त करने हेतु उक्त आध्यात्मिक ग्रन्थों का अनेक बार पठन किया। फलस्वरूप मेरा विश्वास पक्का हो गया कि आत्मानुभूति के लिए आत्मा में अपनापन होना अनिवार्य है।
आत्मानुभूति कैसे ? की प्रस्तावना से साभार
-
१. श्री प्रवचनप्रसाद नं. १८० के ६ पृष्ठ आगे, पृष्ठ १४४२
(178)
गाथा - १०४
विगत गाथा में पंचास्तिकाय के ज्ञान का फल कहकर पंचास्तिकाय की व्याख्या का उपसंहार किया गया है।
अब प्रस्तुत गाथा में दुःख से मुक्त होने का कथन करते हैं। मूल गाथा इसप्रकार है ह्र मुणिऊण एतदट्ठ तदगमणुज्जदो णिहदमोहो । पसमिय रागद्दोसो हवदि हद परापरो जीवो । । १०४ । ।
(हरिगीत)
इस भाँति जिनध्वनिरूप पंचास्ति प्रयोजन जानकर |
जो जीव छोड़े राग-रुष वह छूटता भव दुःख से || १०३ || जीव इस शास्त्र के अर्थभूत शुद्ध आत्मा को जानकर उसके अनुसरण का उद्यम करता हुआ हतमोह होकर अर्थात् दर्शन मोह का क्षय करके तथा राग-द्वेष को प्रशमित करके उत्तर और पूर्व बन्ध का नाश करता है।
आचार्य अमृतचन्द्र टीका में कहते हैं कि ह्न प्रथम, कोई इस शास्त्र के अर्थभूत शुद्ध चैतन्य स्वभाववाले निज आत्मा को जानता है; फिर उसी के अनुसरण का उद्यम करता है; इसलिए उसे दृष्टि मोह का क्षय होता है। तथा स्वरूप के परिचय से ज्ञानज्योति प्रगट होती है, इससे राग-द्वेष प्रशमित होते हैं। इससे उत्तर और पूर्व अर्थात् बाद का और पहले का बन्ध नष्ट होता है तथा पुनः बंध होने के हेतु का अभाव होने से वह जीव सदा स्वरूप स्थित रहकर परमानन्द ज्ञानादि रूप परिणमित होता है। इसी बात को कवि हीरानन्दजी काव्य में कहते हैं ह्र ( सवैया इकतीसा ) याही ग्रन्थविषै अर्थ जीव चेतना- सुभाव, ताकै जानिवे का कोऊ उद्यम धरतु है ।