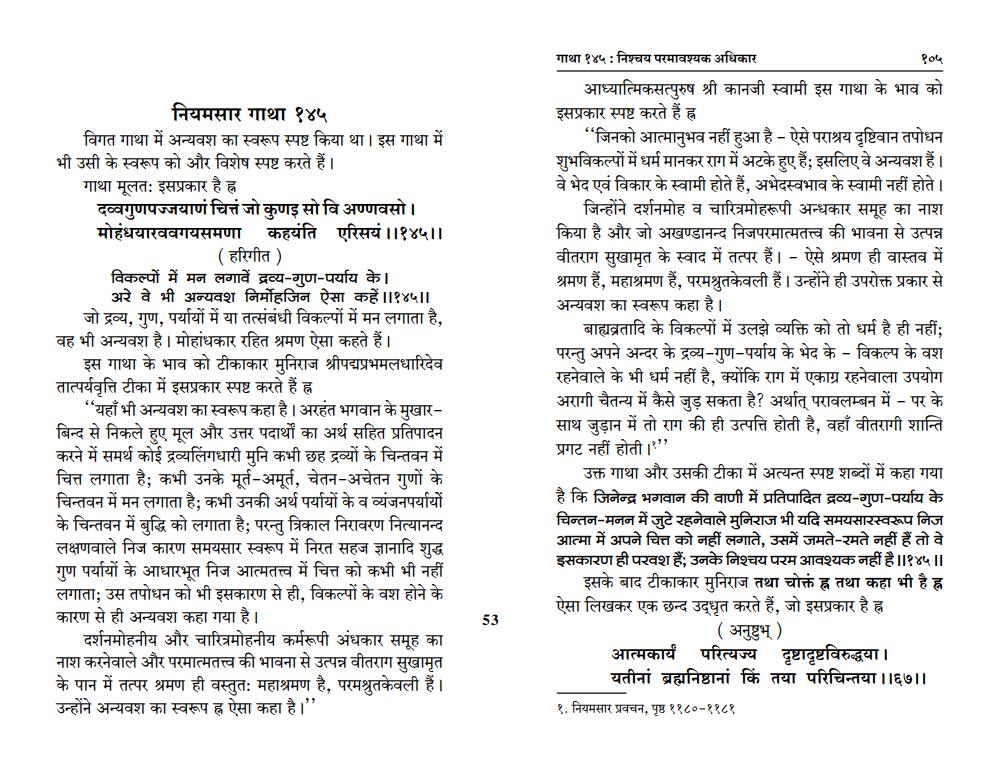________________
नियमसार गाथा १४५ विगत गाथा में अन्यवश का स्वरूप स्पष्ट किया था। इस गाथा में भी उसी के स्वरूप को और विशेष स्पष्ट करते हैं। गाथा मूलतः इसप्रकार है ह्र दव्वगुणपज्जयाणं चित्तं जो कुणइ सो वि अण्णवसो। मोहंधयारववगयसमणा कहयंति एरिसयं ।।१४५।।
(हरिगीत) विकल्पों में मन लगावें द्रव्य-गुण-पर्याय के।
अरे वे भी अन्यवश निर्मोहजिन ऐसा कहें।।१४५|| जो द्रव्य, गुण, पर्यायों में या तत्संबंधी विकल्पों में मन लगाता है, वह भी अन्यवश है। मोहांधकार रहित श्रमण ऐसा कहते हैं।
इस गाथा के भाव को टीकाकार मुनिराज श्रीपद्मप्रभमलधारिदेव तात्पर्यवृत्ति टीका में इसप्रकार स्पष्ट करते हैं ह्र ___ “यहाँ भी अन्यवश का स्वरूप कहा है। अरहंत भगवान के मुखारबिन्द से निकले हुए मूल और उत्तर पदार्थों का अर्थ सहित प्रतिपादन करने में समर्थ कोई द्रव्यलिंगधारी मुनि कभी छह द्रव्यों के चिन्तवन में चित्त लगाता है; कभी उनके मूर्त-अमूर्त, चेतन-अचेतन गुणों के चिन्तवन में मन लगाता है; कभी उनकी अर्थ पर्यायों के व व्यंजनपर्यायों के चिन्तवन में बुद्धि को लगाता है; परन्तु त्रिकाल निरावरण नित्यानन्द लक्षणवाले निज कारण समयसार स्वरूप में निरत सहज ज्ञानादि शुद्ध गुण पर्यायों के आधारभूत निज आत्मतत्त्व में चित्त को कभी भी नहीं लगाता; उस तपोधन को भी इसकारण से ही, विकल्पों के वश होने के कारण से ही अन्यवश कहा गया है।
दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीय कर्मरूपी अंधकार समूह का नाश करनेवाले और परमात्मतत्त्व की भावना से उत्पन्न वीतराग सुखामृत के पान में तत्पर श्रमण ही वस्तुत: महाश्रमण है, परमश्रुतकेवली हैं। उन्होंने अन्यवश का स्वरूप ह्न ऐसा कहा है।"
गाथा १४५ : निश्चय परमावश्यक अधिकार
आध्यात्मिकसत्पुरुष श्री कानजी स्वामी इस गाथा के भाव को इसप्रकार स्पष्ट करते हैं ह्न
“जिनको आत्मानुभव नहीं हुआ है - ऐसे पराश्रय दृष्टिवान तपोधन शुभविकल्पों में धर्म मानकर राग में अटके हुए हैं; इसलिए वे अन्यवश हैं। वे भेद एवं विकार के स्वामी होते हैं, अभेदस्वभाव के स्वामी नहीं होते।
जिन्होंने दर्शनमोह व चारित्रमोहरूपी अन्धकार समूह का नाश किया है और जो अखण्डानन्द निजपरमात्मतत्त्व की भावना से उत्पन्न वीतराग सुखामृत के स्वाद में तत्पर हैं। - ऐसे श्रमण ही वास्तव में श्रमण हैं, महाश्रमण हैं, परमश्रुतकेवली हैं। उन्होंने ही उपरोक्त प्रकार से अन्यवश का स्वरूप कहा है।
बाह्यव्रतादि के विकल्पों में उलझे व्यक्ति को तो धर्म है ही नहीं; परन्तु अपने अन्दर के द्रव्य-गुण-पर्याय के भेद के - विकल्प के वश रहनेवाले के भी धर्म नहीं है, क्योंकि राग में एकाग्र रहनेवाला उपयोग अरागी चैतन्य में कैसे जुड़ सकता है? अर्थात् परावलम्बन में - पर के साथ जुड़ान में तो राग की ही उत्पत्ति होती है, वहाँ वीतरागी शान्ति प्रगट नहीं होती।"
उक्त गाथा और उसकी टीका में अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि जिनेन्द्र भगवान की वाणी में प्रतिपादित द्रव्य-गुण-पर्याय के चिन्तन-मनन में जटे रहनेवाले मनिराज भी यदि समयसारस्वरूप निज आत्मा में अपने चित्त को नहीं लगाते, उसमें जमते-रमते नहीं हैं तो वे इसकारण ही परवश हैं। उनके निश्चय परम आवश्यक नहीं है।।१४५॥
इसके बाद टीकाकार मुनिराज तथा चोक्तं ह्न तथा कहा भी है तू ऐसा लिखकर एक छन्द उद्धृत करते हैं, जो इसप्रकार है ह्र
(अनुष्टुभ् ) आत्मकार्यं परित्यज्य दृष्टादृष्टविरुद्धया।
यतीनां ब्रह्मनिष्ठानां किं तया परिचिन्तया ।।६७।। १. नियमसार प्रवचन, पृष्ठ ११८०-११८१