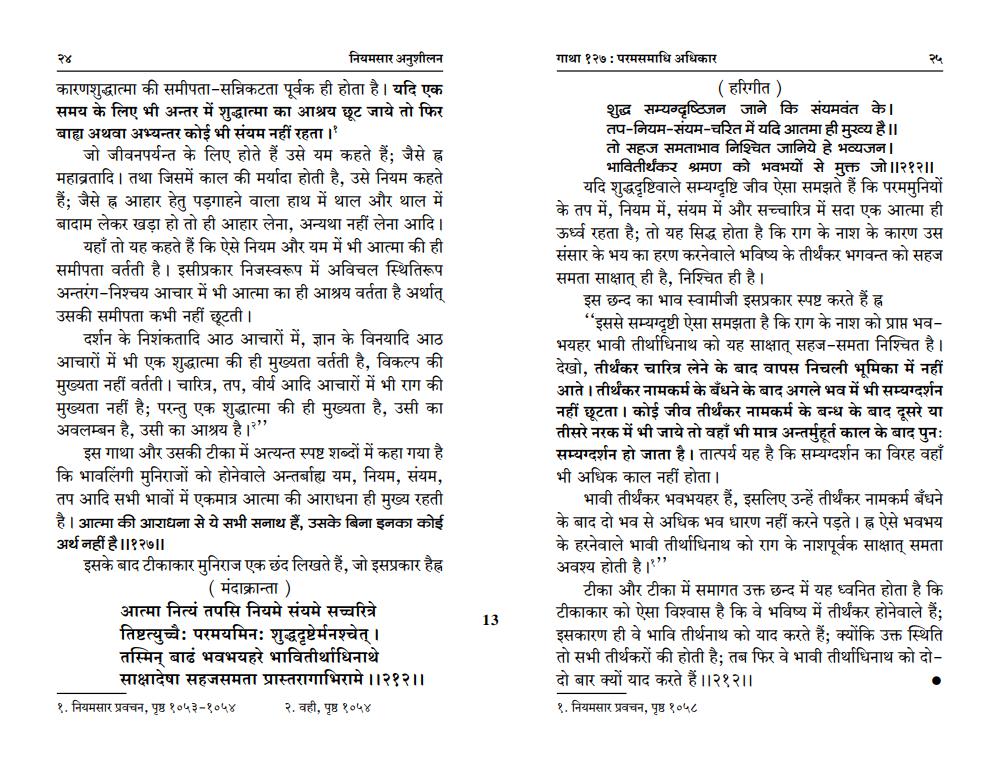________________
नियमसार अनुशीलन कारणशुद्धात्मा की समीपता-सन्निकटता पूर्वक ही होता है। यदि एक समय के लिए भी अन्तर में शुद्धात्मा का आश्रय छूट जाये तो फिर बाह्य अथवा अभ्यन्तर कोई भी संयम नहीं रहता।'
जो जीवनपर्यन्त के लिए होते हैं उसे यम कहते हैं। जैसे ह्र महाव्रतादि । तथा जिसमें काल की मर्यादा होती है, उसे नियम कहते हैं; जैसे ह्र आहार हेतु पड़गाहने वाला हाथ में थाल और थाल में बादाम लेकर खड़ा हो तो ही आहार लेना, अन्यथा नहीं लेना आदि ।
यहाँ तो यह कहते हैं कि ऐसे नियम और यम में भी आत्मा की ही समीपता वर्तती है। इसीप्रकार निजस्वरूप में अविचल स्थितिरूप अन्तरंग-निश्चय आचार में भी आत्मा का ही आश्रय वर्तता है अर्थात् उसकी समीपता कभी नहीं छूटती।
दर्शन के निशंकतादि आठ आचारों में, ज्ञान के विनयादि आठ आचारों में भी एक शुद्धात्मा की ही मुख्यता वर्तती है, विकल्प की मुख्यता नहीं वर्तती। चारित्र, तप, वीर्य आदि आचारों में भी राग की मुख्यता नहीं है; परन्तु एक शुद्धात्मा की ही मुख्यता है, उसी का अवलम्बन है, उसी का आश्रय है।"
इस गाथा और उसकी टीका में अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि भावलिंगी मुनिराजों को होनेवाले अन्तर्बाह्य यम, नियम, संयम, तप आदि सभी भावों में एकमात्र आत्मा की आराधना ही मुख्य रहती है। आत्मा की आराधना से ये सभी सनाथ हैं, उसके बिना इनका कोई अर्थ नहीं है।।१२७॥ इसके बाद टीकाकार मुनिराज एक छंद लिखते हैं, जो इसप्रकार हैह्न
(मंदाक्रान्ता) आत्मा नित्यं तपसि नियमे संयमे सच्चरित्रे तिष्टत्युच्चैः परमयमिन: शुद्धदृष्टेमनश्चेत् । तस्मिन् बाढं भवभयहरे भावितीर्थाधिनाथे
साक्षादेषा सहजसमता प्रास्तरागाभिरामे ।।२१२।। १. नियमसार प्रवचन, पृष्ठ १०५३-१०५४ २ . वही, पृष्ठ १०५४
गाथा १२७ : परमसमाधि अधिकार
( हरिगीत ) शुद्ध सम्यग्दृष्टिजन जाने कि संयमवंत के। तप-नियम-संयम-चरित में यदि आतमा ही मुख्य है। तो सहज समताभाव निश्चित जानिये हे भव्यजन। भावितीर्थंकर श्रमण को भवभयों से मुक्त जो ॥२१२।। यदि शुद्धदृष्टिवाले सम्यग्दृष्टि जीव ऐसा समझते हैं कि परममुनियों के तप में, नियम में, संयम में और सच्चारित्र में सदा एक आत्मा ही ऊर्ध्व रहता है तो यह सिद्ध होता है कि राग के नाश के कारण उस संसार के भय का हरण करनेवाले भविष्य के तीर्थंकर भगवन्त को सहज समता साक्षात् ही है, निश्चित ही है।
इस छन्द का भाव स्वामीजी इसप्रकार स्पष्ट करते हैं ह्र
“इससे सम्यग्दृष्टी ऐसा समझता है कि राग के नाश को प्राप्त भवभयहर भावी तीर्थाधिनाथ को यह साक्षात् सहज-समता निश्चित है। देखो, तीर्थंकर चारित्र लेने के बाद वापस निचली भूमिका में नहीं आते । तीर्थकर नामकर्म के बँधने के बाद अगले भव में भी सम्यग्दर्शन नहीं छूटता। कोई जीव तीर्थंकर नामकर्म के बन्ध के बाद दूसरे या तीसरे नरक में भी जाये तो वहाँ भी मात्र अन्तर्मुहूर्त काल के बाद पुनः सम्यग्दर्शन हो जाता है। तात्पर्य यह है कि सम्यग्दर्शन का विरह वहाँ भी अधिक काल नहीं होता। ____ भावी तीर्थंकर भवभयहर हैं, इसलिए उन्हें तीर्थंकर नामकर्म बँधने के बाद दो भव से अधिक भव धारण नहीं करने पड़ते । ह्न ऐसे भवभय के हरनेवाले भावी तीर्थाधिनाथ को राग के नाशपूर्वक साक्षात् समता अवश्य होती है।"
टीका और टीका में समागत उक्त छन्द में यह ध्वनित होता है कि टीकाकार को ऐसा विश्वास है कि वे भविष्य में तीर्थंकर होनेवाले हैं; इसकारण ही वे भावि तीर्थनाथ को याद करते हैं; क्योंकि उक्त स्थिति तो सभी तीर्थकरों की होती है; तब फिर वे भावी तीर्थाधिनाथ को दोदो बार क्यों याद करते हैं ।।२१२।। १. नियमसार प्रवचन, पृष्ठ १०५८