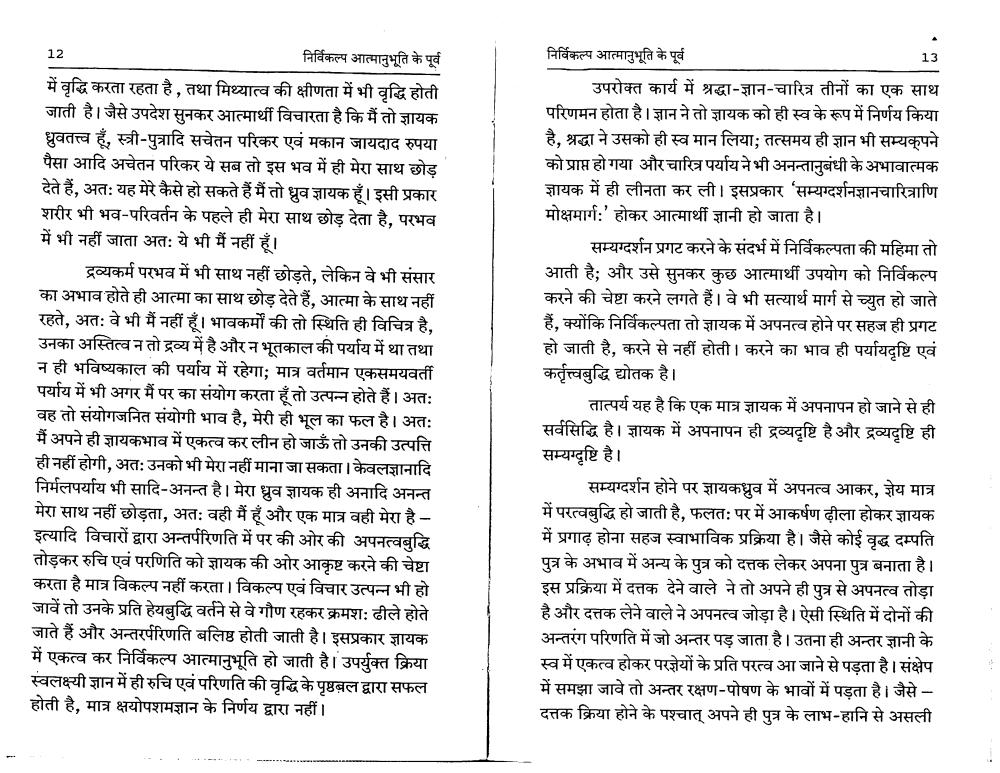________________
13
12
निर्विकल्प आत्मानुभूति के पूर्व में वृद्धि करता रहता है, तथा मिथ्यात्व की क्षीणता में भी वृद्धि होती जाती है। जैसे उपदेश सुनकर आत्मार्थी विचारता है कि मैं तो ज्ञायक ध्रुवतत्त्व हूँ, स्त्री-पुत्रादि सचेतन परिकर एवं मकान जायदाद रुपया पैसा आदि अचेतन परिकर ये सब तो इस भव में ही मेरा साथ छोड़ देते हैं, अत: यह मेरे कैसे हो सकते हैं मैं तो ध्रुव ज्ञायक हूँ। इसी प्रकार शरीर भी भव-परिवर्तन के पहले ही मेरा साथ छोड़ देता है, परभव में भी नहीं जाता अत: ये भी मैं नहीं हूँ।
द्रव्यकर्म परभव में भी साथ नहीं छोड़ते, लेकिन वे भी संसार का अभाव होते ही आत्मा का साथ छोड़ देते हैं, आत्मा के साथ नहीं रहते, अत: वे भी मैं नहीं हूँ। भावकर्मों की तो स्थिति ही विचित्र है, उनका अस्तित्व न तो द्रव्य में है और न भूतकाल की पर्याय में था तथा न ही भविष्यकाल की पर्याय में रहेगा; मात्र वर्तमान एकसमयवर्ती पर्याय में भी अगर मैं पर का संयोग करता हूँ तो उत्पन्न होते हैं। अत: वह तो संयोगजनित संयोगी भाव है, मेरी ही भूल का फल है। अतः मैं अपने ही ज्ञायकभाव में एकत्व कर लीन हो जाऊँ तो उनकी उत्पत्ति ही नहीं होगी, अत: उनको भी मेरा नहीं माना जा सकता। केवलज्ञानादि निर्मलपर्याय भी सादि-अनन्त है। मेरा ध्रुव ज्ञायक ही अनादि अनन्त मेरा साथ नहीं छोड़ता, अत: वही मैं हूँ और एक मात्र वही मेरा है - इत्यादि विचारों द्वारा अन्तर्परिणति में पर की ओर की अपनत्वबुद्धि तोड़कर रुचि एवं परणिति को ज्ञायक की ओर आकृष्ट करने की चेष्टा करता है मात्र विकल्प नहीं करता। विकल्प एवं विचार उत्पन्न भी हो जावें तो उनके प्रति हेयबुद्धि वर्तने से वे गौण रहकर क्रमश: ढीले होते जाते हैं और अन्तरर्परिणति बलिष्ठ होती जाती है। इसप्रकार ज्ञायक में एकत्व कर निर्विकल्प आत्मानुभूति हो जाती है। उपर्युक्त क्रिया स्वलक्ष्यी ज्ञान में ही रुचि एवं परिणति की वृद्धि के पृष्ठबल द्वारा सफल होती है, मात्र क्षयोपशमज्ञान के निर्णय द्वारा नहीं।
निर्विकल्प आत्मानुभूति के पूर्व
उपरोक्त कार्य में श्रद्धा-ज्ञान-चारित्र तीनों का एक साथ परिणमन होता है। ज्ञान ने तो ज्ञायक को ही स्व के रूप में निर्णय किया है, श्रद्धा ने उसको ही स्व मान लिया; तत्समय ही ज्ञान भी सम्यक्पने को प्राप्त हो गया और चारित्र पर्याय ने भी अनन्तानुबंधी के अभावात्मक ज्ञायक में ही लीनता कर ली। इसप्रकार 'सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग:' होकर आत्मार्थी ज्ञानी हो जाता है।
सम्यग्दर्शन प्रगट करने के संदर्भ में निर्विकल्पता की महिमा तो आती है; और उसे सुनकर कुछ आत्मार्थी उपयोग को निर्विकल्प करने की चेष्टा करने लगते हैं। वे भी सत्यार्थ मार्ग से च्युत हो जाते हैं, क्योंकि निर्विकल्पता तो ज्ञायक में अपनत्व होने पर सहज ही प्रगट हो जाती है, करने से नहीं होती। करने का भाव ही पर्यायदृष्टि एवं कर्तृत्त्वबुद्धि द्योतक है।
तात्पर्य यह है कि एक मात्र ज्ञायक में अपनापन हो जाने से ही सर्वसिद्धि है। ज्ञायक में अपनापन ही द्रव्यदृष्टि है और द्रव्यदृष्टि ही सम्यग्दृष्टि है।
सम्यग्दर्शन होने पर ज्ञायकध्रुव में अपनत्व आकर, ज्ञेय मात्र में परत्वबुद्धि हो जाती है, फलत: पर में आकर्षण ढ़ीला होकर ज्ञायक में प्रगाढ़ होना सहज स्वाभाविक प्रक्रिया है। जैसे कोई वृद्ध दम्पति पुत्र के अभाव में अन्य के पुत्र को दत्तक लेकर अपना पुत्र बनाता है। इस प्रक्रिया में दत्तक देने वाले ने तो अपने ही पुत्र से अपनत्व तोड़ा है और दत्तक लेने वाले ने अपनत्व जोड़ा है। ऐसी स्थिति में दोनों की अन्तरंग परिणति में जो अन्तर पड़ जाता है। उतना ही अन्तर ज्ञानी के स्व में एकत्व होकर परज्ञेयों के प्रति परत्व आ जाने से पड़ता है। संक्षेप में समझा जावे तो अन्तर रक्षण-पोषण के भावों में पड़ता है। जैसेदत्तक क्रिया होने के पश्चात् अपने ही पुत्र के लाभ-हानि से असली