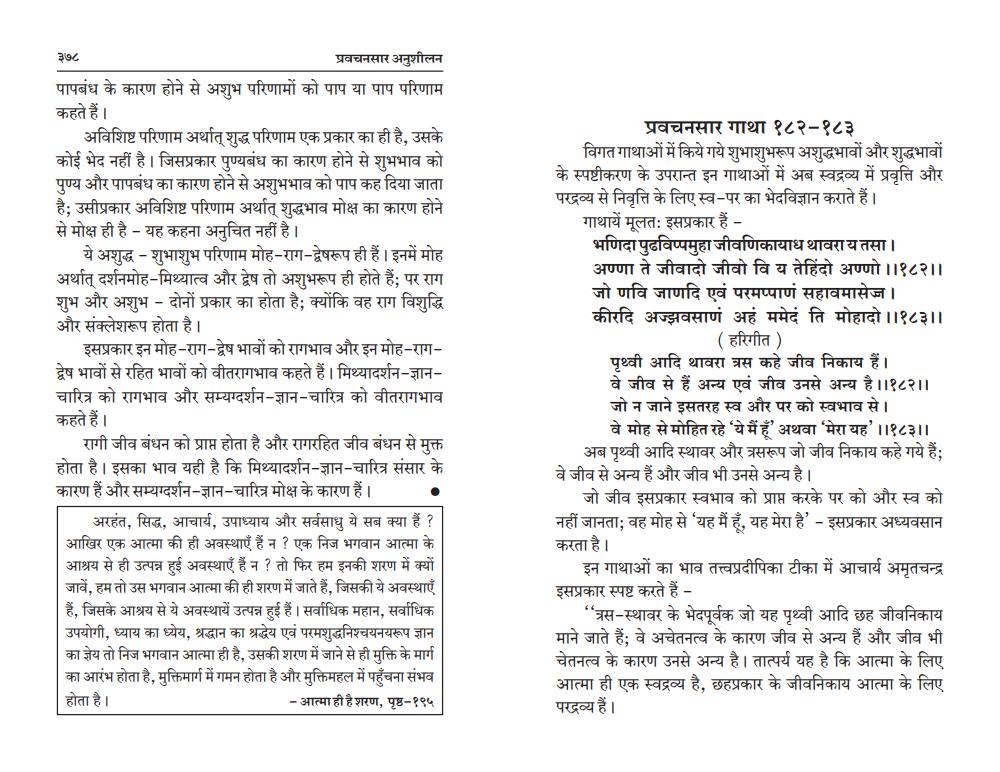________________
३७८
प्रवचनसार अनुशीलन पापबंध के कारण होने से अशुभ परिणामों को पाप या पाप परिणाम कहते हैं।
अविशिष्ट परिणाम अर्थात् शुद्ध परिणाम एक प्रकार का ही है, उसके कोई भेद नहीं है। जिसप्रकार पुण्यबंध का कारण होने से शुभभाव को पुण्य और पापबंध का कारण होने से अशुभभाव को पाप कह दिया जाता है; उसीप्रकार अविशिष्ट परिणाम अर्थात् शुद्धभाव मोक्ष का कारण होने से मोक्ष ही है - यह कहना अनुचित नहीं है।
ये अशुद्ध - शुभाशुभ परिणाम मोह-राग-द्वेषरूप ही हैं। इनमें मोह अर्थात् दर्शनमोह-मिथ्यात्व और द्वेष तो अशुभरूप ही होते हैं; पर राग शुभ और अशुभ - दोनों प्रकार का होता है; क्योंकि वह राग विशुद्धि और संक्लेशरूप होता है।
इसप्रकार इन मोह-राग-द्वेष भावों को रागभाव और इन मोह-रागद्वेष भावों से रहित भावों को वीतरागभाव कहते हैं। मिथ्यादर्शन-ज्ञानचारित्र को रागभाव और सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र को वीतरागभाव कहते हैं।
रागी जीव बंधन को प्राप्त होता है और रागरहित जीव बंधन से मुक्त होता है। इसका भाव यही है कि मिथ्यादर्शन-ज्ञान-चारित्र संसार के कारण हैं और सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र मोक्ष के कारण हैं। __अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और सर्वसाधु ये सब क्या हैं ? आखिर एक आत्मा की ही अवस्थाएँ हैं न ? एक निज भगवान आत्मा के आश्रय से ही उत्पन्न हुई अवस्थाएँ हैं न ? तो फिर हम इनकी शरण में क्यों जावें, हम तो उस भगवान आत्मा की ही शरण में जाते हैं, जिसकी ये अवस्थाएँ हैं, जिसके आश्रय से ये अवस्थायें उत्पन्न हुई हैं। सर्वाधिक महान, सर्वाधिक उपयोगी, ध्याय का ध्येय, श्रद्धान का श्रद्धेय एवं परमशुद्धनिश्चयनयरूप ज्ञान का ज्ञेय तो निज भगवान आत्मा ही है, उसकी शरण में जाने से ही मुक्ति के मार्ग का आरंभ होता है, मुक्तिमार्ग में गमन होता है और मुक्तिमहल में पहुँचना संभव होता है।
-आत्मा ही है शरण, पृष्ठ-१९५
प्रवचनसार गाथा १८२-१८३ विगत गाथाओं में किये गये शुभाशुभरूप अशुद्धभावों और शुद्धभावों के स्पष्टीकरण के उपरान्त इन गाथाओं में अब स्वद्रव्य में प्रवृत्ति और परद्रव्य से निवृत्ति के लिए स्व-पर का भेदविज्ञान कराते हैं। गाथायें मूलत: इसप्रकार हैं - भणिदा पुढविप्पमुहा जीवणिकायाधथावराय तसा। अण्णा ते जीवादो जीवो वि य तेहिंदो अण्णो ।।१८२।। जो णवि जाणदि एवं परमप्पाणं सहावमासेज । कीरदि अज्झवसाणं अहं ममेदं ति मोहादो।।१८३।।
(हरिगीत) पृथ्वी आदि थावरा त्रस कहे जीव निकाय हैं। वे जीव से हैं अन्य एवं जीव उनसे अन्य है।।१८२।। जो न जाने इसतरह स्व और पर को स्वभाव से।
वे मोह से मोहित रहे ये मैं हूँ' अथवा 'मेरा यह' ।।१८३।। अब पृथ्वी आदि स्थावर और त्रसरूप जो जीव निकाय कहे गये हैं; वे जीव से अन्य हैं और जीव भी उनसे अन्य है।
जो जीव इसप्रकार स्वभाव को प्राप्त करके पर को और स्व को नहीं जानता; वह मोह से 'यह मैं हूँ, यह मेरा हैं' - इसप्रकार अध्यवसान करता है।
इन गाथाओं का भाव तत्त्वप्रदीपिका टीका में आचार्य अमृतचन्द्र इसप्रकार स्पष्ट करते हैं -
"त्रस-स्थावर के भेदपूर्वक जो यह पृथ्वी आदि छह जीवनिकाय माने जाते हैं; वे अचेतनत्व के कारण जीव से अन्य हैं और जीव भी चेतनत्व के कारण उनसे अन्य है। तात्पर्य यह है कि आत्मा के लिए आत्मा ही एक स्वद्रव्य है, छहप्रकार के जीवनिकाय आत्मा के लिए परद्रव्य हैं।