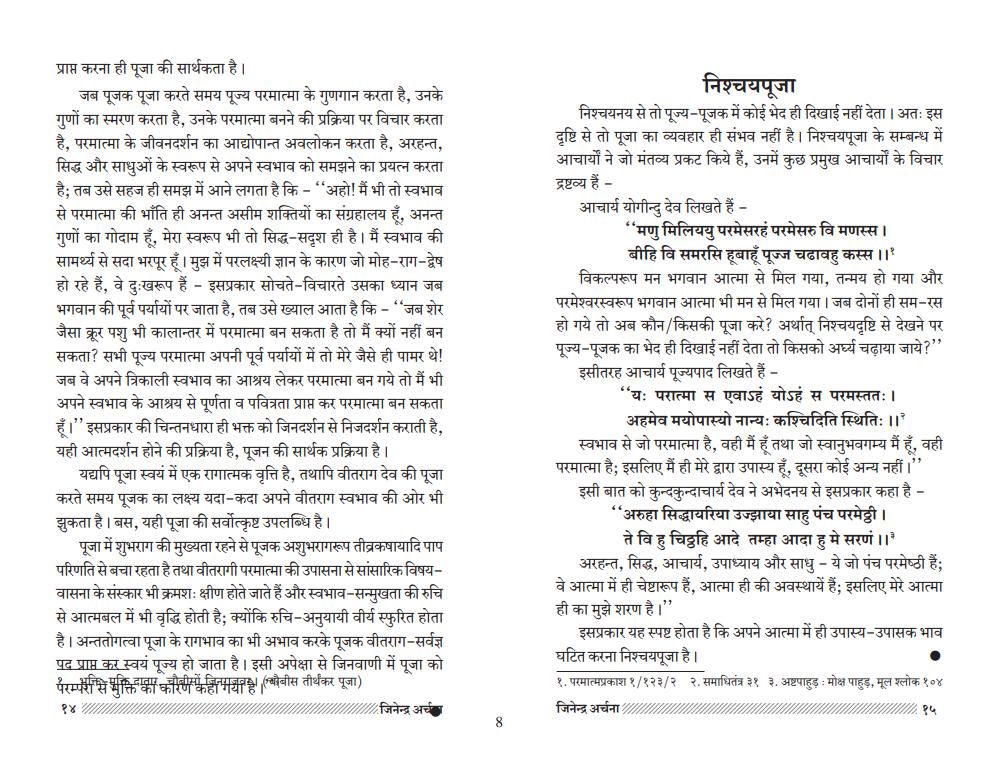________________
प्राप्त करना ही पूजा की सार्थकता है।
जब पूजक पूजा करते समय पूज्य परमात्मा के गुणगान करता है, उनके गुणों का स्मरण करता है, उनके परमात्मा बनने की प्रक्रिया पर विचार करता है, परमात्मा के जीवनदर्शन का आद्योपान्त अवलोकन करता है, अरहन्त, सिद्ध और साधुओं के स्वरूप से अपने स्वभाव को समझने का प्रयत्न करता है; तब उसे सहज ही समझ में आने लगता है कि - "अहो! मैं भी तो स्वभाव से परमात्मा की भाँति ही अनन्त असीम शक्तियों का संग्रहालय हूँ, अनन्त गुणों का गोदाम हूँ, मेरा स्वरूप भी तो सिद्ध-सदृश ही है। मैं स्वभाव की सामर्थ्य से सदा भरपूर हूँ। मुझ में परलक्ष्यी ज्ञान के कारण जो मोह-राग-द्वेष हो रहे हैं, वे दुःखरूप हैं - इसप्रकार सोचते-विचारते उसका ध्यान जब भगवान की पूर्व पर्यायों पर जाता है, तब उसे ख्याल आता है कि - "जब शेर जैसा क्रूर पशु भी कालान्तर में परमात्मा बन सकता है तो मैं क्यों नहीं बन सकता? सभी पूज्य परमात्मा अपनी पूर्व पर्यायों में तो मेरे जैसे ही पामर थे! जब वे अपने त्रिकाली स्वभाव का आश्रय लेकर परमात्मा बन गये तो मैं भी अपने स्वभाव के आश्रय से पूर्णता व पवित्रता प्राप्त कर परमात्मा बन सकता हूँ।" इसप्रकार की चिन्तनधारा ही भक्त को जिनदर्शन से निजदर्शन कराती है, यही आत्मदर्शन होने की प्रक्रिया है, पूजन की सार्थक प्रक्रिया है।
यद्यपि पूजा स्वयं में एक रागात्मक वृत्ति है, तथापि वीतराग देव की पूजा करते समय पूजक का लक्ष्य यदा-कदा अपने वीतराग स्वभाव की ओर भी झुकता है। बस, यही पूजा की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि है।
पूजा में शुभराग की मुख्यता रहने से पूजक अशुभरागरूप तीव्रकषायादि पाप परिणति से बचा रहता है तथा वीतरागी परमात्मा की उपासना से सांसारिक विषयवासना के संस्कार भी क्रमशः क्षीण होते जाते हैं और स्वभाव-सन्मुखता की रुचि से आत्मबल में भी वृद्धि होती है; क्योंकि रुचि-अनुयायी वीर्य स्फुरित होता है। अन्ततोगत्वा पूजा के रागभाव का भी अभाव करके पूजक वीतराग-सर्वज्ञ पद प्राप्त कर स्वयं पूज्य हो जाता है। इसी अपेक्षा से जिनवाणी में पूजा को परम्परसि मुक्तिका कारण हो गया है यौबीस तीर्थंकर पूजा)
1000 जिनेन्द्र अर्चक
निश्चयपूजा निश्चयनय से तो पूज्य-पूजक में कोई भेद ही दिखाई नहीं देता । अतः इस दृष्टि से तो पूजा का व्यवहार ही संभव नहीं है। निश्चयपूजा के सम्बन्ध में आचार्यों ने जो मंतव्य प्रकट किये हैं, उनमें कुछ प्रमुख आचार्यों के विचार द्रष्टव्य हैं - __ आचार्य योगीन्दु देव लिखते हैं -
"मणु मिलिययु परमेसरहं परमेसरु वि मणस्स।
बीहि वि समरसि हूबाहूँ पूज्ज चढावहु कस्स ।।' विकल्परूप मन भगवान आत्मा से मिल गया, तन्मय हो गया और परमेश्वरस्वरूप भगवान आत्मा भी मन से मिल गया। जब दोनों ही सम-रस हो गये तो अब कौन/किसकी पूजा करे? अर्थात् निश्चयदृष्टि से देखने पर पूज्य-पूजक का भेद ही दिखाई नहीं देता तो किसको अर्घ्य चढ़ाया जाये?" इसीतरह आचार्य पूज्यपाद लिखते हैं -
"यः परात्मा स एवाऽहं योऽहं स परमस्ततः ।
अहमेव मयोपास्यो नान्यः कश्चिदिति स्थितिः ।।' स्वभाव से जो परमात्मा है, वही मैं हैं तथा जो स्वानुभवगम्य मैं हैं, वही परमात्मा है; इसलिए मैं ही मेरे द्वारा उपास्य हूँ, दूसरा कोई अन्य नहीं।" इसी बात को कुन्दकुन्दाचार्य देव ने अभेदनय से इसप्रकार कहा है -
"अरुहा सिद्धायरिया उज्झाया साहु पंच परमेठ्ठी ।
ते वि हु चिहि आदे तम्हा आदा हु मे सरणं ।। अरहन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु - ये जो पंच परमेष्ठी हैं; वे आत्मा में ही चेष्टारूप हैं, आत्मा ही की अवस्थायें हैं; इसलिए मेरे आत्मा ही का मुझे शरण है।”
इसप्रकार यह स्पष्ट होता है कि अपने आत्मा में ही उपास्य-उपासक भाव घटित करना निश्चयपूजा है। १. परमात्मप्रकाश १/१२३/२ २. समाधितंत्र ३१ ३. अष्टपाहुड़ : मोक्ष पाहुड़, मूल श्लोक १०४ जिनेन्द्र अर्चना/0000000