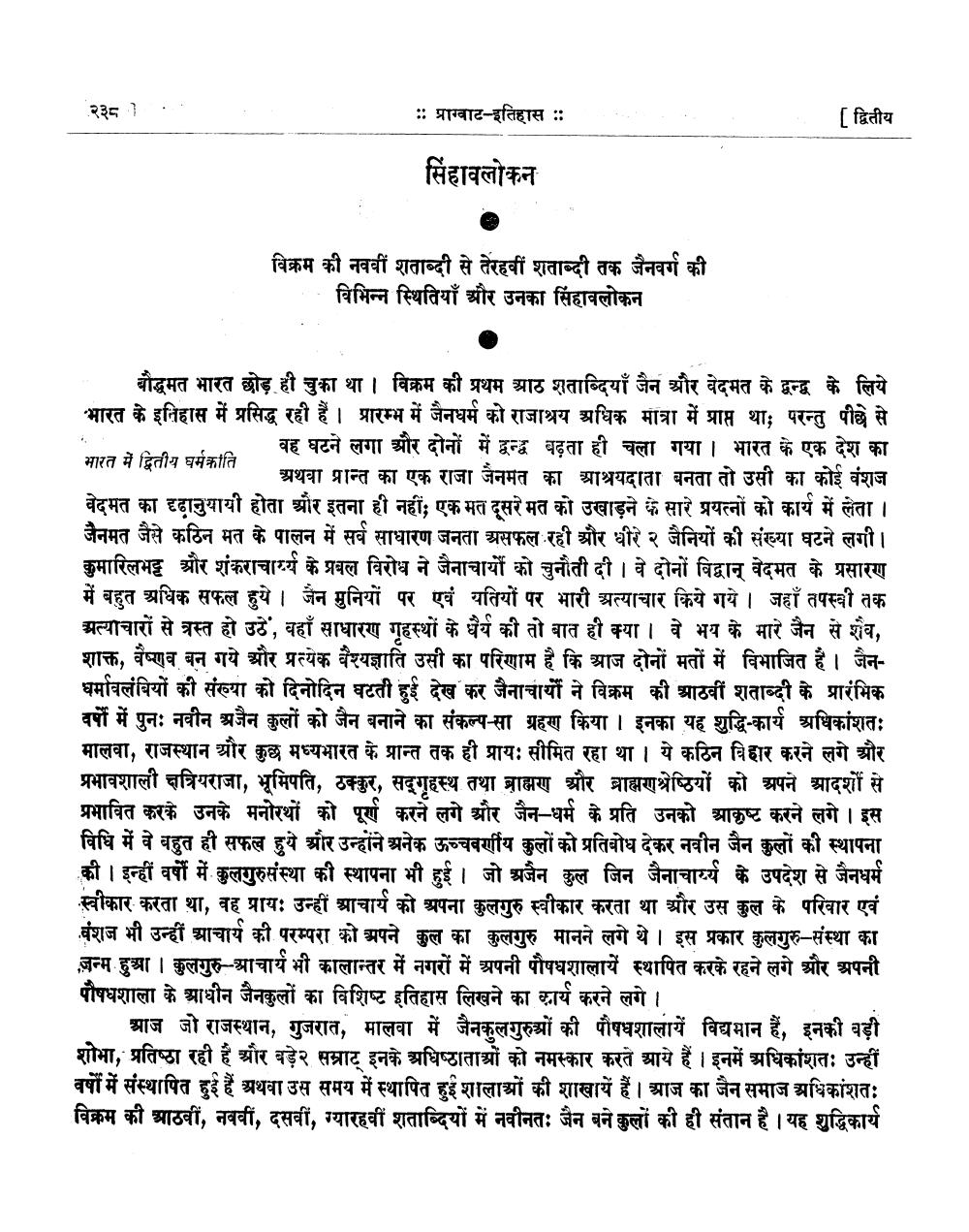________________
२३८1 .
:: प्राग्वाट-इतिहास ::
[द्वितीय
सिंहावलोकन
विक्रम की नववीं शताब्दी से तेरहवीं शताब्दी तक जैनवर्ग की
विभिन्न स्थितियाँ और उनका सिंहावलोकन
बौद्धमत भारत छोड़ ही चुका था। विक्रम की प्रथम आठ शताब्दियाँ जैन और वेदमत के द्वन्द्व के लिये भारत के इतिहास में प्रसिद्ध रही हैं। प्रारम्भ में जैनधर्म को राजाश्रय अधिक मात्रा में प्राप्त था; परन्तु पीछे से
है वह घटने लगा और दोनों में द्वन्द्व बढ़ता ही चला गया। भारत के एक देश का भारत में द्वितीय धर्मक्रांति
" अथवा प्रान्त का एक राजा जैनमत का आश्रयदाता बनता तो उसी का कोई वंशज वेदमत का दृढ़ानुयायी होता और इतना ही नहीं; एक मत दूसरे मत को उखाड़ने के सारे प्रयत्नों को कार्य में लेता। जैनमत जैसे कठिन मत के पालन में सर्व साधारण जनता असफल रही और धीरे २ जैनियों की संख्या घटने लगी। कुमारिलभट्ट और शंकराचार्य के प्रबल विरोध ने जैनाचार्यों को चुनौती दी । वे दोनों विद्वान् वेदमत के प्रसारण में बहुत अधिक सफल हुये। जैन मुनियों पर एवं यतियों पर भारी अत्याचार किये गये । जहाँ तपस्वी तक अत्याचारों से त्रस्त हो उठे, वहाँ साधारण गहस्थों के धैर्य की तो बात ही क्या। वे भय के मारे जैन से शेव, शाक्त, वैष्णव बन गये और प्रत्येक वैश्यज्ञाति उसी का परिणाम है कि आज दोनों मतों में विभाजित है। जैनधर्मावलंबियों की संख्या को दिनोदिन घटती हुई देख कर जैनाचार्यों ने विक्रम की आठवीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में पुनः नवीन अजैन कुलों को जैन बनाने का संकल्प-सा ग्रहण किया। इनका यह शुद्धि-कार्य अधिकांशतः
स्थान और कुछ मध्यभारत के प्रान्त तक ही प्रायः सीमित रहा था। ये कठिन विहार करने लगे और प्रभावशाली क्षत्रियराजा, भूमिपति, ठक्कुर, सद्गृहस्थ तथा ब्राह्मण और ब्राह्मणश्रेष्ठियों को अपने आदर्शों से प्रभावित करके उनके मनोरथों को पूर्ण करने लगे और जैन धर्म के प्रति उनको आकृष्ट करने लगे । इस विधि में वे बहुत ही सफल हुये और उन्होंने अनेक ऊच्चवर्णीय कुलों को प्रतिबोध देकर नवीन जैन कुलों की स्थापना की । इन्हीं वर्षों में कुलगुरुसंस्था की स्थापना भी हुई। जो अजैन कुल जिन जैनाचार्य के उपदेश से जैनधर्म स्वीकार करता था, वह प्रायः उन्हीं आचार्य को अपना कुलगुरु स्वीकार करता था और उस कुल के परिवार एवं वंशज भी उन्हीं आचार्य की परम्परा को अपने कुल का कुलगुरु मानने लगे थे। इस प्रकार कुलगुरु-संस्था का जन्म हुआ । कुलगुरु-आचार्य भी कालान्तर में नगरों में अपनी पौषधशालायें स्थापित करके रहने लगे और अपनी पौषधशाला के आधीन जैनकुलों का विशिष्ट इतिहास लिखने का कार्य करने लगे।
आज जो राजस्थान, गुजरात, मालवा में जैनकुलगुरुओं की पौषधशालायें विद्यमान हैं, इनकी बड़ी शोभा, प्रतिष्ठा रही है और बड़े२ सम्राट् इनके अधिष्ठाताओं को नमस्कार करते आये हैं । इनमें अधिकांशतः उन्हीं वर्षों में संस्थापित हुई हैं अथवा उस समय में स्थापित हुई शालाओं की शाखायें हैं । आज का जैन समाज अधिकांशतः विक्रम की आठवीं, नववीं, दसवीं, ग्यारहवीं शताब्दियों में नवीनतः जैन बने कुलों की ही संतान है । यह शुद्धिकार्य