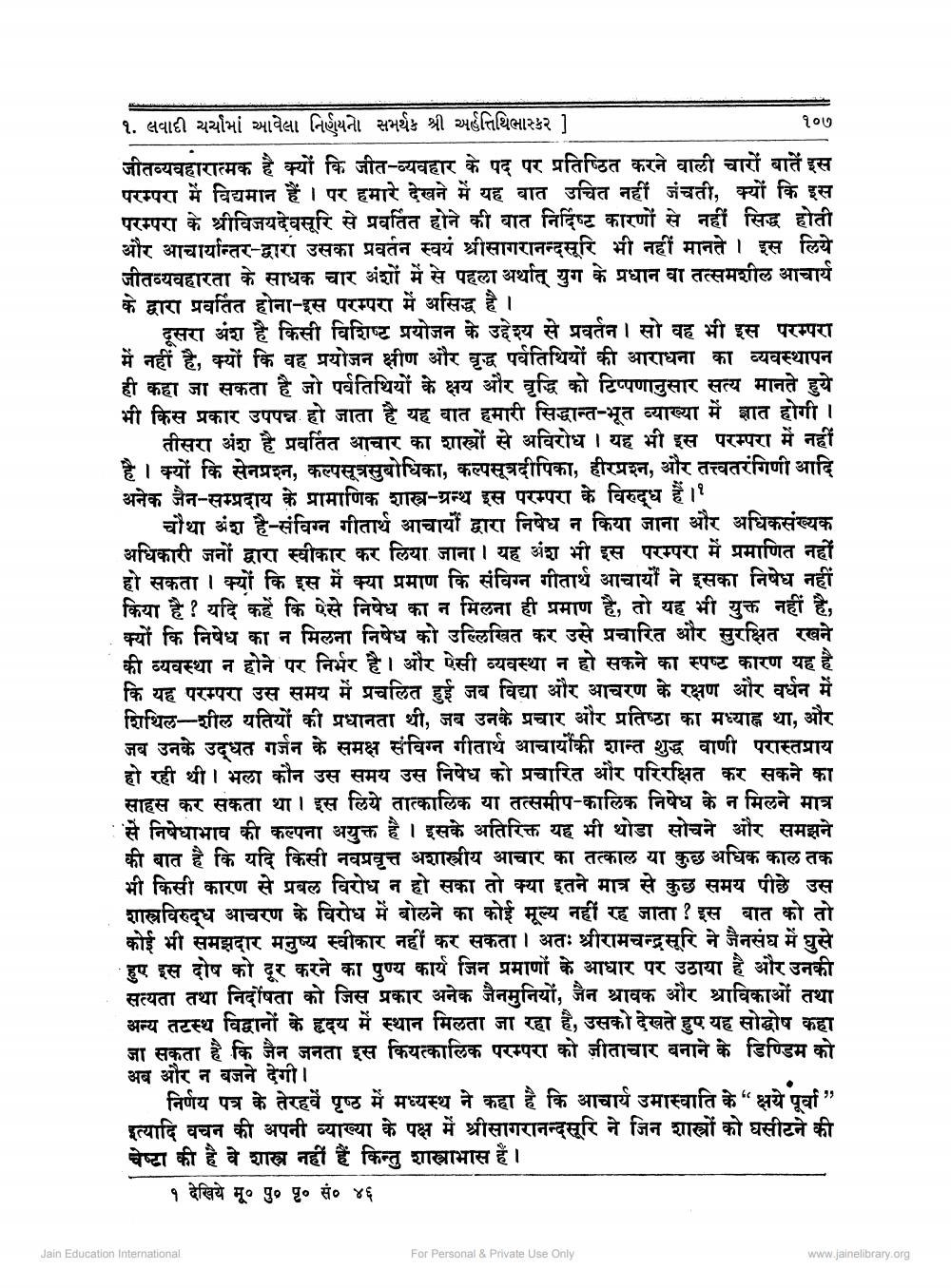________________
૧. લવાદી ચર્ચામાં આવેલા નિર્ણયના સમર્થક શ્રી અત્તિથિભાસ્કર
१०७
anoranत्मक है क्यों कि जीत - व्यवहार के पद पर प्रतिष्ठित करने वाली चारों बातें इस परम्परा में विद्यमान हैं । पर हमारे देखने में यह बात उचित नहीं जंचती, क्यों कि इस परम्परा के श्रीविजयदेवसूरि से प्रवर्तित होने की बात निर्दिष्ट कारणों से नहीं सिद्ध होती और आचार्यान्तर- द्वारा उसका प्रवर्तन स्वयं श्रीसागरानन्दसूरि भी नहीं मानते । इस लिये जीतव्यवहारता के साधक चार अंशों में से पहला अर्थात् युग के प्रधान वा तत्समशील आचार्य के द्वारा प्रवर्तित होना- इस परम्परा में असिद्ध है ।
दूसरा अंश है किसी विशिष्ट प्रयोजन के उद्देश्य से प्रवर्तन । सो वह भी इस परम्परा में नहीं है, क्योंकि वह प्रयोजन क्षीण और वृद्ध पर्वतिथियों की आराधना का व्यवस्थापन ही कहा जा सकता है जो पर्वतिथियों के क्षय और वृद्धि को टिप्पणानुसार सत्य मानते हुये भी किस प्रकार उपपन्न हो जाता है यह बात हमारी सिद्धान्त-भूत व्याख्या में ज्ञात होगी । तीसरा अंश है प्रवर्तित आचार का शास्त्रों से अविरोध । यह भी इस परम्परा में नहीं है । क्यों कि सेनप्रश्न, कल्पसूत्रसुबोधिका, कल्पसूत्रदीपिका, हीरप्रश्न, और तत्त्वतरंगिणी आदि अनेक जैन-सम्प्रदाय के प्रामाणिक शास्त्र - ग्रन्थ इस परम्परा के विरुद्ध हैं ।
चौथा अंश है - संविग्न गीतार्थ आचार्यों द्वारा निषेध न किया जाना और अधिकसंख्यक अधिकारी जनों द्वारा स्वीकार कर लिया जाना । यह अंश भी इस परम्परा में प्रमाणित नहीं हो सकता । क्यों कि इस क्या प्रमाण कि संविग्न गीतार्थ आचार्यों ने इसका निषेध नहीं किया है ? यदि कहें कि ऐसे निषेध का न मिलना ही प्रमाण है, तो यह भी युक्त नहीं है, क्यों कि निषेध का न मिलना निषेध को उल्लिखित कर उसे प्रचारित और सुरक्षित रखने की व्यवस्था न होने पर निर्भर है । और ऐसी व्यवस्था न हो सकने का स्पष्ट कारण यह है कि यह परम्परा उस समय में प्रचलित हुई जब विद्या और आचरण के रक्षण और वर्धन में शिथिल - शील यतियों की प्रधानता थी, जब उनके प्रचार और प्रतिष्ठा का मध्याह्न था, और जब उनके उद्धत गर्जन के समक्ष संविग्न गीतार्थ आचार्योंकी शान्त शुद्ध वाणी परास्तप्राय हो रही थी । भला कौन उस समय उस निषेध को प्रचारित और परिरक्षित कर सकने का साहस कर सकता था । इस लिये तात्कालिक या तत्समीप- कालिक निषेध के न मिलने मात्र से निषेधाभाव की कल्पना अयुक्त है । इसके अतिरिक्त यह भी थोडा सोचने और समझने की बात है कि यदि किसी नवप्रवृत्त अशास्त्रीय आचार का तत्काल या कुछ अधिक काल तक भी किसी कारण से प्रबल विरोध न हो सका तो क्या इतने मात्र कुछ समय पीछे उस शास्त्रविरुद्ध आचरण के विरोध में बोलने का कोई मूल्य नहीं रह जाता ? इस बात को तो कोई भी समझदार मनुष्य स्वीकार नहीं कर सकता । अतः श्रीरामचन्द्रसूरि ने जैनसंघ में घुसे हुए इस दोष को दूर करने का पुण्य कार्य जिन प्रमाणों के आधार पर उठाया है और उनकी सत्यता तथा निर्दोषता को जिस प्रकार अनेक जैनमुनियों, जैन श्रावक और श्राविकाओं तथा अन्य तटस्थ विद्वानों के हृदय में स्थान मिलता जा रहा है, उसको देखते हुए यह सोद्घोष कहा जा सकता है कि जैन जनता इस कियत्कालिक परम्परा को जीताचार बनाने के डिण्डिम को अब और न बजने देगी।
""
निर्णय पत्र के तेरहवें पृष्ठ में मध्यस्थ ने कहा है कि आचार्य उमास्वाति के “ क्षये पूर्वा इत्यादि वचन की अपनी व्याख्या के पक्ष में श्रीसागरानन्दसूरि ने जिन शास्त्रों को घसीटने की चेष्टा की है वे शास्त्र नहीं हैं किन्तु शास्त्राभास हैं ।
१ देखिये मू० पु० पृ० सं० ४६
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org