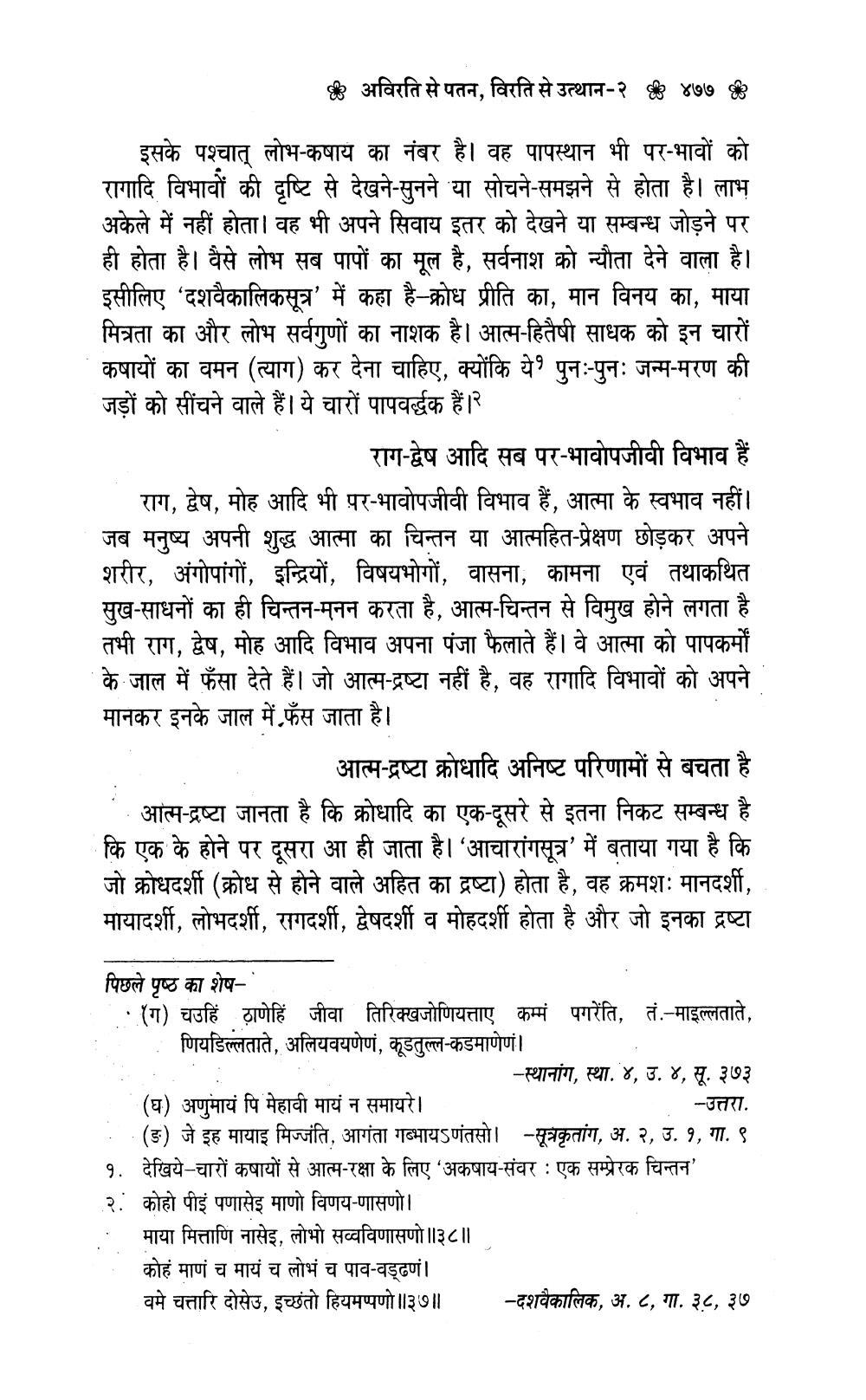________________
ॐ अविरति से पतन, विरति से उत्थान-२
४७७ 8
इसके पश्चात् लोभ-कषाय का नंबर है। वह पापस्थान भी पर-भावों को रागादि विभावों की दृष्टि से देखने-सुनने या सोचने-समझने से होता है। लाभ अकेले में नहीं होता। वह भी अपने सिवाय इतर को देखने या सम्बन्ध जोड़ने पर ही होता है। वैसे लोभ सब पापों का मूल है, सर्वनाश को न्यौता देने वाला है। इसीलिए 'दशवैकालिकसूत्र' में कहा है-क्रोध प्रीति का, मान विनय का, माया मित्रता का और लोभ सर्वगणों का नाशक है। आत्म-हितैषी साधक को इन चारों कषायों का वमन (त्याग) कर देना चाहिए, क्योंकि ये' पुनः-पुनः जन्म-मरण की जड़ों को सींचने वाले हैं। ये चारों पापवर्द्धक हैं।२।।
राग-द्वेष आदि सब पर-भावोपजीवी विभाव हैं राग, द्वेष, मोह आदि भी पर-भावोपजीवी विभाव हैं, आत्मा के स्वभाव नहीं। जब मनुष्य अपनी शुद्ध आत्मा का चिन्तन या आत्महित-प्रेक्षण छोड़कर अपने शरीर, अंगोपांगों, इन्द्रियों, विषयभोगों, वासना, कामना एवं तथाकथित सुख-साधनों का ही चिन्तन-मनन करता है, आत्म-चिन्तन से विमुख होने लगता है तभी राग, द्वेष, मोह आदि विभाव अपना पंजा फैलाते हैं। वे आत्मा को पापकर्मों के जाल में फँसा देते हैं। जो आत्म-द्रष्टा नहीं है, वह रागादि विभावों को अपने मानकर इनके जाल में फँस जाता है।
आत्म-द्रष्टा क्रोधादि अनिष्ट परिणामों से बचता है . आत्म-द्रष्टा जानता है कि क्रोधादि का एक-दूसरे से इतना निकट सम्बन्ध है कि एक के होने पर दूसरा आ ही जाता है। ‘आचारांगसूत्र' में बताया गया है कि जो क्रोधदर्शी (क्रोध से होने वाले अहित का द्रष्टा) होता है, वह क्रमशः मानदर्शी, मायादर्शी, लोभदर्शी, सगदर्शी, द्वेषदर्शी व मोहदशी होता है और जो इनका द्रष्टा
पिछले पृष्ठ का शेष• (ग) चउहि ठाणेहिं जीवा तिरिक्खजोणियत्ताए कम्मं पगरेंति, तं.-माइल्लताते, -णियडिल्लताते, अलियवयणेणं, कूडतुल्ल-कडमाणेणं।।
-स्थानांग, स्था. ४, उ. ४, सू. ३७३ (घ) अणुमायं पि मेहावी मायं न समायरे।
-उत्तरा. (ङ) जे इह मायाइ मिति, आगंता गब्भायऽणंतसो। -सूत्रकृतांग, अ. २, उ. १, गा. ९ १. देखिये-चारों कषायों से आत्म-रक्षा के लिए 'अकषाय-संवर : एक सम्प्रेरक चिन्तन' २. कोहो पीइं पणासेइ माणो विणय-णासणो।
माया मित्ताणि नासेइ, लोभो सव्वविणासणो॥३८॥ कोहं माणं च मायं च लोभं च पाव-वड्ढणं । वमे चत्तारि दोसेङ, इच्छंतो हियमप्पणो॥३७॥ -दशवैकालिक, अ. ८, गा. ३८, ३७